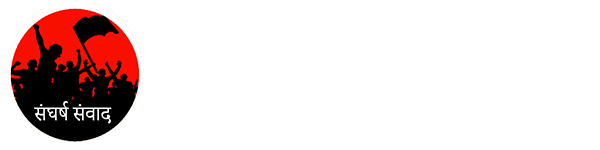भगत सिंह: व्यक्ति नहीं, विचार का नाम।
आदियोग
23 मार्च कलेंडर की कोई तारीख़ भर नहीं है। यह भगत सिंह की शहादत का दिन है या कहें कि शोषणमुक्त और बराबरी पर आधारित समाज की स्थापना के सुहाने सपने को ताज़ादम करने का दिन है, उसे पूरा करने के लिए जुटने और लड़ने-भिड़ने का संकल्प मज़बूत करने का दिन है, जनता की मुक्ति की लड़ाई में विचार की ताक़त और बलिदान की भावना को सम्मानित किये जाने का दिन है, बदलाव के लिए साझा पहल की ज़रूरत को रेखांकित किये जाने का दिन है। अगर ऐसा नहीं है तो भगत सिंह को याद करना बेमानी है, महज़ रस्म अदायगी है, शुद्ध दिखावा है और जो आख़िरकार भगत सिंह की क्रांतिकारी विरासत को सारहीन और धूमिल करने के अलावा और कुछ नहीं।
पिछली 23 मार्च को शहीदों की याद में लखनऊ में रैली निकली। रैली तय समय से एक घंटे बाद निकल सकी। रैली के आयोजन में कोई 35 संगठनों के नाम थे और रैली में बमुश्क़िल सौ लोग शामिल थे हालांकि उस दिन इतवार की छुट्टी भी थी।
यह स्थिति बहुत चिंताजनक है। चौतरफ़ा हाहाकार है और प्रतिरोध की आवाज़ें बहुत मद्धम, कमज़ोर और कुछ थकी-थकी सी लगती हैं। बदलाव की बात करनेवाले सभी लोगों और जन संगठनों के लिए यह आत्ममंथन से गुज़रने का विषय है।
बहरहाल, जैसा कि तय था, इस बार भी देश के विभिन्न हिस्सों में भगत सिंह को याद किया गया। पता नहीं कि पाकिस्तान में उन्हें उन्हें कहां-कहां याद किया गया लेकिन लाहौर के शादमान चौक पर ज़रूर लोग बड़ी संख्या में जुटे। एक बार फिर यह मांग उठी कि शादमान चौक का नाम बदल कर भगत सिंह चौक रखा जाये। लोगों ने कहा कि वे पाकिस्तान को एक ऐसे देश के रूप में देखना चाहते हैं जो सेकुलर और लोकतांत्रिक हो और जहां धर्म के नाम पर किसी के साथ कोई ज़ुल्म-ज़्यादती न हो, कि वे इसके लिए हर क़ीमत पर आवाज़ उठाते रहेंगे, ख़ामोश नहीं बैठेंगे।
याद रहे कि शादमान चौक वही जगह है जहां 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, राजगुरू और सुखदेव को गोरी सरकार ने फांसी पर लटकाया था। इस जगह भगत सिंह के नाम पर साल में दो बार जमावड़ा लगता है- 23 मार्च के अलावा उनकी सालगिरह पर 28 सितंबर को भी। 23 मार्च को अगर भगत सिंह की तस्वीर रख कर शादमान चौक पर मोमबत्तियां जलती हैं तो 28 सितंबर को केक कटता है। इसे उल्टी हवाओं के शहर में चराग़ जलाये रखना कहिये।
कोई साल भर पहले पाकिस्तान से अच्छी ख़बर आयी थी कि लाहौर प्रशासन ने फ़व्वारा चौक उर्फ़ शादमान चौक का नाम बदल कर भगत सिंह चौक कर दिया है। यह पाकिस्तान की सेकुलर और लोकतांत्रिक ताक़तों के निरंतर दबाव का नतीज़ा था। लेकिन इस अभूतपूर्व उपलब्धि का सुखद अहसास जल्दी ही उड़नछू हो गया। कट्टरपंथियों ने लाहौर प्रशासन के फ़ैसले का पुरजोर विरोध किया और उसे अदालत में चुनौती दी। यह मामला अभी भी अदालत में है और हाल-फ़िलहाल उसके सुलझने के आसार भी नज़र नहीं आते। कट्टरपंथियों का भोंड़ा तर्क है कि मुस्लिम बहुल पाकिस्तान में किसी काफ़िर को सम्मान क्यों मिले?
जिसकी आंख पर कट्टरपंथ का चश्मा हो, वो भगत सिंह को मज़हबी दड़बे से बाहर खड़ा कैसे देख सकता है और क्यों देखना चाहेगा? वह भगत सिंह के मशहूर लेख ‘मैं नास्तिक क्यों हूं’ को क्यों पढ़ेगा और पढ़ेगा तो उसे क्यों समझेगा? भगत सिंह केशधारी सिख से टोपीधारी साहब बने थे। यह ग़ुलामी से आज़ादी की जंग में अपनी धार्मिक पहचान शहीद कर देने के साहस का ऐतिहासिक अध्याय है। धार्मिक उन्माद इस जज़्बे को क्यों सलाम करेगा? उसे साझी शहादत और साझी विरासत से क्या लेनादेना? उसे तो शहीदों को भी जाति-धर्म की संकरी गलियों में देखने की आदत है। इसके उजड्ड उदाहरण हिंदुस्तान में भी कम नहीं है।
बहरहाल, कट्टरपंथियों की मांग है कि शादमान चौक को रहमत अली चौक के नाम से जाना जाये। बताते चलें कि भारत से अलग हुए हिस्से के लिए पाकिस्तान का नाम उन्होंने ही सुझाया था। अलग देश के लिए चले आंदोलन में भी वे पहली क़तार में शामिल थे। और सच यह भी है कि पाकिस्तान बनने के बाद बद से बदतर होते हालात से वह इतना खिन्न हुए कि उन्होंने देश ही छोड़ दिया और ताउम्र लंदनवासी रहे हालांकि पाकिस्तान के तमाम लोग उनके इस क़दम को नयी चुनौतियों से मुंह चुरा कर भाग जाना मानते हैं।
पाकिस्तान में शादमान चौक को भगत सिंह के नाम किये जाने की मांग बहुत पुरानी है। लेकिन इसे सबसे पहले 1980 में गति मिली। यह ज़िया उल हक़ की फ़ौज़ी हुक़ूमत का दौर था जिसमें राजनैतिक और नागरिक अधिकार निलंबित कर दिये गये थे। ऐसे में भगत सिंह का नाम लोकतांत्रिक शक्तियों के बीच एकता और संघर्ष का पर्याय हो गया, ख़ौफ़ और दहशत के अंधेरे दौर में मशाल बन गया।
भगत सिंह की यही प्रासंगिकता है। भगत सिंह का मतलब तर्कशीलता और निडरता से है, न्याय और बराबरी की पैरोकारी से है, सच्ची आज़ादी और असली लोकतंत्र के लिए अनवरत युद्ध के बिगुल से है। भगत सिंह व्यक्ति नहीं, जनता की मुक्ति के विचार का नाम है।
पाकिस्तान से एक और गुनगुनी ख़बर है। लाहौर के युवा पत्रकार वक़ार गिलानी की रिपोर्ट के मुताबिक़ गुज़री फ़रवरी को फ़ैसलाबाद प्रशासन ने भगत सिंह के जन्मस्थान को संरक्षित करने और उनके बांगे गांव को विकसित किये जाने की योजना तैयार की है। इस गांव में भगत सिंह ने अपने बचपन का बड़ा हिस्सा गुज़ारा था। जिस मकान में वे पैदा हुए, वहां बेरी का पेड़ है। इसे भगत सिंह के परिवार ने लगाया था। विभाजन के बाद यह मकान जिस परिवार को एलाट हुआ, उसने इस यादगार पेड़ को कटने नहीं दिया। आंगन में लगे इस पेड़ के पास भगत सिंह को इंक़लाबी शहीद बताते हुए तख़्ती लगायी जिसमें उनकी पैदाइश और शहादत की तारीख़ दर्ज़ है। इस परिवार की तीसरी पीढ़ी के पास भगत सिंह के परिवार की लकड़ी की आलमारी और आराम कुर्सी भी किसी नेमत की तरह सुरक्षित है।
बरसों पहले बांगे में हर साल भगत सिंह मेले का आयोजन हुआ करता था जिसकी जगह अब किसी पीर बाबा के उर्स ने ली है। लेकिन हां, भगत सिंह मेले की वापसी की कोशिशें भी हो रही हैं। पता नहीं कि इस मेले में भगत सिंह के विचार पक्ष को कितनी जगह मिलेगी? वैसे यही क्या कम है कि पाकिस्तान में भी ऐसे लोग हैं जो भगत सिंह को अपना आदर्श और जंगे आज़ादी का महानायक मानते हैं- भले ही वे मुट्ठी भर क्यों न हों। वरना तो पाकिस्तान की नयी पीढ़ी भगत सिंह समेत हिंदू नामधारी क्रांतिकारियों से अपरिचित है, जानबूझ कर अपरिचित रखी गयी है।
इसमें कोई नयी बात भी नहीं। यह हमेशा से होता आया है कि उसी इतिहास पर राज्य की मोहर लगती है जो शासकों की सहूलियतों के मुताबिक़ गढ़ा गया हो, तोड़ा-मरोड़ा गया हो- इधर भी और उधर भी, हर उस जगह जहां जन विरोधी ताक़तों के क़ब्ज़े में सत्ता और संसाधनों की चाभी है और इसी कारण आम लोगों की ज़िंदगी बेहाल है। भगत सिंह ने आम लोगों की आज़ादी का सपना देखा था- उस आज़ादी का नहीं कि गोरे अंग्रेज़ चले जायें और काले अंग्रेज़ क़ाबिज़ हो जायें। इस मायने में भगत सिंह का नाम और विचार हिंदुस्तान और पाकिस्तान में सक्रिय जनपक्षधर ताक़तों के बीच पुल की भूमिका अदा कर सकता है। इस पुल को मज़बूत किये जाने की ज़रूरत है।
बहरहाल, अपने देश में इन दिनों लोकसभा के चुनावी घमासान का नज़ारा है। जैसे भी हो, बस चुनाव जीतने की गलाकाटू होड़ है। कमाल की भगदड़ है कि रातों रात आस्था और प्रतिबद्धता बदल जाती है, कि कल तक एक-दूसरे पर लाठी भांजनेवाले आत्मा की पुकार पर अचानक गले मिलने लगते हैं, कि अब तक के वफ़ादार अपने ही सरदारों के कपड़े उतारने लगते हैं। चुनाव को लोकतंत्र का महापर्व कहा जाता है लेकिन हम इस विड़ंबना से दोचार हो रहे हैं कि इस महापर्व के आयोजन में किस तरह झूठ-फ़रेब और बेहया तिकड़मों का, अवसरवादी गठजोड़ों और भितरघातों का, जातिवाद और सांप्रदायिकता का, अपराध और भ्रष्टाचार का, कारपोरेटी गिद्धों और साम्राज्यवादी ताक़तों का बोलबाला है। विचार नाम की चिड़िया ग़ायब है, बेहतर भविष्य का ख़ाका नदारद है और जनता को बस वोट देने का अधिकार है गोया लोकतंत्र में जनता की भागीदारी बस यहीं तक सीमित हो।
संसदीय राजनीति के मैदान में यह चिंता और सरोकार सिरे से लापता है कि नवउदारवाद की आंधी में देश की संप्रभुता ख़तरे में है और आम लोगों के सामने जीने का भयावह संकट है, कि विकास के गर्वीले दावों के पीछे लूट और विनाश का महायज्ञ है, कि लोकतंत्र और आज़ादी का स्वाद मुट्ठी भर लोगों की बपौती है, कि मुनाफ़े के लुटेरे कहीं ज़्यादा ताक़तवर और हमलावर हो गये हैं, कि राज्य अपनी कल्याणकारी भूमिका से पल्ला झाड़ रहा है, और अधिक निरंकुश और बर्बर हो चला है, कि कंपनी राज नये भेस में लौट आया है। याद होगा कि अपने राष्ट्रपति ने पिछले गणतंत्र दिवस पर क्या कहा था? उन्होंने देश की जनता को समझाया था कि राज्य जन कल्याण की कोई दुकान नहीं है यानी होश में आओ, सरकार बहादुरों से मसीहाई की उम्मीद मत पालो।
1947 में देश आज़ाद हो गया और दो टुकड़ों में भी बंट गया- हिंदुस्तान और पाकिस्तान। यह बंटवारा धर्म के नाम पर हुआ। बाद में पाकिस्तान भी बंटा- पूर्वी पाकिस्तान बांग्लादेश हो गया। यह बंटवारा भाषा के नाम पर हुआ। लेकिन जनता का कहीं भी कोई भला नहीं हुआ। आज़ादी मिली लेकिन मेहनतकश और देशभक्त जनता ग़रीबी और बेचारगी से आज़ाद नहीं हो सकी, शोषण और उत्पीड़न के चक्रव्यूह से बाहर नहीं निकल सकी। उसके सामने ज़िंदा रहने का संकट पहले से कहीं अधिक विकराल और व्यापक हो गया। इससे उबरने की स्वाभाविक चाहत और वैज्ञानिक चेतना को दबाने-कुचलने के लिए दकियानूसी विचारों और अंधविश्वासों को खुली आज़ादी मिली, तालिबानी उन्माद और हिंदी-हिंदू-हिंदुस्तान का झंडा लगातार ऊंचा हुआ, आतंकवाद और माओवाद का हव्वा खड़ा हुआ।
कोई 20 साल पहले पाकिस्तान के मशहूर अवामी शायर हबीब जालिब ने कितना सही फ़रमाया था कि ‘हिंदुस्तान भी मेरा है और पाकिस्तान भी मेरा है। लेकिन इन दोनों मुल्क़ों पर अमरीका का डेरा है।’ यह ख़तरनाक़ हाल आज और ज़्यादा बेख़ौफ़ और बेक़ाबू हो चला है, देश की स्वायत्तता, स्वाभिमान और उसकी आत्मनिर्भरता को रौंदने में लगा है। यह नये अंदाज़ में ग़ुलामी के दौर की वापसी का सीन है।
सही मायनों में भगत सिंह को याद करना इस बदरंग और शर्मनाक़ तस्वीर को पलटने का सपना देखना है, उसे चुनौती देने के लिए हिम्मत और हौसला भरना है, विकल्पहीनता के अंधे कुएं से बाहर निकलने की जद्दोजहद में उतरना है। यह समझ हिंदुस्तान में और पाकिस्तान में भी तेज़ी से पक रही है, तमाम हमलों और रूकावटों के बावजूद परवान चढ़ रही है। यह उम्मीद की किरन है कि आज नहीं तो कल, हालात बदलेंगे, ज़रूर बदलेंगे… इधर भी और उधर भी, पूरी दुनिया में।
और क्यों नहीं बदलेंगे? दुनिया के कुल संसाधन का आधा हिस्सा 85 बेहद अमीरों की क़ब्ज़े में है और दूसरी तरफ़ दुनिया की एक तिहाई आबादी भुखमरी और ग़रीबी से बेहाल है। यह सरासर नाइंसाफ़ी है। ऐसे नाजायज़ क़ब्ज़ेदार और भी हैं और जगह-जगह हैं। लेकिन आख़िर कब तलक़ टिकेंगे? वे गिनती में हैं जबकि दुखियारी जनता अनगिनत। इतिहास गवाह है कि सताये जा रहे लोगों का ग़ुस्सा एकजुट होकर फूटता है तो तमाम बांध टूट जाया करते हैं। इंसाफ़ और इंसानियत का यही तक़ाज़ा है, जम्हूरियत का यही रास्ता है। लेकिन हां, यह जितना मुश्क़िल और पेचीदा है, उतना ही जोख़िम भरा भी ज़रूर है। लेकिन यह दुनिया जनता के राज का सपना देखनेवाले सिरफ़िरों से आख़िर कब ख़ाली रही है? जब तक यह सपना पूरा नहीं होता और जनता की ख़ुशहाली का दरवाज़ा नहीं खुलता- भगत सिंह तो पैदा होते रहेंगे…।
(किसी पाकिस्तानी चित्रकार का रेखांकन)