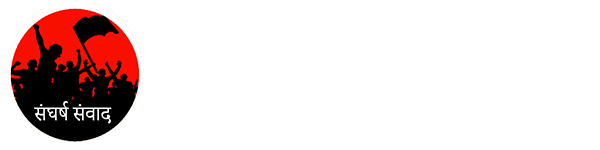कोलंबस के बाद जमीन की सबसे बड़ी लूट
पिछले कुछ सालों में किसानों के खेती छोड़ने की दर भी बढ़ी है. शहरी मजदूर के रूप में उनका पलायन बढ़ा है. जब किसान खेती छोड़ रहा है तो आखिर भूमि अधिग्रहण के ख़िलाफ़ संघर्ष कौन कर रहा है और क्यों? देश भर के किसान आंदोलनों, खेती और किसानी की दुश्वारियों, जमीनों पर पसरते रियल इस्टेट के जाल पर अलग-अलग हिस्सों में घूमकर किए गए अध्ययन पर अभिषेक श्रीवास्तव की एक विस्तृत जमीनी रिपोर्ट जिसे हम कैच हिंदी से साभार साझा कर रहे है.
अरशद खान 2009 तक एक पत्रकार हुआ करते थे. लखनऊ विश्वविद्यालय से पत्रकारिता करने के बाद जनता की आवाज़ बनने का आदर्श उन्होंने व्यवहार में उतारा और सात साल तक दिल्ली में रह कर ख़बरें करते रहे. फिर अचानक 2008 के अंत में मंदी आई.
मंदी भी ऐसी अजीबोगरीब कि हिंदुस्तान टाइम्स जैसे बड़े अखबार ने दस-बीस हज़ार तनख्वाह पाने वाले कुछ कर्मचारियों, मझोले पत्रकारों की नौकरी से निकाल दिया. बेरोज़गारी के बावजूद कुछ ने शहर में टिकने की भरसक कोशिश की, लेकिन 2009-2010 के दौरान अधिकतर पत्रकार कुछ और धंधों की ओर मुड़ गए.
अरशद के पास पर्याप्त ज़मीन थी. उन्हें खेती-किसानी पर पूरा भरोसा था. वे सीधे उत्तर प्रदेश के सीतापुर स्थित अपने गांव निकल लिए. बीते पांच साल में उनकी एकाध बार दोस्तों से फोन पर बात भी हुई. कभी पुदीने की खेती, कभी डेयरी फार्म, कभी पशुपालन की अपनी योजनाएं वे उन्हें बताते रहे. फिर एक लंबा समय गुज़र गया, सबने मान लिया कि अरशद खेती-किसानी में रम चुके हैं.
इसी नवंबर की एक चढ़ती दोपहर में अरशद का फोन आया. वे शहर में थे. अपने पुराने ठिकाने निज़ामुद्दीन के सेंट्रल गेस्ट हाउस में. मिले, तो बाल थोड़े पक चुके थे. चेहरा पत्थर की तरह सपाट था. चेहरे पर संतोष का भाव था. यह संतोष धंधे में कामयाबी का नहीं, सारे कर्ज चुका देने से उपजा था.
यह संतोष धंधे में कामयाबी का नहीं, सारे कर्ज चुका देने से उपजा था
पांच साल की खेती में उनके ऊपर करीब 35 लाख का कर्ज चढ़ चुका था. वे 30 बीघा ज़मीन बेचकर और खेती को हमेशा के लिए अलविदा कह कर दिल्ली में दोबारा लौटे थे, लेकिन इस बार पत्रकारिता के लिए नहीं. दुबई के काग़ज़ात तैयार हो रहे थे. वे किसी भी वक्त अगली फ्लाइट पकड़ने को तैयार थे.
खेती के मारे अरशद अकेले नहीं हैं. वे जिंदा हैं, बस यही गनीमत है. जिस दौर में रोज़ाना पचासेक किसान खुदकुशी करने को मजबूर हों, जिस देश ने पिछले साल 1109 किसानों की मौत देखी हो और जहां खेती की ज़मीन पिछले पांच साल में 0.43 फीसद घटकर 18 करोड़ 23.9 लाख हेक्टेयर रह गई हो, वहां शहरी बेरोज़गारी के संकट से आजिज़ आकर अपनी जड़ों की ओर वापस लौटना खुदकुशी करने से कम कुछ भी नहीं है.
बीते पांच साल के मुकाबले यह बात आज कहीं ज्यादा शिद्दत से लोग महसूस कर रहे हैं. दूसरी ओर, जिनकी समूची आजीविका खेती-किसानी पर ही टिकी हुई थी, वे भी अब शहरों की ओर भागने को बेताब हैं. तीसरा पक्ष सरकारों का है, जो उद्योगों के हित में खेती की ज़मीनों को कब्ज़ाती जा रही हैं. इस संकट को खेती का संकट कहा जाए या ज़मीन की लूट, इस पर बहुत बहस है.
किसान, ज़मीन, विकास, सरकार और खेती के जटिल रिश्ते को आखिर कैसे समझा जाए?
महाराष्ट्र में दिल्ली-मुंबई औद्योगिक गलियारे के खिलाफ आंदोलन चलाने वाली समाजकर्मी उल्का महाजन कहती हैं, “खेती को घाटे का सौदा बताने वाले और प्रचार करने वाले लोगों की मंशा दरअसल कंपनियों और सरकारों के हित में किसानों से ज़मीन छीनने में आसानी पैदा करना है.”
क्या किसान वाकई खेती को घाटे का सौदा नहीं मानता? फिर अरशद जैसे शिक्षित जागरुक किसानों पर इतना कर्ज कैसे चढ़ गया? क्या यह धंधे में उनकी नाकाबिलियत का नतीजा है? आखिर किसानों की बढ़ती खुदकुशी क्या ज़मीन की लूट का प्रत्यक्ष परिणाम है?
एक अहम सवाल यह है कि ज़मीन की लूट के खिलाफ जो भी किसान आंदोलन चल रहे हैं, क्या वहां सारा मामला मुआवजे की लड़ाई तक आकर नहीं सिमट जा रहा है? किसान, ज़मीन, विकास, सरकार और खेती के जटिल रिश्ते को आखिर कैसे समझा जाए?
नाकाम अध्यादेश?
पिछले साल केंद्र में बहुमत से आई नरेंद्र मोदी की सरकार ने जब 29 दिसंबर को भूमि अधिग्रहण कानून 2013 के ‘सहमति’ वाले उपबंध समेत अन्य में संशोधन के लिए अध्यादेश जारी किया, तो हल्ला मच गया. अचानक ऐसा लगा कि ज़मीन के मसले पर क्या राजनीतिक दल और क्या एनजीओ, सभी एक हो गए.
फरवरी में संसद मार्ग पर ‘भूमि अधिकार आंदोलन’ के बैनर तले हुई किसान संगठनों और जनांदोलनों की विशाल संयुक्त रैली और उसके बाद अध्यादेश की देश भर में जलाई गई प्रतियों ने साफ़ इशारा किया कि आने वाले दिनों में ज़मीन की लड़ाई और तीखी होने वाली है.
दो बार अध्यादेश लाने के बाद अगस्त में इसे वापस लेने के सरकारी फैसले को आंदोलनों की बड़ी जीत बताया गया. दिलचस्प यह है कि दिल्ली में जो जंग अब तक ‘ब्लैक एंड वाइट’ दिख रही थी, वह ज़मीन पर उतना ही धुंधलका पैदा कर चुकी थी.
अध्यादेश वापस लिए जाने के बाद 2013 के कानून में संशोधन की जो अस्पष्ट स्थिति थी, उसका फायदा राज्य सरकारों ने उठाया और पिछले एक साल में ज़मीन से जुड़ी जो लड़ाइयां उफान पर आईं, उनमें किसी को भी नहीं पता था कि ज़मीन किस कानून के तहत ली जानी है और मुआवजा किस कायदे के तहत दिया जाना है.
यह किसानों की जीत थी या ‘कोलंबस’ के भारतीय संस्करण का एक और सुनियोजित विस्तार?
राज्यों में पटवारी से लेकर तहसीलदार, डीएम और मुख्य सचिव के स्तर तक यह भ्रम अब तक कायम है और किसानों की नुमाइंदगी करने वाले अब तक जीत की खुमारी में हैं. दूसरी तरफ गिरफ्तारियों व मौतों का सिलसिला बदस्तूर कायम है. यह किसानों की जीत थी या ‘कोलंबस’ के भारतीय संस्करण का एक और सुनियोजित विस्तार?
भूमि अधिग्रहण अध्यादेश को एक साल पूरा होते-होते यह सवाल पूछा जाना बेहद ज़रूरी है क्योंकि बीते एक साल के दौरान किसी ने भी पलट कर ग्रामीण विकास मंत्रालय की 2009 में आई उस मसविदा रिपोर्ट को खंगालने की ज़हमत नहीं उठायी, जिसके 160वें पन्ने पर भारत के आदिवासी इलाकों में कब्जाई जा रही ज़मीनों को धरती के इतिहास में ‘कोलंबस के बाद की सबसे बड़ी लूट’ बताया था.
“कमिटी ऑन स्टेट अग्रेरियन रिलेशंस एंड अनफिनिश्ड टास्क ऑफ लैंड रिफॉर्म्स” शीर्षक से यह रिपोर्ट आज तक सार्वजनिक विमर्श का हिस्सा नहीं बन पाई है, जिसने छत्तीसगढ़ और झारखण्ड के कुछ इलाकों में सरकारों और निजी कंपनियों (नाम समेत) की मिलीभगत से हो रही ज़मीन की लूट से पैदा हो रहे गृहयुद्ध जैसे हालात की ओर इशारा किया था.
ईमानदार अफसर सरकार के भीतर भी हैं, लेकिन सदिच्छा और ईमानदारी काग़ज़ों तक सीमित रह जाने वाली चीज़ है
छह साल पहले आई अपनी ही रिपोर्ट पर यदि समय रहते सरकार ने अमल किया होता, तो आज न तो अध्यादेश की नौबत आती और न ही गृहयुद्ध जैसी स्थिति बस्तर, दंतेवाड़ा या बीजापुर से निकलकर शहरों-कस्बों तक फैलने पाती.
यह रिपोर्ट इस बात का ज्वलंत उदाहरण है कि ईमानदार अफसर सरकार के भीतर भी हैं, लेकिन सदिच्छा और ईमानदारी काग़ज़ों तक सीमित रह जाने वाली चीज़ है.
लूट एक, रास्ते अनेक
यह रिपोर्ट ज़मीन की लूट में सरकारों और कंपनियों की जिस मिलीभगत का जिक्र करती है, उसे आज हम देश के किसी भी कोने में देख सकते हैं. कहानियां एक से एक हैं और दिलचस्प हैं. उत्तराखण्ड के रामनगर में एक छोटा सा गांव है बीरपुर लच्छी.
यहां पीढ़ियों से नेपाली मूल की बुक्सा जनजाति के लोग रहते आए हैं. एक दिन अचानक इस गांव में किसी बाहरी का प्रवेश होता है. वह कुछ ज़मीनें घेर लेता है और फिर गांव से भारी-भरकम डम्परों की आवाजाही शुरू हो जाती है.
गांव वालों को पता लगता है कि सरकार ने उनकी ज़मीन पंजाब के किसी क्रेशर कारोबारी को बेच दी है जो कांग्रेस का नेता भी है. बात तब तक नहीं फैलती है जब तक कि एक दोपहर गांव की एक बच्ची डम्पर से गिरे पत्थर से मारी जाती है.
इसके बाद गांव के लोग डम्परों का रास्ता खोद देते हैं. अचानक रात में क्रेशर का मालिक अपने गुर्गों के साथ गांव पर गोलियों और बमों से हमला बोल देता है. औरतों-बुजुर्गों को पीटा जाता है.
जब बाहर के संगठन इस मामले में दखल देते हैं, तो उन पर जानलेवा हमला करवा दिया जाता है. कहानी पूरी फिल्मी लगती है.
बड़े पैमाने पर गिरफ्तारियां होती हैं. इलाके में धारा 144 लग जाती है. बांध का काम शुरू हो जाता है
दूसरी कहानी उत्तर प्रदेश के सोनभद्र की है. यहां कोई 40 साल पहले से कनहर नदी पर एक बांध की परियोजना लंबित थी. राज्य में 2012 में आई समाजवादी पार्टी की सरकार ने नए सिरे से इसमें दिलचस्पी लेनी शुरू की. पूरा इलाका आदिवासी बहुल है और तीन राज्यों छत्तीसगढ़, यूपी और झारखण्ड की सीमा पर पड़ता है. पता चला कि डूब क्षेत्र में तमाम आदिवासी गांव आ रहे हैं.
दिलचस्प यह है कि तमाम गैर-आदिवासी परियोजना से न केवल अप्रभावित थे बल्कि उनके डम्पर-ट्रैक्टर चल रहे थे. एक दिन आंबेडकर जयन्ती पर आदिवासी शांत जुलूस निकालते हैं. उन पर पुलिसिया फायरिंग होती है. एक को छाती में गोली लगती है. फिर वे धरने पर बैठते हैं तो एक सुबह मुंह अंधेरे पर उन पर पुलिस का हमला हो जाता है. बड़े पैमाने पर गिरफ्तारियां होती हैं. इलाके में धारा 144 लग जाती है. बांध का काम शुरू हो जाता है. यह अगस्त महीने की बात है.
बिलकुल इसी तर्ज पर इलाहाबाद के करछना स्थित कचरी गांव में पावर प्लांट का विरोध कर रहे ग्रामीणों पर आरएएफ और पीएसी का हमला होता है और चार दर्जन असहमत किसानों को जेल में ठूंस दिया जाता है.
कुछ कहानियां ऐसी हैं जहां राष्ट्रहित की भारी आड़ है. मसलन, राजस्थान के अलवर में रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन (डीआरडीओ) को ज़मीन दी गई है. कहा गया है कि यह एक ‘रणनीतिक परियोजना’ है. यह इलाका मेवात का है. यहां पीढ़ियों से मेवाती मुसलमान रहते आए हैं. राष्ट्र का ‘रणनीतिक’ मसला है, इसलिए कोई भी पहचाना जाना गवारा नहीं कर सकता. एक दिन विरोध में मौन जुलूस निकलता है तो अज्ञात लोगों पर एफआईआर दर्ज हो जाती है. इंसान तो इंसान, मेवात की पहाड़ियों पर चरने वाली बकरियों तक को नहीं बख्शा जाता है.
सुप्रीम कोर्ट के आदेश अनुपालन के बाद फिर से इस कवायद का अर्थ समझने में दिक्कत नहीं आनी चाहिए
कुछ कहानियों को सुनकर सुप्रीम कोर्ट भी बगले झांकने लगेगा. बीते दशकों में ओडिशा के नियमगिरि में ज़मीन बचाने की लड़ाई को सबसे कामयाब बताया गया है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने रायगढ़ा और कालाहांडी की 12 ग्राम सभाओं में वेदांता कंपनी के खिलाफ रायशुमारी करवाने का आदेश सरकार को दिया था.
एक रिटायर्ड जज की अगुवाई में 12 ग्राम सभाएं 2013 में हुईं और डोंगरिया कोंढ आदिवासियों ने एकमत से वेदांता कंपनी की खनन परियोजना के खिलाफ अपना मत दिया. इसके बाद वेदांता की बॉक्साइट खनन परियोजना खत्म मानी जा रही थी, लेकिन राज्य सरकार ने हार नहीं मानी है.
दो महीने पहले ही उसने पर्यावरण मंत्रालय को नए सिरे से सुनवाई करवाने को लिखा है. सुप्रीम कोर्ट के आदेश अनुपालन के बाद फिर से इस कवायद का अर्थ समझने में दिक्कत नहीं आनी चाहिए. इसे ही कुछ लोग ‘क्रोनी पूंजीवाद’ कहते हैं, जहां राज्य और कंपनियां देश को बेचने के लिए मिलकर काम करती हैं.
केंद्र सरकार ने जो ‘मेक इन इंडिया’ नाम का कार्यक्रम शुरू किया था, उसकी वेबसाइट पर ‘लाइव प्रोजेक्ट्स’ नाम का एक टैब है
हम कह सकते हैं कि ये फिर भी छिटपुट मसले हैं क्योंकि बड़े मसले वाकई इतने बड़े हैं कि उनसे होने वाले नुकसान का अंदाजा लगाना इतना सहज नहीं है. पिछले साल केंद्र सरकार ने जो ‘मेक इन इंडिया’ नाम का कार्यक्रम शुरू किया था, उसकी वेबसाइट पर ‘लाइव प्रोजेक्ट्स’ नाम का एक टैब है. उसे खोलने पर आंखें भी खुल सकती हैं और दिमाग भी. यह कहता है कि 2014-15 के बजट में पांच औद्योगिक गलियारा परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है जिनके इर्द-गिर्द 100 स्मार्ट सिटी बसाई जाएंगी.
दिल्ली-मुंबई इंडस्ट्रियल कोरिडोर, बंगलुरु-मुंबई इकनॉमिक कोरिडोर, चेन्नई-बंगलुरु इंडस्ट्रियल कोरिडोर, विजैग-चेन्नई इंडस्ट्रियल कोरिडोर, अमृतसर-कोलकाता इंडस्ट्रियल कोरिडोर नाम की ये पांच विशाल परियोजनाएं तकरीबन समूचे भारत को छेक लेती हैं. सिर्फ इससे अंदाजा लगाएं कि दिल्ली से मुंबई के बीच बन रहा गलियारा 1500 किलोमीटर लंबा और 300 किलोमीटर चौड़ा है.
अगर यह गलियारा बन गया, तो साल 2031 तक राजस्थान की 65 फीसदी ज़मीन इसमें चली जाएगी. इन पांचों गलियारों को आपस में जोड़ने वाले लिंक राजमार्ग अलग से होंगे जो बीच की ज़मीनें निगल जाएंगे. इन सभी परियोजनाओं में जेबीआईसी, एडीबी जैसी विदेशी एजेंसियों का पैसा लगा है और कहा जा रहा है कि इनसे जीडीपी की व़द्धि दर बहुत ऊंची हो जाएगी. यह सब कुछ खेती-किसानी की कीमत पर ही होगा.
किसान क्यों करे खेती?
क्या खेती को डकार जाने वाली इन प्रस्तावित परियोजनाओं के बावजूद खेती की जा सकती है? ज़ाहिर है, जो किसान अपनी ज़मीनें बचाने के संघर्ष में जुटे हैं, उन्हें इसका भरोसा तो होगा ही. देश के अलग-अलग हिस्सों में हालांकि अपनी ज़मीनें गंवाने के कगार पर खड़े किसानों से बात करें, तो हकीकत कुछ और समझ में आती है.
ओडिशा के जगतसिंहपुर स्थित ढिंकिया गांव में पान की खेती करने वाला युवक नित्यानंद स्वाईं कहते हैं, “हमारे यहां काजू और पान खूब होता है. इससे हमारी अच्छी कमाई हो जाती है. सरकार अगर उसी हिसाब से बाजार दर पर मुआवजा दे, तो बात बन सकती है वरना हम अपनी ज़मीन छोड़ कर क्यों जाएंगे.”
सोनभद्र के कनहर में अप्रैल की गिरफ्तारियों और अब रिहाई के बाद आदिवासियों को एसडीएम रोज़ाना मुआवजे का चेक बांट रहे हैं. अखबारों में तस्वीरें छप रही हैं. इस मामले समेत करछना के किसानों का मुकदमा लड़ रहे इलाहाबाद के वरिष्ठ अधिवक्ता ओडी सिंह कहते हैं, “लड़ाई तो चलती ही रहेगी. मामला यहीं फंसा है कि किसान 2013 के कानून के मुताबिक मुआवजा मांग रहे हैं जबकि सरकार पहले वाले कानून का सहारा ले रही है.”
कचरी गांव के लोग एक स्वर में शिकायत करते हैं कि उनसे स्कूल, अस्पताल और विकास का वादा किया गया था जिसे पूरा नहीं किया गया. अगर यह सब हो जाता, तो उन्हें लड़ने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती.
कुछ जन संगठनों का कहना था कि इसे भूमि बचाओ आंदोलन कहा जाना चाहिए क्योंकि मुद्दा ज़मीन बचाने का है
हालांकि सब जगह ऐसा नहीं है. झारखण्ड में एक स्टील प्लांट के खिलाफ ‘एक इंच ज़मीन नहीं देंगे’ का जो नारा कुछ साल पहले लगा था, लोगों ने उसे ज़मीन पर उतारा भी और कंपनी को आखिरकार लौटा दिया. यह नारा हालांकि आज की तारीख में कमज़ोर पड़ चुका है क्योंकि अपनी ही खेती पर किसानों को बहुत भरोसा नहीं रहा.
यह स्थिति खासकर उत्तरी भारत के मैदानी इलाकों के संदर्भ में सही जान पड़ती है, जहां टीवी और मोबाइल जैसे उपकरण काफी पहले पहुंच चुके थे और महत्वाकांक्षाओं का स्तर महानगरीय नहीं तो कम से कम शहरी ज़रूर हो चुका है. किसान आंदोलनों के भीतर इसी समझदारी का परिणाम था कि पहली बार अध्यादेश लाए जाने के बाद दिल्ली के कांस्टिट्यूशन क्लब में जब भूमि अधिग्रहण अध्यादेश के खिलाफ साझा मोर्चा बनाने की प्रक्रिया चल रही थी, तो इस मोर्चे के नाम को लेकर संगठनों के बीच मतभेद पैदा हुआ था.
कुछ जन संगठनों का कहना था कि इसे भूमि बचाओ आंदोलन कहा जाना चाहिए क्योंकि मुद्दा ज़मीन बचाने का है. भूमि अधिकार से उन्हें परहेज़ था क्योंकि इसका एक अर्थ यह भी निकलता है कि जिनके पास अपनी खेती की ज़मीन नहीं है, उन्हें भी ज़मीन का अधिकार है. ऐसे में इस आंदोलन का स्वाभाविक विस्तार ज़मीन कब्ज़ाने तक चला जाता.
इस मसले पर एकाध संगठनों ने मंच से खुद को अलग भी कर लिया और बाद में आरएसएस समर्थित अन्ना हजारे के मंच पर जाकर बैठ गए. बाद में हालांकि “भूमि अधिकार आंदोलन” के नाम पर ही सहमति बनी, जिसने साल भर आंदोलन को चलाया और आगे भी इसी नाम से संघर्ष जारी रहेगा.
भूमि आंदोलन के प्रायोजक
जिन किसानों के पास ज़मीनें हैं, ज़ाहिर है ज़मीन की लड़ाई भी वे ही लड़ेंगे लिहाजा किसान आंदोलन का ‘ओनस’ भी उनके ऊपर ही होगा. इसका मतलब यह नहीं कि वे खेती को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं. उत्तर प्रदेश में हाल में हुए जिला पंचायत और प्रधानी के चुनावों में उतरे कई उम्मीदवार ऐसे हैं जो अपने-अपने क्षेत्रों में ज़मीन की लड़ाइयों की नुमाइंदगी करते हैं.
उत्तर प्रदेश में भूमि अधिग्रहण के मामलों पर अक्टूबर में बनारस में एक सम्मेलन हुआ जिसमें करछना के किसानों के समर्थन में एक प्रस्तावित राज्यस्तरीय कार्यक्रम की तारीख केवल इसलिए फंस गई क्योंकि ग़ाज़ीपुर, बलिया, मिर्जापुर आदि से आए किसान नेताओं को खुद या अपनी पत्नियों को चुनाव लड़वाना था.
कुछ ऐसे ही हित भूमि-अधिकार आंदोलन के मशहूर चेहरों के साथ भी जुड़े हैं, जिनमें एक के बारे यह चर्चा आम है कि वे मैग्सेसे पुरस्कार के लिए तगड़ी लॉबिइंग में जुटी हैं. करछना के किसान नेता राजबहादुर पटेल फ़रार चल रहे हैं तो कनहर के एक आदिवासी नेता छाती पर गोली खाने के बाद बांध में सुरक्षागार्ड की नौकरी पा गए हैं.
खेती के मूल तर्क को बहाल करने की लड़ाई अब तक इस देश में संगठित रूप से शुरू नहीं हुई है
सबसे दिलचस्प स्थिति उत्तराखण्ड के नैनीसार की है. यहां गांव वालों के फर्जी दस्तखत कर के जिंदल समूह को सरकार के इशारे पर ग्राम सभा की ज़मीन सौंप देने वाले 30 वर्षीय ग्राम प्रधान गोकुल राणा अल्मोड़ा विश्वविद्यालय के अपने दिनों में पुराने आंदोलनकारी पीसी तिवारी के अनुयायी हुआ करते थे. अब, जबकि पीसी तिवारी की उत्तराखण्ड परिवर्तन पार्टी खुद गांव वालों के साथ और प्रधान के खिलाफ ज़मीन के मसले पर खड़ी है, तो राणा कहते फिर रहे हैं, “हम छात्र जीवन में खुद तिवारीजी से बहुत प्रभावित रहते थे. हमें क्या पता था कि वो ये सब काम भी करते हैं. वे हमारे गांव में कैसे घुस गए, यह हमारे लिए अब तक रहस्य है.”
उधर, ओडिशा के जगतसिंहपुर और नियमगिरि, राजस्थान के अलवर और महाराष्ट्र के नागपुर में ज़मीन की लड़ाई लड़ने वाले कुछ जन-नेताओं ने पिछले चुनावों में आम आदमी पार्टी का दामन टिकट के चक्कर में थाम लिया था और हारने के बाद अब तक इस सदमे से उबर नहीं पाए हैं.
कुछ और जगहों पर दिलचस्प प्रयोग हुए हैं. मसलन, छत्तीसगढ़ के रायगढ़ में जिंदल कंपनी के खिलाफ़ ज़मीन की लड़ाई लड़ रहे किसानों ने संघर्ष करते-करते कोयला खोदने के लिए खुद ही एक कंपनी बना डाली. इन किसानों की नेता सरिताजी बड़े गर्व से बताती हैं कि अब गोरताप उपक्रम प्रोड्यूसर कंपनी के माध्यम से आदिवासी खुद अपना कोयला खनन करेंगे और उन्हें किसी निजी कंपनी का मुंह नहीं देखना पड़ेगा.
खेती का संकट अपनी जगह बना हुआ क्योंकि खेती के मूल तर्क को बहाल करने की लड़ाई अब तक इस देश में संगठित रूप से शुरू नहीं हुई है. खेती-किसानी का बुनियादी तर्क यह था कि आदमी अपने खाने-पकाने के लिए अनाज उपजाता था. जो बच जाता था, उसे वह बेच देता था. पहले पेट भरता था, फिर बचे तो मंडी.
वे कभी नहीं मानेंगे कि किसान ज़मीन बेचने को तैयार बैठा है जबकि किसान बार-बार यही कह रहा है
आजादी के बाद से किसान एफसीआई के गोदामों के लिए उपजाने लगा क्योंकि उस दौर में वैश्विक राजनीति का एक बड़ा आयाम खाने में आत्मनिर्भरता का था. इसके चलते बहुफसली खेती चौपट हुई. बाजार के लिए एकफसली उपज होने लगी. नब्बे के दशक में किसान को कहा गया कि घरेलू नहीं, वैश्विक बाजार के लिए अन्न उपजाओ. कौन सा अन्न?
सोयाबीन, कपास, जटरोफा, सूरजमुखी, आदि. किसान बीते तीन दशक से जो उपजा रहा है, वह अपने पेट के लिए नहीं बल्कि कारों का पेट भरने के लिए है. सोयाबीन, जतरोफा, सूरजमुखी, गन्ना, मकई आदि से बायोडीजल बन रहा है. खेती का पूरा तर्क ही सिर के बल खड़ा कर दिया गया है. किसान जान रहा है कि उसे वैश्विक बाजार के लिए उपजाना है और खुद भूखे मरना है, इसलिए वह खेती से कन्नी काट रहा है.
जहां इस तर्क को दरकिनार कर के सिर्फ ज़मीन बचाने की लड़ाई चल रही है, वहां दिल्ली के बड़े मंचों पर नुमाइंदगी करने वाले नेता इस बात को स्वीकार करने से कतराते हैं कि सारी जंग सही मुआवजे की है. वे कभी नहीं मानेंगे कि किसान ज़मीन बेचने को तैयार बैठा है जबकि किसान बार-बार यही कह रहा है. ऐसे में किसानों की मूल भावना और किसान मंचों की प्रायोजित भावना के बीच बड़ी दूरी पैदा होती जा रही है.
ऐसे में अरशद जैसे लाखों किसानों को जब अपनी सही नुमाइंदगी करने वाला कोई नहीं मिल रहा, तो वे शहरों का रुख कर रहे हैं. साठ फीसदी किसान भारी कर्ज में हैं और पंजाब जैसे संपन्न राज्य में भी किसान अपनी जान दे रहे हैं. साल 2011 की जनगणना को मानें तो औसतन 2,300 लोग रोज़ाना खेती छोड़ रहे हैं और अतंरराष्ट्रीय रेटिंग एजेंसी क्राइसिल की मानें तो बीते आठ साल में तीन करोड़ 70 लाख किसान खेती छोड़कर शहरों की ओर पलायन कर गए हैं.
कवि और पत्रकार रघुवीर सहाय ने बहुत पहले लिखा था, “खतरा होगा, खतरे की घंटी होगी, उसे बादशाह बजाएगा, रमेश!”
यह बात अलग है कि विनिर्माण क्षेत्र में नौकरियां नहीं मिलने के कारण 2012 से 2014 के बीच करीब डेढ़ करोड़ लोग वापस अपने गांवों को लौट गए हैं. संकट दुतरफा है. एक ओर गांव के गांव खाली हो रहे हैं तो दूसरी ओर शहरों पर बढ़ रहे आबादी के दबाव के कारण शहरी ढांचे तबाह हो रहे हैं.
कुछ विश्लेषक कहते हैं कि अगले बीस सालों में देश की आधी आबादी शहरों की निवासी होगी. कवि और पत्रकार रघुवीर सहाय ने बहुत पहले लिखा था, “खतरा होगा, खतरे की घंटी होगी, उसे बादशाह बजाएगा, रमेश!”
खतरे की यह घंटी 2009 में ही बजा दी गई थी. बादशाह ने ही बजाई थी. बीते छह साल में इसे किसी ने नहीं सुना. सुन कर भी नजरंदाज़ किया. आज कोलंबस पूरे देश को चर रहा है. अन्नदाता को बचाने के लिए क्या और बड़ा सबूत हमें चाहिए?