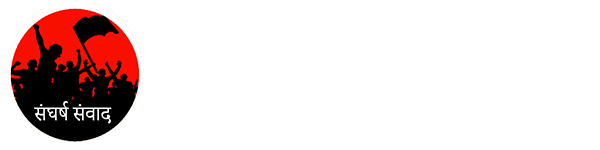मुसहरों को नसीहत नहीं, अधिकार चाहिए
बरही नवादा से लौट कर आदियोग
 |
| मंच पर भीड़ |
 |
| …और छलक पड़े आंसू |
यह गुज़री 2 दिसंबर को बनारस के बरही नवादा गांव में आयोजित मुसहर-दलित-वंचित सम्मेलन का सीन था- तयशुदा कार्यक्रम और उसके मक़सद से एकदम उलट। सम्मेलन के आयोजन के पीछे मक़सद था कि मुसहरों के साथ दूसरे अति वंचित समुदाय जुड़ें। अपने दुख-दर्द साझा करें और बेहतरी के लिए उठाये जानेवाले ज़रूरी क़दमों पर फ़ैसला लें। इस तरह यथास्थिति के टूटने की शुरूआत हो।
महिलाओं ने बयान किये दर्द