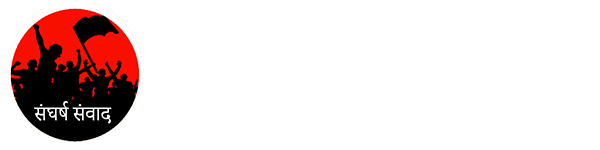भगत सिंह को याद करने का मतलब
आदियोग
23 मार्च कलेंडर की तारीख़ भर नहीं है। यह भगत सिंह की शहादत का दिन है या कहें कि शोषणमुक्त और बराबरी पर आधारित समाज की स्थापना के सुहाने सपने को ताज़ादम करने का दिन है, उसे पूरा करने के लिए जुटने और लड़ने-भिड़ने का संकल्प दोहराने का दिन है, जनता की मुक्ति की लड़ाई में विचार और बलिदान के महत्व को रेखांकित किये जाने का दिन है…। ज़ाहिर है कि देश के विभिन्न हिस्सों में आज का दिन भगत सिंह के नाम होगा। पाकिस्तान में भी हलचल होगी- ख़ास कर लाहौर के शादमान चौक पर तो ज़रूर। तय है कि एक बार फिर यह मांग ज़ोर पकड़ेगी कि शादमान चौक का नाम बदल कर भगत सिंह चौक रखा जाये। यह वही जगह है जहां 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, राजगुरू और सुखदेव को गोरी सरकार ने फांसी पर लटकाया था।
कोई साल भर पहले पाकिस्तान से अच्छी ख़बर आयी थी कि लाहौर प्रशासन ने फ़व्वारा चौक उर्फ़ शादमान चौक का नाम बदल कर भगत सिंह चौक कर दिया है। यह पाकिस्तान की सेकुलर और लोकतांत्रिक ताक़तों के निरंतर दबाव का नतीज़ा था। लेकिन इस अभूतपूर्व उपलब्धि का सुखद अहसास जल्दी ही उड़नछू हो गया। कट्टरपंथियों ने लाहौर प्रशासन के फ़ैसले का पुरजोर विरोध किया और उसे अदालत में चुनौती दी। यह मामला अभी भी अदालत में है और हाल-फ़िलहाल उसके सुलझने के आसार भी नज़र नहीं आते। कट्टरपंथियों का तर्क है कि मुस्लिम बहुल पाकिस्तान में किसी काफ़िर को सम्मान क्यों मिले?
जिसकी आंख पर कट्टरपंथ का चश्मा हो, वो भगत सिंह को मज़हबी दड़बे से बाहर खड़ा कैसे देख सकता है और क्यों देखना चाहेगा? वह भगत सिंह के मशहूर लेख ‘मैं नास्तिक क्यों हूं’ को क्यों पढ़ेगा और पढ़ेगा तो उसे क्यों समझेगा? उसे साझी शहादत और साझी विरासत से क्या लेनादेना? उसे तो शहीदों को भी जाति-धर्म की संकरी गलियों में देखने की आदत है। इसके उजड्ड उदाहरण हिंदुस्तान में भी कम नहीं है।
बहरहाल, कट्टरपंथियों की मांग है कि शादमान चौक को रहमत अली चौक के नाम से जाना जाये। बताते चलें कि बंटवारे से बने नये देश के लिए पाकिस्तान का नाम उन्होंने ही सुझाया था। बंटवारे के लिए चले आंदोलन में प्रमुख भूमिका अदा करनेवालों में उनका नाम गिना जाता है। सच यह भी है कि पाकिस्तान बनने के बाद बद से बदतर होते हालात से वह इतना खिन्न हुए कि उन्होंने देश ही छोड़ दिया और ताउम्र लंदनवासी रहे।
पाकिस्तान में शादमान चौक को भगत सिंह के नाम किये जाने की मांग बहुत पुरानी है। लेकिन इसे सबसे पहले 1980 में गति मिली। यह ज़िया उल हक़ की फ़ौज़ी हुक़ूमत का दौर था जिसमें राजनैतिक और नागरिक अधिकार निलंबित कर दिये गये थे। ऐसे में भगत सिंह का नाम लोकतांत्रिक शक्तियों के बीच एकता और संघर्ष का पर्याय हो गया, ख़ौफ़ और दहशत के अंधेरे दौर में मशाल बन गया।
भगत सिंह की यही प्रासंगिकता है। भगत सिंह का मतलब तर्कशीलता और निडरता है, न्याय और बराबरी की पैरोकारी है, सच्ची आज़ादी और असली लोकतंत्र के लिए अनवरत युद्ध का बिगुल है। भगत सिंह व्यक्ति नहीं, जनता की मुक्ति के विचार का नाम है।
देश में लोकसभा के चुनावी घमासान का नज़ारा है। जैसे भी हो, बस चुनाव जीतने की गलाकाटू होड़ है। कमाल की भगदड़ है कि रातों रात आस्था और प्रतिबद्धता बदल जाती है, कि कल तक एक-दूसरे पर लाठी भांजनेवाले आत्मा की पुकार पर अचानक गले मिलने लगते हैं। चुनाव को लोकतंत्र का महापर्व कहा जाता है लेकिन हम इस विड़ंबना से दोचार हो रहे हैं कि इस महापर्व के आयोजन में किस तरह झूठ-फ़रेब और बेहया तिकड़मों का, अवसरवादी गठजोड़ों और भितरघातों का, अपराध और भ्रष्टाचार का, कारपोरेटी गिद्धों और साम्राज्यवादी ताक़तों का बोलबाला है। विचार नाम की चिड़िया ग़ायब है, बेहतर भविष्य का ख़ाका नदारद है।
संसदीय राजनीति के मैदान में यह चिंता और सरोकार सिरे से लापता है कि नवउदारवाद की आंधी में देश की संप्रभुता ख़तरे में है और आम लोगों के सामने जीने का भयावह संकट है, कि विकास के गर्वीले दावों के पीछे लूट और विनाश का महायज्ञ है, कि लोकतंत्र और आज़ादी का स्वाद मुट्ठी भर लोगों की बपौती है, कि मुनाफ़े के लुटेरे कहीं ज़्यादा ताक़तवर और हमलावर हो गये हैं, कि राज्य अपनी कल्याणकारी भूमिका से पल्ला झाड़ कर और अधिक निरंकुश और बर्बर हो चला है, कि कंपनी राज नये भेस में लौट आया है।
सही मायनों में भगत सिंह को याद करना इस बदरंग तस्वीर को पलटने का सपना देखना है, उसे चुनौती देने के लिए हिम्मत और हौसला भरना है, विकल्पहीनता के अंधे कुएं से बाहर निकलने की जद्दोजहद में उतरना है। यह समझ हिंदुस्तान में और पाकिस्तान में भी तेज़ी से पक रही है, परवान चढ़ रही है। यह उम्मीद की किरन है कि आज नहीं तो कल, हालात बदलेंगे, ज़रूर बदलेंगे… ।
किसी पाकिस्तानी चित्रकार की कूची से भगत सिंह का रेखांकन