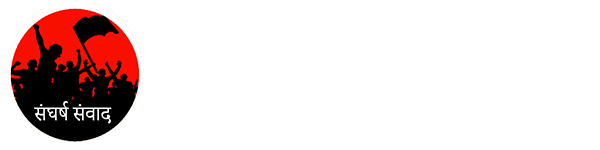मनरेगा : काम के अधिकार के साथ बेहूदा मज़ाक़
तो मनरेगा मज़दूरों ने बंद हाल में अपनी व्यथा कथा रखी। उनकी सुनने को एक पैनल था। इसमें वरिष्ठ पत्रकार महेश पांडे, ट्रेड यूनियन नेता केके शुक्ला और उच्च न्यायालय के वरिष्ठ अधिवक्ता अंबिका प्रसाद भी थे। तीनों ने माना कि मनरेगा की चाल कहीं से ठीक नहीं है, इसलिए कि सरकारी नीयत ही ठीक नहीं है। इसे पटरी पर लाने के लिए संगठित संघर्ष के सिवा दूसरा चारा नहीं। पिछले साल अक्तूबर में राज्य सरकार ने मनरेगा का सोशल आडिट निदेशालय खोला था जिसका कामकाज अब कहीं जाकर शुरू हो सका। पैनल के सदस्य के बतौर उसके निदेशक कार्यक्रम में ज़रूर पहुंचे लेकिन संबंधित विभाग के समाजवादी मंत्री जी अपनी रज़ामंदी के बावजूद दुखियारों की आवाज़ सुनने के लिए फ़ुर्सत नहीं निकाल सके।
मनरेगा मज़दूरों का यह जमावड़ा कासा, जन केंद्रित विकास समिति और लोक हक़दारी मोर्चा की संयुक्त पहल से मुमकिन हुआ। इसमें उत्तर प्रदेश के आठ जिलों में किये गये मनरेगा के सोशल आडिट की रिपोर्ट भी पेश हुई। सोशल आडिट जालौन, बांदा, मीरज़ापुर, सोनभद्र, चित्रकूट, झांसी, फतेहपुर और देवरिया की 11 ग्राम पंचायतों के कुल 5658 परिवारों तक सीमित था। हस्तक्षेप का आकार भले ही बहुत छोटा था लेकिन उसके नतीज़े यह बताने के लिए काफी हैं कि ग्रामीण जनता को काम का क़ानूनी अधिकार देनेवाली केंद्र की इस महत्वपूर्ण योजना का हालचाल किस हद तक गड़बड़ है। कि यह बड़े पैमाने पर मनमर्ज़ी, धांधली और घपलों के हवाले है।
नियमानुसार मनरेगा की कार्य योजना पंचायत की खुली बैठक में तैयार की जानी चाहिए और इसके लिए सभी को सूचित भी किया जाना चाहिए। लेकिन वास्तव में ऐसा होता नहीं। अधिकतर लोगों को पता ही नहीं चलता और कार्य योजना ‘सर्वसम्मति’ से तैयार हो जाती है। यह काम प्रधान जी और पंचायत सचिव अकेले निपटा देते हैं। जहां बैठक होती भी है तो वहां दमदार लोग प्रस्ताव रखते हैं और बाक़ी लोग केवल सहमति में हाथ उठाने के लिए होते हैं। मनरेगा केवल काम के बदले मज़दूरी देने भर के लिए नहीं है। मक़सद यह भी है कि ऐसे कामों की योजना बने जो स्थानीय ज़रूरतों के हिसाब से हो और जिसका लाभ या प्रभाव लंबे समय तक टिके। यह तभी मुमकिन है जब सभी लोगों की सक्रिय भागीदारी हो, उन्हें अपनी राय रखने की आज़ादी हो और ज़िम्मेदारों में उस पर विचार किये जाने की उदारता हो।
लेकिन यह उदारता हो तो कहां से हो? नया पंचायती राज आया तो उम्मीद बंधी थी कि अब गांवों में रहनेवाले ग़रीबों के दिन बहुरेंगे। लोगों को अपना और अपने गांव का भला करने का मौक़ा मिलेगा। पंचायत को स्थानीय स्वशासन की इकाई का नाम मिला। लेकिन दुर्भाग्य से पंचायतों को महज़ सरकारी योजनाओं और कार्यक्रमों के क्रियान्वयन की इकाई बना दिया गया। पेंचदार सरकारी प्रक्रियाओं ने उसकी स्वयात्तता का अपहरण कर लिया और उसे सरकारी कठपुतली की भूमिका में क़ैद कर लिया। ज़ाहिर है कि पंचायतें संसदीय राजनीति के अखाड़ों का हिस्सा हो गयीं। पंचायती चुनाव लड़ना लगातार ख़र्चीला होता गया और चुनाव जीतना धनबल, बाहुबल और जातीय समीकरणों के भरोसे हो गया। विकास के नाम पर जारी फ़ंड की लूट का नया अड्डा बन गया। मनरेगा को भी भ्रष्टाचार के निशाने पर तो आना ही था।
अभी फ़रवरी में मनरेगा की मज़दूरी में राज्यवार बढ़त हुई है। उत्तर प्रदेश में यह 125 रूपये से बढ़ कर 145 रूपये प्रतिदिन हो गयी है। अब यह मामूली हिसाब मज़दूरी की नयी दर से लगायें। माना कि हर परिवार को साल में सौ दिन का काम मिला, समय से मज़दूरी का दाम मिला और वह भी नियमानुसार। उसमें कोई कमीशन नहीं कटा। साल की कुल मज़दूरी होगी- साढ़े 14 हज़ार। अब इसे 365 दिनों से भाग करें। यह 40 रूपये प्रति परिवार प्रतिदिन से कम है। अगर एक परिवार में औसतन पांच सदस्य मानें तो प्रति व्यक्ति हिस्सेदारी आठ रूपये से कम है। मनरेगा के नगाड़े का इतना ऊंचा शोर और उसकी इतनी पिद्दी थिरकन? तो मनरेगा ग्रामीण आजीविका के नाम पर केवल सजाधजा झुनझुना है और वह भी सही तरीक़े से नहीं बजता।
इसका यह मतलब भी नहीं कि इस मुद्दे से पल्ला झाड़ लिया जाये। मनरेगा इसलिए आया था कि कांग्रेस को भाजपा की अगुवाईवाली तत्कालीन केंद्र सरकार के ‘शाइनिंग इंडिया’ के नारे को ख़ाली डिब्बे का शोर बताना था और ‘हर हाथ को काम दो’ के पुराने नारे की नयी उठान को भी साधना था। मनरेगा तेज़ी से बदलती राजनैतिक परिस्थितियों और बढ़ते जन दबाव का नतीज़ा था। लोकसभा चुनाव आनेवाले हैं। मज़दूरी की दर में इसीलिए बढ़त हुई है। यों भी बढ़ती मंहगाई को देखते हुए मज़दूरी बढ़ने की मांग पहले से ज़ोर पकड़ रही थी। यही समय है जब परिवार के बजाय हर बालिग को काम की गारंटी देने और उसे सौ दिन के बजाय तीन सौ दिन करने का सवाल चौतरफ़ा गूंजे। सरकारें बहादुरें तभी चेतती हैं जब दुखियारी जनता की आवाज़ें उनके वजूद पर ख़तरा बन मंडराने नहीं लगतीं।
फ़िलहाल, बेबसी में डूबे इन चंद बयानों पर ग़ौर करें;
मुनरी देवी (बौरी गांव, मरदह ब्लाक, ग़ाज़ीपुर) को पिछले साल कुल दस दिन काम मिला। मज़दूरी के भुगतान के लिए कई मर्तबा ब्लाक और ज़िले तक का चक्कर लगाया। तब कहीं जाकर भुगतान हुआ लेकिन उनके हाथ कुल दो सौ रूपये लगे। बाक़ी रूपये प्रधान जी ने ख़ुद रख लिये। उन्हीं के गांव की कालिका देवी को पिछले तीन साल से कोई काम ही नहीं मिला। दोनों के पास बस कहने भर को खेती की ज़मीन है। दाने-दाने की क़िल्लत रहती है पर उनके परिवारों के पास राशन कार्ड भी नहीं।
पतिराम (चौराबोझ गांव, मरदह ब्लाक, ग़ाज़ीपुर) के मुताबिक़ प्रधान जी सबका जाब कार्ड अपने पास रखते हैं। बाहर से मिली इस जानकारी को अफ़वाह बताते हैं कि काम के लिए आवेदन करना होता है, कि उसकी पावती लेनी चाहिए, कि काम न मिले तो बेरोज़गारी भत्ते की हक़दारी बनती है। पप्पूराम (तिसड़ा गांव, सादात ब्लाक, ग़ाज़ीपुर) के मुताबिक़ प्रधान जी किसी को मस्टर रोल नहीं दिखाते, खुलेआम फ़र्ज़ीवाड़ा करते हैं। बीडीओ से शिक़ायत की तो जवाब मिला कि प्रधान तो आख़िर तुम्हीं लोगों ने चुना है तो अब हम क्या करें?
कृष्णानंद यादव (लांबी गांव, बभनी ब्लाक, सोनभद्र) के गांव में दो साल पहले कुएं की खुदाई हुई, 16-17 मज़दूरों ने काम किया लेकिन मज़दूरी का भुगतान अभी तक नहीं हो सका है। उन्हीं के गांव में विश्वनाथ जैसे दर्ज़नों लोगों को कभी काम ही नहीं मिला। बताते चलें कि पिछले साल इस गांव में डेढ़ सौ से अधिक शौचालय बनाये गये थे जो छह माह भी नहीं चले और ढह गये।
भय्या लाल पिछले 20 सालों से चित्रकूट के मऊ और मानिकपुर ब्लाक में कोल आदिवासियों के हित-अधिकारों को लेकर सक्रिय हैं। बताते हैं कि 2011-12 में दोनों ब्लाक की अधिकतर ग्राम पंचायतों में जाब कार्डधारी परिवारों को सौ दिन काम की गारंटी नहीं मिल सकी। काम मिला तो भुगतान में ख़ूब लेटलतीफ़ी हुई और भुगतान हुआ भी तो अमूमन 120 रूपये प्रतिदिन के हिसाब से यानी हर कार्य दिवस पर हर मज़दूर की मज़दूरी से पांच रूपये की कटौती। उदाहरण के तौर पर वे मानिकपुर के दर्ज़नों पंचायतों का नाम लेते हैं- गढ़चपा, छेदियाखुर्द, इटवां, मनगवां, मड़ैयन आदि। मऊ की छह और मानिकपुर की 25, कुल 31 ग्राम पंचायतों में तो वन विभाग ने मनरेगा को लोगों की स्थाई आजीविका छीनने का औज़ार बना डाला। खेती की ज़मीन पर पौधारोपण करवा दिया गया। एक ओर जंगल बेरहमी से काटे जा रहे हैं, दूसरी ओर जंगल बढ़ाने के लिए लोगों की ज़मीनों पर हमला है। मनरेगा की यह सबसे बड़ी उलटबांसी है।
शिमला देवी (पतौना गांव, कटहरी ब्लाक, अंबेदकर नगर) सजग और जुझारू महिला हैं। उन्होंने अपने जैसे ग़रीब-गुरबों को मनरेगा के सोशल आडिट के लिए जुटाया। यह मुश्क़िल और चुनौती भरा काम था, एक तरह से प्रधान जी के ख़िलाफ़ मोर्चा खोलने की तैयारी जैसा। बहरहाल, सीमित दायरे में ही सही लेकिन सोशल आडिट हुआ और इतने में ही तीन फ़र्ज़ी जाब कार्ड का भेद खुल गया। तीनों में साल में 150 दिन का काम दर्ज़ था। चौथा कार्ड ऐसा भी था जिसका मुखिया पांच साल पहले मर चुका है और बाक़ी सदस्यों ने कभी मज़दूरी ही नहीं की लेकिन उसे पूरे सौ दिनों के काम के ब्यौरों से भर दिया गया। लखनऊ तक इसकी शिक़ायत पहुंचायी गयी, कार्रवाई के लिए फ़ाइल वापस जिले तक पहुंची भी लेकिन वहीं अटकी पड़ी है। लाखों रूपयों का घोटाला हुआ मगर उसके ख़िलाफ़ कोई हरक़त नहीं।
आशीष कुमार (फ़र्रुखाबाद गांव, ब्लाक चिनहट, लखनऊ) का जाब कार्ड पिछली प्रधानी के समय बना था लेकिन नया प्रधान उन्हें काम ही नहीं देता। तीन साल पहले एक महीने का काम मिला था लेकिन अभी तक उसकी मज़दूरी का भुगतान बक़ाया है। उन्हीं के गांव के अर्जुन ने 42 दिन काम किया लेकिन मज़दूरी का भुगतान हुआ कुल 13 दिन का।
सोशल आडिट में उभरी गड़बड़ तसवीर
क़ानून कहता है कि काम के इच्छुक हर परिवार के नाम जाब कार्ड बनना चाहिए लेकिन हर पंचायत में औसतन 23-24 परिवार इससे वंचित हैं। इससे उलट 130 परिवार ऐसे भी हैं जिनके पास एक से अधिक जाब कार्ड हैं- प्रति पंचायत औसतन 12 परिवारों में।
सरकारी दावा है कि मनरेगा के तहत जितने भी मजदूरों को काम मिला, उन सभी ने कार्य हेतु आवेदन किया था जिसकी तिथिवार सूचना मनरेगा की बेबसाइट पर बाक़ायदा दर्ज़ है। लेकिन सोशल आडिट में शामिल 50 फ़ीसदी मजदूरों ने बताया कि उन्होंने काम के लिए कभी आवेदन नहीं किया। उन्हें जब भी काम मिला, बिना आवेदन के मिला। इनमें से अधिकतर को पता ही नहीं कि काम के लिए आवेदन भी करना होता है।
क़ायदे से काम के आवेदन की पावती मिलनी चाहिए और आवेदन के 15 दिन के भीतर काम मिल जाना चाहिए लेकिन अपनी गरदन कौन फंसाये? सो, जिन 579 मज़दूरों ने काम का आवेदन किया, उनमें से किसी को भी इसकी पावती नहीं दी गयी। पावती नहीं तो बेरोजगारी भत्ते की दावेदारी का आधार ही नहीं।
लगभग सभी मज़दूरों की शिक़ायत है कि कार्यस्थल से मस्टररोल ग़ायब रहता है, बिरले ही दिखता है। मस्टररोल पर कुल 30 फ़ीसदी मजदूरों ने हाजिरी भरी है लेकिन नियमित रूप से लगभग कभी नहीं। अब ऐसा भी नहीं कि हाज़िरी भरी ही नहीं जाती। कुछ तो हिसाब रखना ही होता है। इसके लिए कहीं रजिस्टर होता है तो कहीं कापी-डायरी वरना सादे कागज से ही काम चला लिया जाता है। मतलब कि मस्टररोल अपनी सहूलियत के हिसाब मुताबिक़ बाद में भर दिया जाता है। धांधली का पिटारा इस तरह बंधता है।
मनरेगा में साफ़ हिदायत है कि काम पूरा होने के 15 दिन के भीतर मज़दूरी का भुगतान हो जाना चाहिए। लेकिन 90 फ़ीसदी मज़दूरों को समय से मज़दूरी कभी नहीं मिली। 22 मज़दूर ऐसे भी मिले जिनकी मज़दूरी के भुगतान में एक साल से भी अधिक का समय लग गया।
मस्टररोल और जाब कार्ड में दर्ज़ ब्यौरे कहीं इक जैसे नहीं मिले। मस्टररोल बताते हैं कि 27 परिवारों को पूरे सौ दिन काम मिला जबकि सोशल आडिट में यह संख्या सात परिवारों से आगे नहीं बढ़ सकी। मस्टररोल के मुताबिक़ सभी मजदूरों को सवा सौ रूपये प्रतिदिन की दर से मजदूरी का भुगतान किया गया जबकि 40 फ़ीसदी से भी अधिक मज़दूरों का बयान इसे सरासर झूठ करार देता है।
पूरी दुनिया में हर स्तर पर महिलाओं और विकलांगों को बराबर का मौक़ा और सम्मान दिये जाने की पैरवी है। मनरेगा में भी उनके लिए ख़ास प्रावधान हैं लेकिन अमूमन उनकी अनदेखी होती है। आम शिक़ायत है कि मनरेगा में महिलाओं को कमज़ोर और विकलांगों को नाक़ाबिल मानने की समझ हावी रहती है और जो उनकी गरिमा को घायल करती है। और अक़्सर उन्हें काम के अधिकार से वंचित कर देने का काम करती है।
कार्यस्थल पर पीने का पानी, दोपहर की छुट्टी के समय छायादार जगह और किसी दुर्घटना की स्थिति में प्राथमिक उपचार जैसी सहूलियत हमेशा नदारद रहती हैं। मांओं के साथ कार्यस्थल पर आनेवाले छोटे बच्चों की देखरेख के लिए कोई बंदोबस्त नहीं होता। कुल मिला कर कहें तो मनरेगा के तमाम प्रावधान काग़ज़ों से बाहर निकल कर ज़मीन पर नहीं उतर पाते। (आलेख और तसवीरें: आदियोग)