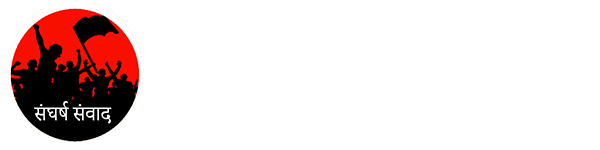परमाणु लॉबी का बंधक बना भारतीय लोकतंत्र
तो फिर इस उल्टी कहानी में परमाणु डील में अमेरिका, रूस और फ्रांस आदि देशों से रिएक्टर खरीदने का सौदा पहले हो जाने के बाद देश के अन्दर परमाणु ऊर्जा के पक्ष में माहौल बनाना और इसके रास्ते में आने वाली हर आर्थिक, कानूनी और लोकतांत्रिक अड़चन को हटाने का एक सिलसिला शुरू हुआ. विदेशी कम्पनियां बिना जोखिम उठाए रिएक्टर बेच पाएं, इसके लिए उनके मुनाफिक परमाणु दायित्व क़ानून (Nuclear Liability Act) बनाया गया। परमाणु ऊर्जा विभाग के अन्दर जो वैज्ञानिक विदेशी रिएक्टरों के खिलाफ थे उनको चुप कराया गया. परमाणु बिजलीघरों की लाइसेंसिंग और उनके सुरक्षा नियमन के लिए जिम्मेवार परमाणु ऊर्जा नियमन बोर्ड (Atomic Energy Regulatory Board – AERB) को ख़त्म करके एक नई प्रस्तावित इकाई – परमाणु सुरक्षा नियमन प्राधिकरण (Nuclear Safety Regulatory Authority) के गठन की कवायद शुरू हुई जो कहने को तो स्वतंत्र है, लेकिन इसके पास लाइसेंसिंग और नियमन के अधिकार सीमित हैं और यह विदेशी रिएक्टरों की सुरक्षा की स्वतंत्र जांच रिएक्टरों का सौदा होने से पहले नहीं कर सकेगी. परमाणु विभाग से जुडी जानकारी देश की जनता के साथ बांटने में राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पर पहले भी कोताही बरती जाती रही है, लेकिन कूड़नकुलम परियोजना की सुरक्षा से जुडी जानकारी खुद सूचना आयोग के अध्यक्ष को भी नहीं दी गई। इसके साथ ही देश भर में ज़मीन पर इन नई रिएक्टर परियोजनाओं का विरोध कर रहे लोगों का निर्मम दमन शुरू हुआ. तमिलनाडु के कूड़नकुलम में दस हज़ार से ज़्यादा लोगों पर रिएक्टर का शांतिपूर्ण विरोध करने के कारण देशद्रोह और भारतीय राज्य के खिलाफ युद्ध छेदने के आरोप में मुकदमे दर्ज किए गए हैं। इन हज़ारों लोगों में महिलाएं और किशोर भी शामिल है। कूड़नकुलम में संघर्ष कर रहे लोग आम मछुआरे हैं जिन्हें जीविका और सुरक्षा के सवाल सता रहे है। कूड़नकुलम में पुलिसिया कारवाईयों में अब तक दो लोगों की जान जा चुकी है. ऐसे ही महाराष्ट्र के जैतापुर में एक मछुआरे की पुलिस फायरिंग में मौत हो चुकी है. देश के अन्य हिस्सों – हरियाणा के फतेहाबाद, गुजरात के मीठी विर्दी, आन्ध्र प्रदेश के कोवादा, मध्य प्रदेश के चुटका और राजस्थान के रावतभाटा में नए रिएक्टरों और परमाणु ईंधन प्रकल्प का विरोध कर रहे लोगों के प्रति भी सरकार का रवैया ऐसा ही छल और दमन भरा है. देश भर के परमाणु-विरोधी आन्दोलनों की उपेक्षा और दमन को मनमोहन सिंह सरकार द्वारा विदेशी कंपनियों को रिएक्टर खरीद के लिए किए जा चुके वादों की पृष्ठभूमि में देखें तो ऐसा लगता है जैसे आम लोग एक ऐसी सरकार से गुहार कर रहे हैं जिसने खुद उनको मारने की सुपारी ले रखी हो.
परमाणु खतरे के साए में लोकतंत्र और मानवाधिकार
भारत और अमेरिका के बीच हुए परमाणु सौदे को तब दुनिया के ‘सबसे बड़े लोकतंत्र’ और ‘सबसे पुराने लोकतंत्र’ के मिलन का नाम दिया गया था। लेकिन जब कूड़नकुलम और जैतापुर जैसी परियोजनाओं के अंतर्गत आने वाली दर्जनों स्थानीय ग्राम-पंचायतों की तरफ से आम राय में विरोध का प्रस्ताव आता है, तब किसी को इस असली लोकतंत्र की इज्ज़त याद नहीं आती। देश के लोकतंत्र और न्यूनतम शर्म का भी गला घोंट कर दिसंबर 2010 में ठीक फ्रांसीसी राष्ट्रपति के आगमन की पूर्व-संध्या पर जैतापुर परियोजना को आनन-फानन में पर्यावरणीय मंजूरी दे दी गयी, जिसके बारे में खुद तत्कालीन वन एवं पर्यावरण मंत्री जयराम रमेश ने स्वीकार किया कि इस मंजूरी में अंतरर्राष्ट्रीय रिश्तों को तरजीह दी गयी। ठीक इसी तरह हिलेरी क्लिंटन की भारत यात्रा से पहले संसद से वह परमाणु दायित्व बिल पास कराया गया, जिस पर बहस के दौरान स्वास्थ्य, गृह, और पर्यावरण समेत आठ मंत्रालयों के सचिव यह कह चुके थे कि उनके मंत्रालय किसी बड़ी परमाणु दुर्घटना की स्थति से निपटने के लिए तैयार नहीं हैं। विपक्ष के कुछ दलों के दबाव में दुर्घटना की मुआवजा राशि बढ़ाकर 500 से 1500 करोड़ ज़रूर की गई . लेकिन परमाणु दुर्घटना के आर्थिक दुष्परिणाम इससे कहीं अधिक होते हैं और फुकुशिमा में सिर्फ साईट की सफाई में अगले पचीस सालों में 600 बिलियन डॉलर खर्च होने की उम्मीद है, इसमें दुर्घटनाग्रस्त प्लांट के 20 किलोमीटर के दायरे से विस्थापित लाखों लोगों के जीविका के नुकसान और आने वाले दशकों में होने वाले स्वास्थ्य और पर्यावरण की क्षति शामिल नहीं है. लेकिन एक क्रूर आश्चर्य यह है कि भारत में रिएक्टर लगाने को आतुर विदेशी कंपनियों को 1500 करोड़ का सीमित मुआवजा भी मंज़ूर नहीं है. संसद में 2010 में यह क़ानून पास होने के बाद इन कंपनियों के दबाव में सरकार ने उक्त क़ानून के तहत बनाए गए विस्तृत नियमों (सिविल लायबिलिटी फॉर न्यूक्लियर डैमेज रूल्स, 2011) के अंतर्गत ऐसे प्रावधान डाले जो मूल क़ानून की भावना के ही खिलाफ है। इसमें विदेशी परमाणु कंपनियों का दायित्व घटाकर 5 साल करना और मुआवजे की राशि को खरीदे गए मशीन की कीमत से जोड़ना जैसी चालबाजी शामिल है. सवाल यह उठता है की अगर परमाणु ऊर्जा इतनी ही सुरक्षित है जितने इसके दावे बड़े-बड़े लोग कर रहे हैं, तो फिर परमाणु कम्पनियों को मुआवजे का वायदा भर करने से क्या दिक्कत है? और अगर ये कम्पनियां अपने ही उत्पाद पर इतना भरोसा नहीं करतीं की अपनी आर्थिक सेहत दाँव पर लगाएं, तो फिर देश के आम गरीब लोगों से यह अपेक्षा क्यों की जा रही है की वो अपनी ज़िंदगी अपनी जीविका, अपना सर्वस्व इन परियोजनाओं के लिए दाँव पर लगाएं जबकि इन रिएक्टरों की बिजली और इससे पैदा होने वाला ‘विकास’ उन तक वैसे भी नहीं पहुँचाने वाला है.
दुर्घटना के दायित्व की तरह ही परमाणु रिएक्टरों की सुरक्षा और उनके पर्यावरणीय प्रभावों पर लोगों की चिंता को भी सरकार इसी तरह की धूर्तता और दमन से किनारे कर रही है. फुकुशिमा दुर्घटना के बाद जापान, जर्मनी, ईटली, स्वीडन और स्विट्ज़रलैंड से लेकर फ्रांस तक परमाणु ऊर्जा पर अपनी निर्भरता कम करने में लगे हैं और पूरी दुनिया में जनमत का रुझान परमाणु ऊर्जा के खिलाफ है, जैसा कि 2011 में बीबीसी द्वारा एक वैश्विक सर्वेक्षण से पता चला. लेकिन इस समझदारी के उलट भारत में न सिर्फ ज़मीनी परमाणु-विरोधी आन्दोलनों पर जबरदस्त दमन ढाया जा रहा है बल्कि सरकार के शीर्ष स्तर से इन जनांदोलनों के विदेशी हाथ से प्रेरित होने जैसे दुष्प्रचार किए जा रहे हैं . प्रधानमंत्री के दावों के उलट कूड़नकुलम में अब तक किसी विदेशी हाथ का पता सरकार नहीं लगा सकी है. केंद्र सरकार ने पिछले साल NIMHANS के मनोचिकित्सकों को कूड़नकुलम के लोगों की मदद के लिए भेजा जिसे जन-भावनाओं के साथ एक क्रूर मजाक ही कहा जा सकता है. परमाणु कंपनियों को किए गए वादों के दबाव में सरकार ने ऐसे ही पर्यावरणीय मंजूरी के लिए आयोजित की जाने वाली जन-सुनवाइयों को भी मज़ाक में तब्दील कर दिया है. इसी मार्च में गुजरात के मीठी विरदी हुई जन-सुनवाई में स्थानीय लोगों ने इस प्रक्रिया का बहिष्कार किया और जमकर विरोध किया. सरकार की जेबी संस्थाओं द्वारा तैयार पर्यावरणीय प्रभावों के अध्ययन पर पर्यावरण मंत्रालय के निर्देशों के तहत होने वाली स्थानीय रायशुमारी की खानापूर्ति करने अफसरों को लोगों ने भगा दिया और मीटिंग हुई ही नहीं। ठीक ऐसा ही पिछले साल अगस्त में हरियाणा के गोरखपुर में हुआ. इन घटनाओं की मीडिया में रिपोर्टिंग भी हुई, लेकिन इसके बावजूद स्थानीय प्रशासन ने इन जगहों पर जन सुनवाइयों के सफल होने और स्थानीय लोगों का परियोजना को समर्थन मिलने का दावा मंत्रालय को भेजी अपनी रिपोर्टों में किया. इन फर्जी पर्यावरणीय प्रभाव अध्ययनों को तैयार करने वाली एजेंसियों के पास परमाणु विकिरण से सम्बंधित विशेषज्ञता और परमाणु परियोजनाओं का अध्ययन करने के लिए ज़रूरी आधिकारिक मान्यता (accredition) तक नहीं है. हाल के महीनों में पीयूसीएल, एमनेस्टी इंटर्नेशनल और ह्यूमन राइट्स वाच जैसी अग्रणी मानवाधिकार संस्थाओं द्वारा परमाणु ऊर्जा के लिए संविधान और आम लोगों के दमन पर चिंता जताया जाना वाजिब है. जस्टिस राजेन्द्र सच्चर, जस्टिस ए.पी. शाह और जस्टिस सोली सोराबजी जैसे वरिष्ठ विधिवित्ताओं ने भी परमाणु ऊर्जा विभाग द्वारा विभिन्न मामलों में किए जा रहे कानूनी उल्लंघनों पर खुल के विरोध किया है.
क़ानून को ताक पर रखने की इतनी जल्दी क्यों है?
आखिर किया वजह है की परमाणु ऊर्जा को आगे बढाने के लिए इतने बड़े स्तर पर संविधान को दरकिनार किया जा रहा है? सौर ऊर्जा जैसे नवीकरणीय विकल्प जो दुनिया भर में उन्नत, लोकप्रिय और सस्ते साबित हो रहे हैं, भारत में पनपने न पाए इसके लिए परमाणु ऊर्जा विभाग के अध्यक्ष पद से रिटायर सज्जन को सौर ऊर्जा परियोजनाओं की जिम्मेदारी दे दी गयी है, क्या यह परस्पर विरोधी हितों को अलग रखने के न्यूनतम संवैधानिक आदर्श का उल्लंघन नहीं है? अगर हम परमाणु ऊर्जा के पक्ष में मीडिया में चल रहे सरकारी प्रचार से परे जा कर देखें तो हमें स्वतंत्र विशेषज्ञों, नागरिक आन्दोलनों और जादूगोड़ा से लेकर हिरोशिमा-फुकुशिमा और चेर्नोबिल तक के लोगों की सच्चाई का एहसास होगा और यह भी समझ आएगा की इस हकीकत को दबाने के लिए ही मानवाधिकारों और कानूनों के खुलेआम उल्लंघन की ज़रुरत शासकवर्ग को पड़ रही है.
कारपोरेट और सरकारी दावों के उलट न तो परमाणु ऊर्जा सुरक्षित है, न ही सस्ती और न ही यह ग्लोबल वार्मिंग से निपटने का कोई सही उपाय है. भारत में पहले से चल रहे अणु-बिजलीघर भी फ़ुकुशिमा जैसी त्रासदी की सम्भावना से मुक्त नहीं हैं. मुम्बई के बहुत नजदीक स्थित तारापुर रिएक्टर अमेरिकी कम्पनी जी.ई. (General Electrics) के उसी मार्क-वन डिज़ाइन के रिएक्टर हैं, जो फ़ुकुशिमा में हैं. इन रिएक्टरों में द्वितियक नियंत्रण ढाँचे (secondary containment structure) का अभाव है और शेष ईंधन (spent fuel) रिएक्टर के ऊपरी हिस्से में जमा होता है. तारापुर में पिछले चार दशकों से इकट्ठा यह अत्यधिक रेडियोधर्मी कचरा अमेरिका न तो वापस ले जा रहा है और ना ही भारत को इसे पुनर्संश्लेषित (reprocessing) करने दे रहा है. उत्तरप्रदेश के नरोरा स्थित परमाणु-संयत्र में शीतन के लिये जरूरी बिजली पूरे २४ घंटे गुल होने और नियंत्रण-कक्ष की मशीनें फुँक जाने की घटना १९९३ में हो चुकी है. जपान के अब तक दुनिया के सबसे सुरक्षित और तकनीक-सम्पन्न माने जाने वाले रिएक्टरों में मची तबाही और अफ़रा-तफ़री से यह साफ़ दिख जा रहा है कि परमाणु तकनीक अपनेआप में असुरक्षित है और कितनी कोशिशों के बाद भी एक छोटी सी चूक, प्राकृतिक आपदा या आतंकी घटना इन बिजलीघरों को दशकों के लिए जानलेवा बना सकती है.
आजकल परमाणु ऊर्जा के को कार्बन मुक्त और जलवायु परिवर्तन का हल बताया जाता है. लेकिन अणु-ऊर्जा के उत्पादन में युरेनियम खनन, उसके परिवहन से लेकर रिएक्टर के निर्माण तक काफी कार्बन खर्च होता है जिसकी गिनती नहीं की जाती. अणु-ऊर्जा से बिजली बनती है, गाड़ियाँ नहीं चलतीं और पेट्रोल के अत्यधिक इस्तेमाल से हो रहे पर्यावरणीय नुकसान के मामले में यह कोई विकल्प नहीं है. मैसाचुसेट्स तकनीकी संस्थान (MIT) के अनुसार जलवायु-परिवर्तन को कुछ हद तक रोकने के लिये कम-से-कम एक हज़ार परमाणु रिएक्टर चाहिए जबकि एक रिएक्टर के निर्माण में आठ से दस साल तक लगते हैं. २०५० तक अगर पूरी दुनिया में परमाणु बिजली उत्पादन चगुना भी कर दिया जाय तो इससे होने वाली कुल कार्बन कटौती सिर्फ़ चार प्रतिशत ही होगी, जबकि २०२० के उच्चतम कार्बन उत्सर्जन के स्तर के बाद २०५० तक दुनिया में ८० से ९० प्रतिशत कार्बन कटौती की ज़रूरत होगी. ऐसे में, जलवायु परिवर्तन से बचने के लिये परमाणु विकल्प एक धोखा भर है. साथ ही फ़ुकुशिमा ने यह भी साबित कर दिया है कि जलवायु परिवर्तन का समाधान होने की बजाय अणु-ऊर्जा केन्द्र दरअसल बदलते जलवायु और भौगोलिक स्थितियों को झेल नहीं पाएंगे क्योंकि इन्हें बनाते समय वे सारी स्थितियां सोच पाना मुमकिन नहीं जो जलावायु-परिवर्तन भविष्य में अपने साथ लेकर आ सकता है. चालीस साल पहले फ़ुकुशिमा के निर्माण के समय जापान में इतनी तेज सुनामी की दूर-दूर तक सम्भावना नहीं थी, वैसे ही जैसे भारत में कलपक्कम अणु-ऊर्जा केंद्र को बनाते समय सुनामी के बारे में नहीं सोचा गया था. अधिकतम पचास-साठ साल तक काम करने वाले इन अणु-बिजलीघरों में उसके बाद भी हज़ारों सालों तक रेडियोधर्मिता और परमाणु-कचरा रहता है. ऐसे में, इतने लम्बे भविष्य की सभी भावी मुसीबतों का ध्यान रिएक्टर-डिजाइन में रखा गया है, यह दावा आधुनिकता और तकनीक के अंध-व्यामोह के अलावा कुछ नहीं कहा जा सकता है.
परमाणु बिजली भारत की ऊर्जा-सुरक्षा का हल नहीं है. पूरे सरकारी समर्थन और संरक्षण के बावजूद परमाणु ऊर्जा विभाग अपने ही निर्धारित लक्ष्यों पर हर बार बुरी तरह असफल रहने के मामले में भारत सरकार का सबसे निकम्मा विभाग साबित हुआ है.१९६२ में खुद होमी भाभा ने दावा किया था कि १९८७ तक भारत में १८-२० हज़ार मेगावाट की परमाणू बिजली क्षमता होगी. असल में १९८७ में परमाणु बिजली क्षमता १.०६ हज़ार मेगावाट – भाभा के आकलन का लगभग पाँच प्रतिशत – रही. भाभा के बाद परमाणु ऊर्जा आयोग की कमान सम्भालने वाले विक्रम साराभाई ने खुद स्वीकार किया कि यह कार्यक्रम ’अपने लक्ष्य से बुरी तरह पिछड़ चुका है’. इस खाई को पाटने के लिये १९७२ से प्रतिवर्ष ५०० मेगावाट क्षमता के रिएक्टर जोड़ने की बात साराभाई ने की, लेकिन ५०० मेगावाट का पहला रिएक्टर तारापुर में कुल पैंतीस साल बाद २००५ में अस्तित्व में आया. इस पिछड़ेपन को आमतौर पर १९७४ के परीक्षण के बाद आने वाली दिक्कतों के माथे मढ़ दिया जाता है, लेकिन १९८४ में भी परमाणु ऊर्जा आयोग की योजना के मुताबिक वर्ष २००० तक १०,००० मेगावाट बिजली का लक्ष्य घोषित किया गया था. यह १९८९ की योजना में भी दुहराया गया और यह विश्वास दिखाया गया कि यह लक्ष्य पूरी तरह प्राप्य है. २००३ में जब आयोग इस लक्ष्य के नज़दीक भी नहीं पहुँच पाया तो आयोग के अध्यक्ष अनिल काकोडकर ने अगले चार सालों में ६८०० मेगावाट बिजली का नया लक्ष्य सामने रखा. परमाणु ऊर्जा विभाग का इतिहास यह बताता है कि इसके पिछले दस रिएक्टर अपने निर्धारित समय के वर्षों देर से शुरु हो पाए और इससे उनकी लागत में ३०० प्रतिशत से अधिक का इज़ाफ़ा हुआ. २०१० में कुल उत्पादन ४१२० मेगावाट रहा जो देश में पैदा कुल बिजली का तीन प्रतिशत से भी कम है. ध्यान रहे कि भारत में दूरस्थ बिजलीघरों से शहरों और गावों के उपभोग केंद्रों तक बिजली पहुँचाने के दौरान होने वाला नुकसान (Transmission loss) तीस प्रतिशत से भी ज़्यादा है.
विज्ञान परमाणु कचरे का कोई समाधान अब तक नहीं ढूँढ पाया है और ज़्यादातर रिएक्टरों के आसपास ही इसे सिर्फ़ भंडारित करके रखा जाता है. एक औसत रिएक्टर साल भर में २० से तीस टन उच्च-स्तरीय जहरीला कचरा निकालता है. इसमें प्लूटोनियम-२३९ (अर्ध-आयु २४,००० साल) और युरेनियम-२३५ (७१० मिलियन वर्ष) से लेकर नेप्चूनियम, स्ट्राँशियम, सीज़ियम, और ट्रीशियम जैसे कई अन्य जहर भी होते हैं जो कई दशकों तक जानलेवा बने रहते हैं. इन जहरीले पदार्थों की कोई भी खुराक सुरक्शःइत नहीं होती और अपने सम्पर्क में आने वाली आबादी से लेकर पेड़-पौधों तक में इनके विकीरण से दूरगामी दुष्प्रभाव पड़ते हैं.
परमाणु खतरे के अंधे कुएं से बचाव ज़रूरी
इस मार्च की 11 तारीख को फुकुशिमा परमाणु दुर्घटना के दो साल पुरे हुए. यह उस दुर्घटना की बरसी नहीं है, क्योंकि दुर्घटना अभी भी जारी है। फुकुशिमा के बीस किलोमीटर के दायरे से विस्थापित हुए लोगों को घर-वापसी की कोई आशा नहीं दिख रही, रिएक्टरों से अभी भी खतरनाक विकिरण रिस रहा है जो आने वाली कई सदियों तक जानलेवा बना रहेगा. इस सन्दर्भ में दुर्घटनाएं कार चलाने से लेकर सड़क पार करने तक में होती हैं, जैसे तर्क सिर्फ घटिया ही नहीं, निर्मम भी हैं। फुकुशिमा के बाद उभरे तथ्यों ने जापान जैसे तकनीकी और प्रशासनिक रूप से उन्नत देश के बारे में भी यह साबित कर दिया की परमाणु-उद्योग राजनेताओं और मीडिया के गठजोड़ ने कैसे न सिर्फ लोगों को इतने सालों तक रिएक्टरों के दुष्प्रभावों से ओझल रखा, बल्कि दुर्घटना के समय और उसके बाद भी उसके प्रभावों के बारे में खतरनाक गोपनीयता बरती। सोवियत रूस के ज़माने में 1986 में हुई चेर्नोबिल परमाणु दुर्घटना की सत्ताईसवीं बरसी इसी अप्रैल की 26 तारीख को उस इलाके के लोग मनाएंगे, जो अब युक्रेन में पड़ता है. परमाणु विकिरण और दुर्घटनाओं के दुष्प्रभाव इतने विनाशकारी और दूरगामी होते हैं की समय के साथ राजनीतिक मानचित्र बदल जाते हैं लेकिन इंसानियत को उसकी मार झेलनी पड़ती है. ऐसे में, सीमित और तात्कालिक राजनीतिक तथा आर्थिक हितों की पूर्ति के लिए देश के आम लोगों की सुरक्षा और संवैधानिक संस्थाओं को परमाणु महत्वाकांक्षाओं की बलि चढने से किसी भी हाल में रोका जाना चाहिये.
लेखक परिचय: लेखक परमाणु निरस्त्रीकरण और शान्ति गठबंधन (Coalition for Nuclear Disarmamenta and Peace) के शोध-सलाहकार हैं। परमाणु मसलों से जुडी जानकारी, बहसों और दस्तावेजों के लिए इनकी वेबसाईट www.dianuke.org एक अच्छा ठिकाना है.