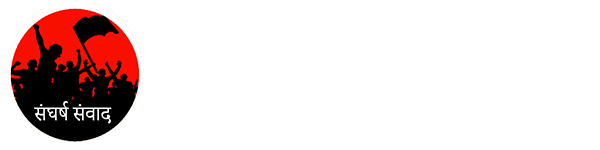मध्य प्रदेश : जंगल बचा रहे अलीराजपुर के आदिवासी
आजादी के पचहत्तर साल में वन अधिकार पर अब जाकर कुछ बातें हो रही हैं और परंपरागत वनवासियों को कहीं-कहीं पट्टे दिए भी दिये जा रहे हैं, लेकिन कुछ आदिवासी इलाके ऐसे हैं जहां जंगल को बचाने का विवेक और तकनीक बरसों से कायम है। मध्य प्रदेश का अलीराजपुर ऐसा ही एक जिला है, जिसे सबसे पिछड़ा माना जाता है, लेकिन यहां के लोग अपने अधिकारों को लेकर सबसे जागरूक दिखाई देते हैं। प्रस्तुत है, इसी पर आदित्य सिंह की एक रिपोर्ट;
मगन और गुजालिया दो भाई आज जंगल में निकले हैं आज उनकी ड्यूटी है जंगल संभालने की। अलीराजपुर के ककराना गांव के ये भील आदिवासी बारी-बारी से अपने जंगल की ख़ैर-खबर लेने निकलते हैं। दोनों भाईयों ने सुबह से जंगल में कई पेड़ों को देखा, छोटे पौधों के आसपास झाड़ी लगाई, पानी के गड्ढों के किनारे से गंदगी साफ की और उंची नीची पहाड़ियों से होते हुए दोपहर बाद अपने घर लौट आए। अब गांव का एक दूसरा परिवार ऐसा ही करेगा।
ये जंगल अलीराजपुर जिले के ककराना गांव का है। जहां के लोग इसे पिछले चार दशकों से इसी तरह बचाते रहे हैं। इन लोगों का कहना है कि उनका जंगल सबसे पहले उनकी ही जिम्मेदारी है क्योंकि वे सदियों से इन्हीं जंगलों में रहते आए हैं। ‘संयुक्त राष्ट्र संघ’ ने 2021 से 2030 के दशक को ‘पारिस्थितिक तंत्र की बहाली का दशक’ घोषित किया है और दुनिया भर में इसके लिए काम हो रहा है। अलीराजपुर के आदिवासियों के द्वारा अपने जंगलों के प्रति किया जा रहा ये काम ‘संयुक्त राष्ट्र संघ’ के इस अभियान का एक बेहतरीन उदाहरण है।
साल 2022 में ककराना गांव को ‘अनुसूचित जनजाति और अन्य पारंपरिक वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006’ (वनाधिकार कानून) के तहत सामुदायिक पट्टा मिला है। जिले में अब कई गांवों में लोग इसी अधिकार के तहत अपने जंगलों को संवार रहे हैं। इनमें ककराना में हो रहा काम सबसे अच्छा माना जाता है। ‘वनाधिकार कानून’ यानी अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासियों के अधिकारों की मान्यता से इंसान और जंगल के बीच का यह रिश्ता और मजबूत हुआ है।
2011 की जनगणना के मुताबिक अलीराजपुर देश में सबसे अधिक अशिक्षित जिला था। इसके बाद स्थितियां कुछ बेहतर हुईं, लेकिन बहुत ज्यादा अंतर अब भी नहीं है। अशिक्षा के बावजूद यहां के आदिवासियों ने जंगलों के प्रति अपनी जिम्मेदारी और ‘वनाधिकार कानून’ पर शानदार तरीके से अमल किया है और वे अपने सदियों पुराने जीवन जीने के तरीके और संस्कृति को फिर से अपना रहे हैं। संस्कृति, जिसमें वन और मानव अलग-अलग नहीं थे।
‘वनाधिकार कानून’ के प्रावधानों के तहत वनभूमि और वन्य संसाधनों का उपयोग करने के लिए अनुसूचित जनजातियों और अन्य पारंपरिक वन निवासियों के पात्र व्यक्तियों और समुदायों के अधिकारों को मान्यता दी जाती है। इसके तहत आने वाले व्यक्तिगत अधिकारों में वनभूमि पर खेती और निवास का अधिकार भी शामिल है। वहीं वनभूमि में जानवरों की चराई, जलस्त्रोतों तक पहुंच, मछली पकड़ना, पारंपरिक मौसमी संसाधनों तक पहुंच और इन संसाधनों के प्रबंधन आदि को इस कानून के तहत मिलने वाले सामुदायिक अधिकारों में शामिल किया गया है।
अलीराजपुर का ‘खेड़ूत मजदूर चेतना संगठ’ 80 के दशक से कुछ ऐसे ही विचारों पर काम करता आ रहा है। आदिवासी जो अपने जंगलों को खुद बचाना चाहते हैं, उनमें निवास और उपयोग के अधिकार की उम्मीद रखते हैं जिससे पारिस्थितिकी तंत्र न बिगड़े। इसके तहत इस संगठन ने साल 1983 में अट्ठा गांव से काम शुरु किया। यहां पुरुषों और महिलाओं ने अपनी ‘ढास’ (सामूहिक श्रम) परम्परा के अनुसार पारंपरिक सामुदायिक श्रम के तहत अपने जंगलों की रक्षा करने का फैसला किया। ‘ढास’ परम्परा के तहत सभी लोग बारी-बारी से श्रमदान करते हैं और इसी के तहत जंगल के प्रति उन्होंने अपने कर्तव्य को निभाया है।
इस संगठन के सचिव और वयोवृद्ध कार्यकर्ता रूपसिंह पडियार बताते हैं कि कुछ दशकों पहले वन विभाग के कई लोग शहरी ग्राहकों को बेचने के लिए हमारे जंगलों से लकड़ी काट लेते थे और इसका आरोप स्थानीय आदिवासियों पर लगता था। इसलिए हमने अपनी ओर से जंगलों की कटाई बिल्कुल बंद कर दी और बाहरी लोगों से उनकी रक्षा करना शुरू कर दिया। यही जंगल हमारे देवता हैं जो हमें भोजन और आजीविका देते हैं। रूपसिंह बताते हैं कि उस समय कुछ पढ़े-लिखे सामाजिक कार्यकर्ताओं ने लोगों को समझाने में उनकी मदद की। इनमें खेमराज, राहुल बनर्जी, अमित भटनागर, चितरुपा पालित, जयश्री जैसे कार्यकर्ताओं की भूमिका अहम रही, जिन्होंने आदिवासियों को उनकी संस्कृति और वनों को संरक्षित करने के लिए प्रेरित किया।
इसके बाद से ही गांव की महिलाएं और पुरुष मिलकर जंगलों की रक्षा करने लगे। इसी संगठन की एक अन्य अनुभवी सदस्य दहेलीबाई कहती हैं, “महिलाएं ज्यादातर समय जंगलों में जलाऊ लकड़ी, घास, फल, सब्जियां और जड़ी-बूटियां इकट्ठा करने में बिताती थीं। इसलिए हमने सोचा कि जंगल की हर तरह से रक्षा करना होगी और अपने और अपने पशुओं के लिए अधिक पौष्टिक भोजन का इंतज़ाम इन्हीं जंगलों से करना होगा।”
ककराना गांव में यह प्रयास कुछ और भी शानदार दिखाई देते हैं। बारिश में यहां का जंगल खिल उठा है, लेकिन गर्मियों के दौरान भी यहां रौनक कम नहीं होती। गांव को सामुदायिक वन अधिकार मिला है। इसके तहत ककराना गांव के लोग ही इस जंगल की देखभाल करते हैं और ग्रामसभा जंगलों की स्थिति की लगातार समीक्षा करती है।
जंगल की बीते 19 साल से चौकीदारी करने वाले डीलू जंगल में ही बने अपने छोटे से घर में परिवार के साथ रहते हैं। वे दिन भर एक डंडा लेकर जंगल में घूमते हैं। इसके बदले में गांव के लोग चंदा करके उन्हें करीब बीस हजार रुपये सालाना देते हैं। इसके अलावा वे अपनी छोटी सी जमीन पर ज्वार और बाजरे की खेती करते हैं। वे बताते हैं कि पहले गांव का जंगल काटने बहुत से लोग आते थे। उस समय वे गांव वालों के साथ उन लोगों को डराकर भगा देते थे, लेकिन अब कोई जंगल काटने नहीं आता।
सेटलाइट मैप देखने से पता चलता है कि ककराना में 3.85 वर्ग किमी का इलाका हरा-भरा है। यहां गांव और जंगल दोनों का अस्तित्व है। इस तरह यहां करीब 400 हैक्टेयर का जंगल इन्होंने संरक्षित कर रखा है। यहां कोई पेड़ नहीं काटा जाता या किसी तरह से भी जंगल को नुकसान नहीं पहुंचाया जाता। यहां इंसान और जंगल अलग दिखाई नहीं देते।
गांव के लोग जंगल में पड़ी लकड़ियां, घास और थोड़े बहुत पत्ते या अन्य फल वगैरह ला सकते हैं। वे जरुरत के मुताबिक जंगल में अपने मवेशी चरा सकते हैं और वहां उपलब्ध पानी के संसाधनों का उपयोग कर सकते हैं। इसकी जानकारी भी ग्रामसभा को होती है। हालांकि पानी का उपयोग करने की जरुरत यहां नहीं होती क्योंकि ये नर्मदा नदी के बिल्कुल किनारे बसे हुए गांव हैं।
संगठन के शंकर तड़वाल बताते हैं कि जिले में ज्यादातर आदिवासी समाज जंगल में ही रहता है और इससे किसी भी तरह से अलग नहीं है। चार दशक पहले शहर या कस्बों में रहने वाले वनवासियों की संख्या और भी कम थी। उस समय ‘जंगल रोको अभियान’ की शुरुआत की गई। इसका सीधा संदेश यह था कि अपना जंगल केवल वन विभाग के कर्मचारियों के जिम्मे नहीं छोड़ा जा सकता। तड़वाल बताते हैं कि उस समय वन विभाग के साथ उनके अच्छे अनुभव नहीं थे।
अपने अभियान के शुरुआती दिनों के बारे में शंकर बताते हैं कि तब एक परिवार जंगल की रखवाली करता था और फिर लौटते हुए एक निशान किसी अन्य परिवार के घर के बाहर रख देता था। इस तरह जंगल की चौकीदारी की जिम्मेदारी अब उस परिवार की हो जाती थी। यह प्रक्रिया लंबे समय तक जारी रही और अब ये ग्रामसभा के माध्यम से तय किया जाता है कि जंगल की देखभाल कौन करेगा। शंकर बताते हैं कि उनके संगठन ने साल 2021 में ‘वनाधिकार कानून’ के तहत ‘सामुदायिक वनाधिकार पत्र’ की मांग की और पूरी कवायद के बाद साल 2022 में यह अधिकार हासिल किया।
अट्ठा गांव से शुरु हई जंगलों को बचाने की यह परंपरा अब अलीराजपुर के एक बड़े हिस्से में दिखाई देती है। लोग अपने-अपने तरीके से अपना जंगल बचाते हैं। हालांकि पट्टा हासिल करने के बाद कुछेक मामलों में यह प्रयोग बहुत सफल नहीं हैं, लेकिन कहा जा सकता है कि जंगल बचाने वाले जागरुक आदिवासियों की संख्या बढ़ रही है। जिले के झंडाना, सुगट, भिताडा, पुजारा की चौकी, ककराना, सेमलानी, मेहलगांव आदि में जंगलों को बचाने के अच्छे प्रयास हो रहे हैं।
इस इलाके में सक्रिय सामाजिक कार्यकर्ता राहुल बनर्जी बताते हैं कि ‘जंगल बचाओ अभियान’ का महत्व आदिवासियों ने समझा और इसे बहुत गंभीरता से आगे बढ़ाया। यही वजह है कि यह अभियान अब जिले के 70 से अधिक गांवों में फैल चुका है। बनर्जी बताते हैं कि कई गांवों में ‘सामुदायिक वन अधिकार’ के तहत पट्टा दिया गया है और इन सभी में ककराना का वन्य क्षेत्र सबसे आगे है जहां ग्रामीणों ने अपने आसपास का जंगल भी संरक्षित किया है।
साभार : सप्रेस