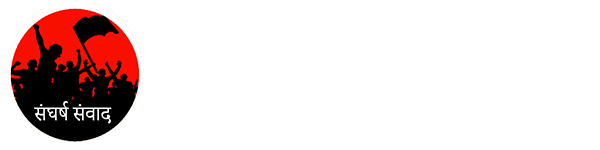लघु वन उत्पादों से बेदखल होते आदिवासी
अपने तरह-तरह के जैविक, सामाजिक और प्राकृतिक उपयोगों के आलावा आजकल जंगल व्यापार-धंधे में भी भारी मुनाफा कूटने के काम आ रहे हैं। इसमें सेठों, सरकारों की बढ़-चढ़कर भागीदारी हो रही है। कैसे किया जाता है, यह कारनामा? और क्या होते हैं, इसके नतीजे? प्रस्तुत है, इसी विषय पर प्रकाश डालता राज कुमार सिन्हा का यह लेख;
देश के 625 जिलों में से 190 जिलों में आदिवासी निवास करते हैं, जहां 65 प्रतिशत जंगल हैं। यह इसलिए हुआ क्योंकि आदिवासी ने हर समय जंगल को जीवनदायी व्यवस्था के रूप में माना और यही बात उनकी समाज व्यवस्था की विशेषताओं को चिन्हित करती है। जरूरत से ज्यादा उपयोग नहीं करने एवं कम आवश्यकता वाली अर्थनीति, अपनी जमीन एवं जंगल के मालिक न होकर सहोदर रहने एवं दोहन न करके समान रूप से हिस्सेदारी करने की उनकी आर्थिक, सांस्कृतिक एवं धार्मिक व्यवस्था रही है। उनके संसाधनों पर समाज की मालिकी मानी जाती थी और उनका सामूहिक तौर पर इस्तेमाल करने की प्रथा थी। ब्रिटिश हुकूमत ने जंगल की लूट के लिए कानूनी ढांचा तैयार कर जंगल को नियंत्रित करना शुरू किया जिसके विरुद्ध भारत की अनेकों जन-जातियों ने अभूतपूर्व संघर्ष किया। इसमें लाखों आदिवासी शहीद हुए।
आजादी के बाद विकास के नये दौर में आदिवासी इलाकों में पाये जाने वाले संसाधनों की जरूरत बढ़ने लगी। जिन वस्तुओं का अभी तक कोई मूल्य नहीं था, वे मूल्यवान होती गईं। आदिवासी समुदाय अपने तौर से इन संसाधनों का उचित उपयोग करके शांति से जिंदगी बिताता था। आदिवासी का उनके नये उपयोग से कोई सरोकार नहीं रहा। उनके लिए इमारती लकङी खेती की बागङ बनाने, लौह-अयस्क को पत्थर और नदियों को पवित्र मानने के मूल्य थे, लेकिन आज की औद्योगिक व्यवस्था में आदिवासी इलाकों में पाई जाने वाली हर चीज का नया मूल्य हो गया।
नदी-घाटी पर बांध बनाकर सिंचाई एवं बिजली बनाने और औद्योगिक वस्तुओं के निर्माण के लिए खनिज आवश्यक है। जंगल नई सभ्यता की तरह – तरह की जरूरतों को पूरा करने और पर्यावरण संरक्षण के लिए जरूरी हो गए हैं। आदिवासी विकास के रास्ते में बाधक और अवांछनीय हो गया है और उसके साथ जबरदस्ती बेदखली और विस्थापन का दौर शुरू हो गया। जो भी आदिवासी समुदाय के संवैधानिक अधिकारों और न्याय के लिए आवाज उठाता है, उस पर विकास विरोधी होने और ‘अर्बन नक्सल’ का ठप्पा लगाकर मुद्दे को खारिज करने का खेल शुरू हो जाता है।
वर्ष 1980 में लागू हुए ‘वन संरक्षण अधिनियम’ के बाद वर्ष 2004 तक देश की 11,282 विकास परियोजनाओं के लिए 9.81 लाख हेक्टेयर वनभूमि का गैर-वनीकरण किया गया। वर्ष 2004 से 2013 के बीच 4.07 लाख हेक्टेयर वनभूमि विकास परियोजनाओं एवं तेल और खनन के लिए गैर-वनीकरण में परिवर्तित की गईं। ‘केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री’ ने 20 मार्च 2020 को संसद में जानकारी दी कि 2014 – 15 से 2018-19 के बीच ‘वन संरक्षण अधिनियम– 1980’ के तहत 69,414.32 हेक्टेयर वनभूमि, 3616 परियोजनाओं के लिए दी गई।
हाल के 2023 के संसद के शीतकालीन सत्र में पर्यावरण राज्यमंत्री अश्विनीकुमार चौबे ने सदन में जानकारी दी कि पिछले पांच सालों में 88,903.80 हेक्टेयर वनभूमि अलग- अलग प्रोजेक्ट के लिए गैर-वानिकी उद्देश्य से परिवर्तित की गई है। मध्यप्रदेश के संदर्भ में देखें तो 1980 से 2021-22 तक विभिन्न परियोजनाओं के लिए 2,87,336.711 हेक्टेयर वनभूमि, गैर-वनभूमि में परिवर्तित की गई है।
वनक्षेत्र में आयी कमी, जंगल की जमीन का अवमूल्यन तथा परती भूमि में आयी बढत के कारण ‘पर्यावरण संरक्षण’ या पर्यावरण को बचाने की आवाजें तेज हुई हैं। इसी तरह ‘ग्लोबल वार्मिंग’ का मुद्दा पर्यावरण के क्षरण की तरफ ध्यान खींचता है। पर्यावरण संरक्षणवादियों का उद्देश्य है कि जंगल में बसे आदिवासी समुदाय के पारम्परिक अधिकारों को आमान्य कर जंगल से बेदखल किया जाए, ताकि जंगलों को फिर से हरा – भरा किया जा सके और उसमें वन्यजीवों का संरक्षण किया जा सके।
आज भारत में पूरे वनक्षेत्र के सिर्फ 4 प्रतिशत पर संरक्षित (अभ्यारण्य, राष्ट्रीय-उद्यान, बॉयोस्फियर) क्षेत्र हैं। इसे 16 प्रतिशत तक बढाने की योजना पर काम चल रहा है। इसलिए मध्यप्रदेश में 10 ‘राष्ट्रीय-पार्क’ और 25 ‘अभयारण्य’ के बावजूद 2021 में 11 नये ‘अभयारण्य’ बनाने की दिशा में काम हो रहा है। 10 ‘राष्ट्रीय-पार्क’ में से 6 को ‘टाईगर रिजर्व’ घोषित कर ‘कोर’ एवं ‘बफर’ जोन के नाम पर सैकङों आदिवासी गांवों को हटाया जा रहा है। ‘रातापानी (रायसेन एवं सीहोर जिले में फैले) अभयारण्य’ को ‘टाईगर रिजर्व’ बनाने के नाम पर 32 गांवों के हजारों परिवारों को हटाए जाने की कार्यवाही प्रगति पर है।
मध्यप्रदेश सरकार के ‘प्रधान मुख्य वन संरक्षक’ कार्यालय ने 20 अक्तूबर 2020 को 37 लाख हेक्टेयर बिगङे-वनों को ‘पब्लिक-प्राइवेट-पार्टनरशिप’ (पीपीपी) मोड पर निजी कम्पनियों को देने का आदेश जारी किया था, परन्तु विरोध के बाद इसे रोका गया। इसी ‘संरक्षित वन’ में से लोगों को ‘वनाधिकार कानून – 2006’ के अन्तर्गत ‘सामुदायिक वन निस्तार हक्क’ या ‘सामुदायिक वन संसाधनों’ पर समुदाय का अधिकार दिया गया है या दिया जाने वाला है। अगर ये 37 लाख हेक्टेयर वनभूमि उद्योगपतियों के पास होगी, तो फिर लोगों के पास कौन सा जंगल होगा? ‘इंडिया स्पेंड’ की 2019 की रिपोर्ट के अनुसार देश के 10 लाख आदिवासियों से जमीन छीनकर कारोबारियों को दे दी गई है।
प्रकृति को सुधारने के नाम पर मुनाफा कमाते हुए पूंजी बढाने की तरकीब है – ‘कार्बन व्यापार’ या ‘कार्बन ट्रेडिंग।’ वर्ष 2021 में ‘वैश्विक कार्बन क्रेडिट बाजार’ में 164 प्रतिशत की वृद्धि हुई है और वर्ष 2030 तक इसके 100 बिलियन अमेरिकी डालर पार करने की उम्मीद है। ‘कार्बन व्यापार’ के जरिए (वनीकरण करके) अन्तराष्ट्रीय बाजार से करोङों रुपए कमाना प्राथमिकता में है। भारत सरकार ने 2008 से 12 के बीच बिगङे-वन, गांव का चारागाह एवं पङत-जमीन पर वनीकरण कर ‘कार्बन क्रेडिट’ के जरिए 1250 लाख डॉलर कमाने की योजना बनाई थी। विश्वबैंक के आंकलन के अनुसार लकङी, बांस एवं अकाष्ठीय वनोत्पाद का मूल्य 20,000 लाख डॉलर है। ‘संयुक्त वन प्रबंधन’ इलाके के पारिस्थितिकीय एवं पर्यावरणीय टूरिज्म का मूल्य 17,000 लाख डॉलर आंका जा रहा है।
‘ग्रीन इंडिया मिशन’ और ‘रिडयूसिंग एमिशन फ्रॉम डिफारेस्ट्रेशन एण्ड डिग्रेडेशन’ (आरईडीडी), जिसे संक्षिप्त में ‘रेड’ कहा जाता है, के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा अन्तराष्ट्रीय पूंजी लाने की योजना है। पर्यावरण बचाने के नाम पर विश्व बाजार तैयार करना भी अन्तरराष्ट्रीय पूंजी का हिस्सा हो गया है। अब तो ‘एनजीओ’ भी आदिवासियों को उनके कब्जे की भूमि से बेदखल कर वृक्षारोपण करने का कार्यक्रम चला रहे हैं। ऐसा ही एक मामला मध्यप्रदेश के उमरिया जिले के मानपुर और ताला विकास खंड में आया है, जहां एक संस्था द्वारा आदिवासियों को उनकी ‘वनाधिकार कानून’ के दावे वाली वनभूमि से हटाकर वृक्षारोपण करने की शिकायत मिली है।
पर्यावरण बचाने के नाम पर धन भी बहुत है, लेकिन पूंजीवादी सोच के कारण सब कुछ व्यापारिक दृष्टिकोण से किया जा रहा है। इससे न तो जंगल और न ही पर्यावरण बच पा रहा है। आदिवासियों के बारे में कहा जाता है कि वे आज के लिए कमाते हैं और भविष्य की नहीं सोचते। उनका विश्वास है कि जल, जंगल, जमीन आधारित प्राकृतिक व्यवस्था उनकी जरूरत पूरी कर देगी। जो संसाधन जीवन देता है उसको आराध्य मानना उनकी संस्कृति का हिस्सा है। आदिवासियों के लिए जंगल मंदिर होता है और पेङ उनके देवता। जिन संसाधनों और मूल्यों को उन्होंने जीवन-शैली का आधार माना, उसे उनके पिछङे होने का सूचक मान लिया गया है।
साभार : सप्रेस