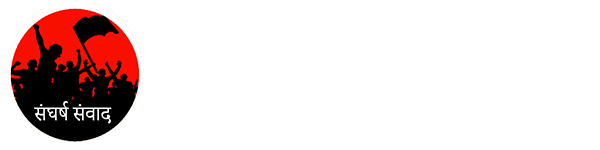ख़ूनी चेहरे के रंग-रोगन की क़वायद
गृह मंत्रालय ने सुरक्षा बलों को निर्देश दिया है कि अगर माओवादी किसी मुठभेड़ में महिलाओं और बच्चों को ढाल बनाते हैं तो वे उनसे भिड़ते समय पूरी एहतियात बरतें, और अगर बेगुनाहों की जान को ख़तरा दिखे तो उनसे मुठभेड़ करने से बचें। यह निर्देश पिछली 29 जून को बीजापुर जिले में ‘माओवादियों से हुई मुठभेड़’ के एक पखवारा बाद जारी हुआ जिसमें 17 लोगों की जानें गयी और जिसे स्वतंत्र जांच दलों के अलावा घटना स्थल तक पहुंचे मीडिया के एक हिस्से ने भी फ़र्ज़ी मुठभेड़ का नाम दिया था। सच को बाहर आने में देर नहीं लगी और सरकार कटघरे में खड़ी हो गयी। यह निर्देश इसी रोशनी में है।
यह निर्देश एक तीर से कई निशाने साधने की ग़रज़ से है। यह 28 जून को हुई ख़ूंरेज़ी में वर्दी पर पड़ रहे छींटों को हल्का करने और लगे हाथ अपने पिछले पापों को भी धोने की जुगत है। यह माओवादियों की उस छवि पर हमला करने का नया हथियार है जिसमें वे आदिवासियों के हमदर्द और उनके हित-अधिकारों के लिए लड़नेवाले योद्धा नज़र आते हैं। माओवादियों का चेहरा बदरंग दिखेगा तो ज़ाहिर है कि सरकार और सुरक्षा बलों का पलड़ा भारी होगा। यह क़वायद कुछ इस तरह से है कि देखिये साहब, माओवादी इतने कायर होते हैं कि जिन आदिवासियों के पक्ष में खड़े होने का दावा करते हैं, सुरक्षा बलों के हमले से बचने के लिए उन्हीं को अपनी ढाल बना लेते हैं।
कि उनमें इतना दम नहीं कि सुरक्षा बलों से सामना कर सकें। कि इससे पता चलता है कि माओवादी कितने ख़ुदग़र्ज़ हैं और आदिवासियों के कट्टर दुश्मन हैं। कि बिचारे भोले-भाले आदिवासी तो उनकी चाल में फंस-पिस रहे हैं। कि सरकार उन्हें आदिवासियों के चंगुल से छुड़ाने और उन्हें विकास की मुख्यधारा से जोड़ने की हर मुमकिन कोशिशों में लगी हुई है। कि इसके लिए सुरक्षा बलों को मुश्किल हालात में काम करना पड़ता है, अपनी जान जोखिम में डाल कर भारी चुनौतियों से जूझना पड़ता है। कि देश के लोगों को इसे समझना चाहिए और सुरक्षा बलों का मनोबल नहीं गिरने देना चाहिए। कि माओवादियों के सफ़ाये में सरकार के साथ खड़े होना चाहिए।
28 जून की रात छत्तीसगढ के तीन सुदूर गांवों में वर्दी पहन के आयी दरिंदगी ने ख़ौफ़ और दहशत का कभी न भुलाया जा सकनेवाला मंज़र पेश किया। 29 जून की सुबह तक चले इस ख़ूनी सिलसिले के तुरंत बाद पी. चिदंबरम ने नयी दिल्ली में पत्रकारों को यह पक्की ख़बर दी कि बीजापुर जिले में सीआरपीफ़ के साथ हुई मुठभेड़ में 17 दुर्दांत माओवादी ढेर कर दिये गये। उन्होंने इसे माओवादियों के ख़िलाफ़ जारी सरकारी मुहिम की बड़ी उपलब्धि करार दिया और इसके लिए सीआरपीएफ़ के साहस और कौशल की तारीफ़ की। लेकिन अगले अगले दिन ही उन्हें फ़र्ज़ी मुठभेड़ की खुलती परतों के बीच अपने बयान को थोड़ा बदलना पड़ा कि अगर सचमुच कोई ऐसा बेगुनाह मारा गया है जिसका माओवादियों से किसी तरह का रिश्ता नहीं था तो इसका हमें अफ़सोस है।
बच्चों और महिलाओं की लाशों की तसवीरें ही सबसे बड़ी गवाही है कि चिदंबरम की ख़बर कितनी कच्ची और सरासर झूठ थी। तो भी उन्होंने ढिठाई से कहा कि यह सच्चाई तो जांच के बाद ही सामने आ सकेगी कि क्या कोई बेगुनाह भी मारा गया। यह कहां का क़ायदा है कि रायपुर से मिली सूचना को बिना तौले-परखे पक्की ख़बर बता कर प्रसारित कर दिया जाये और जब उस पर सवाल खड़े हों तो उसे जांच के नाम पर टाल दिया जाये। यह जम्हूरी निजाम के हिटलरी हुक़्मरानों का अंदाज़ है।
सीआरपीएफ़ केंद्रीय गृह मंत्रालय के अधीन काम करती है और चिंबरम साहब इस मंत्रालय के मुखिया हैं। इस हैसियत से उन्होंने देश के सामने 28 जून को सीआरपीएफ़ के हाथ लगी बड़ी कामयाबी को उजागर किया था। भले ही चिदंबरम साहब फ़िलहाल इसे न मानें लेकिन अब जबकि इस कामयाबी की असलियत पर ही शुबहा है और जिसमें सीआरपीएफ़ का दहशतग़र्द और बर्बर चेहरा दिखता है तो गृह मंत्री को मामले की जांच किये जाने का एलान करना चाहिए था। लेकिन जांच दल के गठन के बावत उन्होंने यह कहते हुए अपनी ज़िम्मेदारी से पल्ला झाड़ लिया कि यह काम छत्तीसगढ सरकार का है, वह इसकी ज़रूरत समझेगी तो जांच दल का गठन करेगी।
अब जांच दल के गठन को किक मारने की बारी रमन सरकार की थी। दिल दहला देनेवाली इतनी बड़ी वारदात की जांच का काम भोपालपटनम तहसील के सब दिवीज़ल मजिस्ट्रेट आरए कुरूवंशी को सौंप दी गयी और मजिस्ट्रेट साहब ने साफ़ कर दिया कि उनका घटनास्थल का दौरा करने का इरादा नहीं है- कि जिनको अपना बयान दर्ज़ कराना हो, 9 जुलाई को उनके दफ्तर पहुंचे। यह कैसी जम्हूरियत है कि जहां ज़ुल्म के मारे, दुख और सदमे में सरापा भीगे-ठिठुर रहे लोगों से कहा जाता हो कि अपनी फ़रियाद लेकर फ़लां दिन दरबार में हाज़िर हों। उनकी शिक़ायतें सुनने के लिए साहब हुज़ूर इतनी दूर जाने की ज़हमत क्यों उठायें?
लेकिन उन्हीं साहब हुज़ूर को गांव का दौरा लगाना पड़ा- जांच के लिए नहीं, गांववालों के बीच दैनिक ज़रूरतों का सामान बांटने के लिए। देश-दुनिया में हो रही थूथू को देखते हुए राज्य सरकार को अपनी रहमदिली दिखाने की सुध आयी। ऊपर से आदेश मिला तो साहब हुज़ूर सामानों से भरा ट्रक लेकर कोत्तागुड़ा पहुंचे। लेकिन गांववालों ने यह कहते हुए सरकारी राहत को ठुकरा दिया कि ‘तुमने हमारे लोगों को मारा, बच्चों तक को नहीं छोड़ा और उन्हें माओवादी बताया तो माओवादियों की मदद क्यों? यह ग़ुस्सा ही उनका सबसे ठोस बयान है कि उनकी आत्मा पर इतना गहरा ज़ख़्म हुआ कि कोई मलहम उसे सुखा नहीं सकता, कि उन्हें सरकार से कोई उम्मीद भी नहीं है, कि सरकार ही उनके साथ हुए ज़ुल्म की गुनाहगार है। आदिवासी अनपढ़ हो सकते हैं लेकिन सदियों से ख़ुद्दारी का पाठ पढ़ते रहे हैं। वे सहज-सरल होते हैं लेकिन दोस्त और दुश्मन के बीच फ़र्क़ करना ख़ूब जानते हैं। सरकारें इसे क्या जानें?
मसले के तूल पकड़ने पर सीआरपीएफ़ के डीजी के. विजय कुमार ने कहा था कि सीआरपीएफ़ कोई अनुशासनहीन और ग़ैर ज़िम्मेदार इकाई नहीं है। लेकिन इस सवाल से घिरने पर कि उसमें तो बेगुनाह लोग मारे गये, उनका बेशर्म जवाब था कि ‘माओवादी अगर महिलाओं और बच्चों को अपनी ढाल बनाते हैं तो हम क्या कर सकते हैं? गोलियां अंधी होती हैं, लिंग और उम्र में फ़र्क़ करना नहीं जानतीं। वैसे भी 29 जून की रात बहुत अंधेरी थी।’ पहली बात तो यह कि वह चांदनी रात थी और अगर अंधेरी भी थी तो बाहर से ख़रीदी गयीं उन मंहगी और क़ीमती दूरबीनें क्या कर रही थीं जो घुप्प अंधेरे में भी बहुत साफ़ देख लेती हैं? बेशक़, गोलियां अंधी होती हैं अगर आंख मूंद कर दागी जायें। अव्वल तो गोलियां ख़ुद नहीं दगतीं, उन्हें दागा जाता है। यह काम बंदूकधारियों के हाथ करते हैं, और हाथ दिमाग़ और आंख के तालमेल से काम करते हैं। यह फ़ौज़ी अनुशासन है कि दिमाग का इस्तेमाल उतना ही किया जाये जितना हुक़्म बजाने के लिए ज़रूरी हो और आंखें भी उतना ही देखें जो इसे मुकम्मल बनाने के लिए ज़रूरी हो। यहां दिल का कहा मानने की मनाही है।
पुलिस हो या कि सीआरपीएफ़, वह तो सरकार की लाठी है। इस बेरहम लाठी को क्यों कोसें? उसे तो बनाया ही इसलिए गया है कि जब और जहां ज़रूरत पड़े, भांजा जा सके। लाठी सोचने-विचारने का काम नहीं करती। यह काम उसे थामनेवाले का होता है। नहीं भूला जाना चाहिए कि पुलिस का गठन गोरी हुक़ूमत ने किया था और इसका मक़सद लोगों के जान-माल की हिफ़ाज़त करना नहीं था। 1857 की सशस्त्र क्रांति के बाद बने जांच आयोग की सिफ़ारिशों के आधार पर उसे खड़ा किया गया था ताकि ऐसे किसी अगले जन उभार को समय रहते कुचला जा सके।
ख़बर है कि जिस रात सीआरपीएफ़ के जवानों ने आदिवासियों पर हमला कर अपनी ‘वफ़ादार मर्दानिगी’ का सबूत किया, उसी दिन बीजापुर के तमाम पत्रकारों को सरकारी ख़र्च पर वातानुकूलित लग्ज़री बस से सैर-सपाटे के लिए हैदराबाद रवाना कर दिया गया था। यह योजना दुर्ग में तैनात एसटीएफ़ के राजेंद्र नारायण दास ने तैयार की थी जो बीजापुर का एसपी रह चुका है। पत्रकारों पर हुई इस सरकारी इनायत को आदिवासियों पर बरपा की गयी हैवानियत की पटकथा से जोड़ कर क्यों न देखा जाये? पहरेदारों की ग़ैर हाज़िरी में चोर, उचक्के, लुटेरे और हत्यारे की पौ बारह होती है। इसके लिए पहरेदारों को तैयार भी किया जा सकता है, बहला-फुसला कर या डरा-धमका कर। इसे महज़ संयोग नहीं माना जा सकता कि idhaइधर पत्रकारों ने जिले से कूच किया और उधर वहशियत का ख़ूनी खेल हुआ।
इससे समझा जा सकता है कि स्थानीय मीडिया में राज्य दमन से जुड़ी ख़बरों को जगह क्यों नहीं मिल पाती या कि मिलती भी है तो सरकारी ज़ुबान में ही क्यों? यह सरकार और प्रशासन के मीडिया मैनेजमेंट का करिश्मा है। ख़रीदा उसे जाता है जो बिकाऊ होता है। यहां तो बीजापुर ही नहीं, पूरे छत्तीसगढ़ में उनकी लंबी सूची है। लेकिन अपवाद कहां नहीं होते? यहां भी हैं। कोत्तागुड़ा गांव में हुए नर संहार की घटना उन्हीं चंद पत्रकारों की निडर फुर्ती से बाहर आ सकी जो सरकारी दान-कृपा से दूरी रखते हैं और पत्रकारिता के उसूलों से समझौता नहीं करते। वाचडाग की भूमिका से कट कर किसी का लैपडाग हो जाना गवारा नहीं करते।
पत्रकार की ज़िम्मेदारी है कि वह लोगों तक सच पहुंचाये। सच की तह तक जाने के लिए मेहनत करनी पड़ती है, निगाहें खुली रखनी होती हैं, लोभ और भय से बचना होता है और सच को जस का तस पेश करने के लिए जिगरा रखना होता है। इधर इस जज़्बे और हौसले में तेज़ी से गिरावट आयी है। पत्रकारिता की दुनिया में ऐसे लोगों की फ़ौज़ और उनकी पूछ बढ़ती जा रही है, जो भले ही पत्रकारिता की बाक़ायदा पढ़ाई कर चुके हैं लेकिन दिल-दिमाग़ से अंगूठा टेक हैं। उनकी आंखें वही देखती हैं जिसे वे देखना चाहते हैं, उनके कान वही सुनते हैं जिसे वे सुनना चाहते हैं। गोया कि मीडिया में बुद्धि विरोधी मोरचा खुल गया हो जिसकी कमान संपादक जी के हाथ में हो।
लेकिन यह अधूरा सच है। पूरा सच तो यह है कि मीडिया में आज़ादी की लक्ष्मण रेखाएं पहले से खिंची होती हैं जिसे लांघना मुश्किल से हासिल की गयी नौकरी से हाथ धो बैठने का ख़तरा उठाना होता है। पत्रकारों की आज़ादी का दायरा मीडिया को चला रहे कारपोरेट समूहों के व्यापारिक हितों से तय होता है, सामाजिक हितों से नहीं। अगर किसी मीडिया समूह का उत्पाद केवल मुनाफ़ा कमाने के लिए है, अपने उपभोक्ताओं को सही सूचना देने के लिए नहीं तो किस बात की ईमानदारी, कौन सी प्रतिबद्धता, कहां की सवेदनशीलता और कैसे मूल्य? सच की ज़ुबान पर बंदिश इस तरह लगती है और जनता को सजग बनाने की ज़िम्मेदारी दूर की कौड़ी हो जाती है।
मीडिया अक़्सर अभिव्यक्ति की आज़ादी का सवाल उठाता है। अब यह सवाल कौन करे और कैसे कि साहब जी, आख़िर किसकी आज़ादी और कैसी आज़ादी? आख़िर मीडिया की आज़ादी का मतलब क्या? क्या सच को ढांक-झुठला कर झूठ परोसने की आज़ादी? क्या मुनाफ़े के लुटेरों का चेहरा चमकाने की आज़ादी? सरकार बहादुरों के धतकरमों पर परदा डालने की आज़ादी? नक़ली मुद्दों पर आग लगाने और असली मुद्दों को पीछे ढकेल देने की आज़ादी? भूख और ज़ुल्म की मारी जनता की आहों से मुंह फेरने की आज़ादी? और इसके बदले ऐश और बेफ़िक़ी हासिल करने की आज़ादी?
यह पाठकों, श्रोताओं और दर्शकों उर्फ़ मीडिया के उपभोक्ताओं का अधिकार है कि उन्हें किसी घटना, सवाल या मुद्दे को हर कोण से जांचने-परखने और उसके मुताबिक अपनी राय बनाने की सहूलियत मिले। यह तभी मुमकिन है जब उन्हें हर उस घटना, फ़ैसले या प्रक्रियाओं की सही और पूरी जानकारी मिले जो उनके जीवन और समाज पर असर डालनेवाला हो या डाल सकता हो। किसी पक्ष को दबाने, तोड़ने-मरोड़ने या अधूरा रखने से यह मुमकिन नहीं। वैसे, ग़लत जानकारी से भली ग़ैर जानकारी होती है जो कम से कम सनसनी और अफ़वाह को तो पैदा नहीं करती। अधकचरी जानकारी के आधार पर बना जनमत कभी सही नहीं हो सकता। माओवादियों और सरकार के बीच जारी भिड़ंत के मामले में भी यही बात लागू होती है। माओवादियों के नियंत्रण से बाहर के इलाक़ों में यह तसवीर बनाने की कोशिश है जिसमें माओवादी देश और समाज के लिए नासूर हैं, आतंकवाद का दूसरा चेहरा हैं। यह तसवीर गढ़ने में मीडिया का बड़ा हिस्सा सरकार का भरोसेमंद साथी दिखता है।
अकबर इलाहाबादी का यह शेर बहुत मशहूर है कि ‘खींचो न कमानों को न तलवार निकालो/जब तोप मुकाबिल हो तो अख़बार निकालो.’ यानी ताक़त के मामले में अख़बार किसी तोप से कमतर नहीं होते। आज़ादी से पहले तमाम अख़बारों ने इसे साबित कर दिखाया और देश की जनता के साथ मिल कर गोरी हुक़ूमत को देश से खदेड़ देने में उल्लेखनीय भूमिका अदा की। ज़ाहिर है कि इसकी उन्होंने भारी कीमत भी चुकायी। कुर्की, जेल, ज़ुर्माना, शहर निकाला. ना जाने क्या-क्या झेला लेकिन अपने क़दम पीछे नहीं किये।
तब अख़बार कम थे और आज अख़बारों की भरमार है। पहले अख़बार निकालने का मक़सद जनता की आवाज़ बनना था। आज ज़्यादातर अख़बारों का मक़सद दौलत कमाना है। ख़बरिया चैनलों का हाल तो और बुरा है। कुल मिला कर कहें तो पत्रकारिता में जन सरोकारों की जगह तेज़ी से घटती जा रही है। लगता है जैसे मीडिया के बड़े हिस्से में तोप से भिड़ने के बजाय उसका भोंपू बनने की होड़ मच गयी हो।
इस भगदड़ में सच कराह रहा है, सिसकियां भर रहा है। गांव के 15-16 साल के दो बच्चों ने इसी साल जनवरी में विशाखापत्तनम की यात्रा की थी। यह मौक़ा उनकी क़ाबलियत का ईनाम था जिसका ख़याल शायद उन्होंने सपने में भी नहीं बांधा होगा कि कभी वह इतने लंबे सफ़र पर निकलेंगे और समुंदर देखेंगे- किसी अजूबे की तरह। यह उनका अपनी सिमटी हुई दुनिया से बाहर निकलना था, समझना था कि दुनिया कित्ती बड़ी और दिलकश है और ज़िंदगी कितनी क़ीमती होती है। इस सुनहरे और यादगार सफ़र में न जाने कितनी मासूम ख़्वाहिशें पैदा हुई होंगी, भविष्य के ख़ूबसूरत सपने सजे होंगे। भले ही दोनों सफ़र पूरा कर अपनी दुनिया में लौट गये लेकिन नन्हीं उम्मीदें तो ऐसी मीठी यादों में जागती रहती हैं, अरसे तक ताज़ादम रहती हैं। आख़िर 15-16 साल की कच्ची उम्र ख़ुद ही रूमानियत से भरी होती है। सपनों को अभी परवान चढ़ना था कि 29 जून की रात सीआरपीएफ़ की गोलियों ने सपना बुननेवाली आंखों को हमेशा की नींद में भेज दिया। दोनों किशोर हाई स्कूल के छात्र थे और बसगुड़ा में रह कर पढ़ाई कर रहे थे। गरमियों की छुट्टी में घर आये हुए थे और स्कूल वापसी की तैयारी में थे लेकिन माओवादियों के सफ़ाये पर निकली सीआरपीएफ़ की टुकड़ी तो उनकी मौत का फ़रमान बन कर आयी थी। गोलियों की बौछार से उनके शरीर छलनी हुए और उसी दम उनके बेगुनाह सपनों का भी क़्त्ल हो गया। उसका मुवावज़ा कौन भर सकेगा।
छत्तीसगढ़ छोड़ने के लिए मजबूर किये गये हिमांशु कुमार के मुताबिक़ बैलाडीला में कई कंपनियों को लोहे की खदानों की लीज़ दी गयी है जिसमें टाटा और एस्सार जैसी कंपनियां भी शामिल हैं जो एक से बढ़ कर एक अपनी घाघ तिकड़मों के लिए जानी जाती हैं और इसलिए बच निकलती हैं कि उनकी ऊंची सियासी पहुंच है या कहें कि सियासत ही उनकी जेब में रहती है। ख़ैर, लोहे को बाहर ले जाने के लिए सेना बीजापुर से जगदलपुर तक सड़क बना चुकी है। अब बैलेडीला से बीजापुर तक सड़क बनाना बाक़ी है। सारकेगुड़ा गांव जिसने कोत्तागुड़ा और राजपेटा गांव के संग 29 जून का कहर झेला, इसी रास्ते पर पड़ता है और अधूरी सड़क को पूरा किये जाने में रोड़ा है। क्या वह ख़ूनी रात इस रोड़े को हटाने के लिए थी? कोत्तागुड़ा की पूरी कहानी सामने आनी ही चाहिए और इसमें इस सवाल का जवाब भी होना चाहिए।
सुकमा के कलेक्टर को माओवादियों के क़ब्ज़े से रिहा कराने में अपनी कामयाब भूमिका अदा करने के बाद गांधीवादी बीडी शर्मा ने कहा था कि देश में माओवाद की समस्या न तो कलेक्टर के अपहरण से शुरू हुई थी और ना ही कलेक्टर की रिहाई से ख़तम हो गयी है। उन्होंने यह टिप्पणी रिहाई के लिए हुए समझौते के मुताबिक़ राज्य सरकार के काम न करने से दुखी होकर की थी। यह राज्य सरकार को ताक़ीद थी कि वह समझदारी दिखाये वरना मसला अभी और उलझेगा। लेकिन इस नसीहत को हवा में उड़ा दिया गया और माओवादी होने के ज़ुर्म में बेगुनाहों पर, हक़ और इनसाफ़ के पैरोकारों पर निशाना साधने का सिलसिला जारी रहा। 29 जून की घटना उसका अब तक का सबसे ज़ालिम पड़ाव था।
माओवादियों का सफ़ाया करने की नयी दिल्ली और रायपुर की ज़िद और ज़बरदस्ती के अभी थमने के आसार नहीं दिखते। ऐसे में माओवादी समस्या के सुलटने के सुराग़ भी नहीं मिलते। मिल भी नहीं सकते। आदिवासियों के साथ जब तक दुश्मनों जैसा सुलूक़ जारी रहेगा, माओवादियों की बढ़त होती रहेगी, उनका दायरा फैलता रहेगा। विकास के नारों, कल्याणकारी कार्यक्रमों और माओवाद विरोधी डुगडुगी से उसे रोका नहीं जा सकता। फ़िलहाल, सरकारी ज़िद और ज़बरदस्ती के आलम को देख कर तो यही लगता है कि अंधेरी रात अभी बहुत लंबी है।