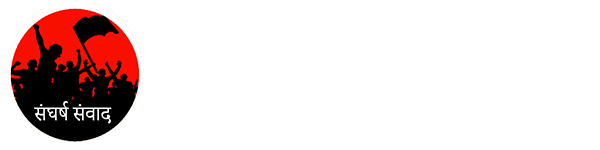आपातकाल : भारत की आत्मा पर स्थायी दाग
भारत में आंतरिक आपातकाल की घोषणा को 26 जून को 40 वर्ष हो जाएंगे। चार दशक पश्चात भी भारत की आत्मा से वह दाग धुल नहीं पाया है। वर्तमान पीढ़ी की इस संघर्ष को लेकर बनी अनभिज्ञता वास्तव में चाैंकाने वाली है। भारत के अनेक राज्यों और केंद्र सरकार के ढ़ेर सारे निर्णय व्यक्ति व समुदाय की स्वतंत्रता को बाधित करने हेतु प्रयासरत है। आपातकाल पर पुर्नविचार हमें लोकतंत्र की अनिवार्यता के मायने समझाने में सहायक होगा। पेश है न्यायमूर्ति (से. नि.) राजिंदर सच्चर का सप्रेस से साभार यह आलेख;
ऐ से राष्ट्र जो अपना सद्य अतीत याद नहीं रखते वहां उसी त्रासदी की पुनरावर्ती का खतरा पैदा हो जाता है। यह ख्याल मुझे तब आया जब मैनें लोगों से अचानक 26 जून 1975 (आपातकाल दिवस) के महत्व के बारे में प्रश्न किया। 35 वर्ष और उससे कम उम्र के लोग जो कि भारत की जनसंख्या का 2/3 हिस्सा हैं, में से अधिकांश को इसके बारे में कुछ पता नहीं था। इतना ही नहीं 55 वर्ष तक के लोगों के जवाब भी उत्साहवर्धक नहीं थे।
समाचारपत्र भी कभी इसे मुखपृष्ठ पर स्थान नहीं देते, कुछ तो इस संबंध में कोई जानकारी तक नहीं देते और कुछ ऐसे ही कामचलाऊ तरह से अंदरूनी पन्नों पर कहीं कोने-कचरे में इसकी जानकारी दे देते हैं। अनेक विपक्षी दल जो कि आपातकाल का शिकार हुए थे, भी इसे ज्यादा तवज्जो नहीं देना चाहते। हालांकि पी.यू.सी.एल. एवं अन्य नागरिक स्वतंत्रता संगठन हमेशा ही इस दिन विरोध प्रदर्शन व बैठकें करते हैं। परंतु टीवी व समाचारपत्र सोची समझी नीति के तहत इसका उल्लेख करने से बचते है। वैसे भी उनमें से अधिकांश सरकार की नवउदारवादी नीतियों के साथ हैं या उनमें डर की कोई भावना है क्योंकि आपातकाल थोपने वाला सत्ताधारी दल अभी कुछ ही समय पूर्व तक सŸाासीन था। यह त्रासदायी है कि इसी दिन भारत ने अपना लोकतंत्र खो दिया था। उसी दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति ने व्यंग्यपूर्व तरीके से दंभ भरा था कि अब अमेरिका दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। यह दूसरी बात है जयप्रकाश नारायण (जे. पी.) के नेतृत्व में भारतीयों द्वारा किए गए त्याग व बलिदान से अमेरिका के राष्ट्रपति का दंभ केवल 18 महीनों में टूट गया।
ऐसा नहीं है आपातकाल का कोई प्रतिरोध नहीं हुआ। हजारों लोग जेल गए। जिनमें पूर्व केंद्रीय मंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री, राज्यपाल, अधिवक्ता, विधायक और कुछ साहसी पत्रकार भी शामिल थे। अनेक मानवाधिकार कार्यकर्ता भी भूमिगत हो गए थे। लेकिन अहिंसक लोग एक हद तक ही असंयमी और कमोवेश एक फासिस्ट राज्य, जैसा कि भारत उन दिनों बन चुका था का सामना कर सकते थे। न्यायपालिका से उम्मीद की जाती है कि आपातकाल जैसे संकट के समय वह प्रशासन द्वारा किए जा रहे अत्याचारों या अतियों के खिलाफ नागरिकों का बचाव करेगी। जबलपुर के अतिरिक्त दंडाधिकारी (ए.डी.एम.) द्वारा दिया गया निर्णय कि आपातकाल के दौरान जीवन का अधिकार अर्थहीन हो जाता है, से सहमति जताकर भारतीय सर्वोच्च न्यायालय ने स्वतंत्रता पर शर्मनाक प्रहार किया था। सर्वोच्च न्यायालय की यह भीरुता अथवा कातरता भविष्य में भी मानवधिकारों की सुरक्षा को लेकर बनी रही थी।
सर्वोच्च न्यायालय ने ए.डी.एम. जबलपुर 1976 के मामले में विभिन्न राज्यों के 9 उच्च न्यायालयों के निर्णयों की वैधता जिसमें कि यह आदेश दिये गए थे कि सरकारों द्वारा गिरफ्तारी हेतु दिए गए आदेश गैरकानूनी हैं तथा कुछ मामलों में तो निरुद्ध किए गए व्यक्तियों को छोड़ने तक के आदेश दे दिए थे, को रद्द (ओवररुल) कर दिया। यदि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा उच्च न्यायालयों के विचार को मान लिया गया होता तो आपातकाल उसी समय धराशायी हो जाता। लेकिन हमें शर्मसार करते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने 4 न्यायाधीशों बनाम 1 न्यायाधीश (अपवादस्वरूप न्यायमूर्ति खन्ना) के यह स्थापित किया, ‘‘27 जून 1975 के राष्ट्रपति के आदेश के परिप्रेक्ष्य में कोई भी व्यक्ति अनुच्छेद 226 के अन्तर्गत उच्चन्यायालय के समक्ष बंदी प्रत्यक्षीकरण (हेबसकार्पस) और कोई अन्य याचिका (रिट पिटीशन) आदेश या निर्देश नहीं दे सकेगा जिनके अन्तर्गत निरुद्ध करने के आदेश की वैधानिकता को चुनौती दी गई हो।‘‘(सारांश)
अपने को शर्मिंदा करते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने महाधिवक्ता की यह दलील स्वीकार कर ली कि यदि एक पुलिसकर्मी अपने वरिष्ठ अधिकारी के आदेश के तहत किसी व्यक्ति को गोली मार देता है या सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश तक को गिरफ्तार कर लेता है तो इसको बचने के लिए कोई भी वैधानिक राहत उपलब्ध नहीं है। स्वाभाविक है ऐसी परिस्थिति में आपातकाल के विरुद्ध कोई भी शांतिपूर्ण आंदोलन चल ही नहीं सकता था। मुझे यह देखकर धक्का लगा कि बहुमत वाला निर्णय किस तरह युद्ध के दौरान सन् 1942 में ब्रिटेन के हाउस आफ लार्डस द्वारा लिवरसीज विरुद्ध एंडरसन वाले मामले जिसमें लार्ड एटकिन ने स्मरणीय असहमति जताई थी, पर आधारित हो सकता है। गौरतलब है बाद में ब्रिटिश न्यायालय अपने इस निर्णय से इस कदर शर्मिंदा हुए थे कि उन्होंने बहुत सजगता से इस निर्णय को कूड़े के ढेर में फेक दिया था।
कुछ टिप्पणीकारों ने लिवरसीज के बहुमत से निर्णय मामले में न्यायालय के योगदान को विश्वयुद्ध के लंबे होने का कारण बताया था। ठीक इसी तरह हमारे देश में जबलपुर मामले में सर्वोच्च न्यायालय के फैसलों को सन् 1975 में आपातकाल की निरंतरता का कारण माना जाता है। यदि सर्वोच्च न्यायालय 9 उच्चन्यायालयों जैसा ही रुख दिखाता तो आपातकाल तुरंत भरभरा कर ढह जाता क्योंकि संभवतः कोई भी न्यायालय जयप्रकाश नारायण, मोरारजी देसाई, रामनारायण, जार्ज फर्नाडिस, मधु लिमये जैसी महान हस्तियों और देशभक्तों तथा कुलदीप नैय्यर जैसे साहसी पत्रकार एवं हजारों भारतवासियों जिन्हें देश की सुरक्षा के लिए खतरा बताया जा रहा था को जेल में बंद नहीं रख सकता था। इसका अपरिहार्य परिणाम यही होता कि इन नेताओं की तुरंत रिहाई से विपक्षी आंदोलन को जबरदस्त मदद मिलती और सन् 1976 के मध्य तक इंदिरा गांधी की सरकार का सूपड़ा साफ हो जाता। लेकिन कई बार राष्ट्रों की नियति कुछ व्यक्तियों की भीरूता से प्रभावित हो जाती है। इस मामले में यह देश की सर्वोच्च न्यायापालिका से प्रकट हुई, जिसे किसी भी परिस्थिति में झुकना नहीं था।
सन् 1978 में सरकार परिवर्तन के तुरंत बाद न्यायमूर्ति चन्द्रचूड़ और न्यायमूर्ति भगवती ने सार्वजनिक रूप से दुख प्रकट किया और स्वीकार किया कि उनके निर्णय गलत थे और अगर वे न्यायमूर्ति खन्ना के साथ होते तो वह निर्णय बहुमत का निर्णय हो जाता। लेकिन सब कुछ समाप्त हो जाने के बाद ऐसा रोना रोना भी अर्थहीन हो जाता है। इस निर्णय की वजह से न्यायपालिका के प्रति ऐसा संदेह या अविश्वास पैदा हुआ जिससे कि संसद को ऐहतियातन सन् 1978 में संविधान में 44वां संशोधन करना पड़ा। जिसके अन्तर्गत राष्ट्रपति से अनुच्छेद 21 को निलंबित करने के अधिकार ले लिए गए। इसके बावजूद हमें लगातार यह ध्यान में रखना होगा कि व्यक्तियों की स्वतंत्रता की सुरक्षा को बनाए रखने के लिए देश को सतत निगरानी रखनी ही होगा। साथ ही साथ प्रेस को भी आम जनता को इस बात की बार-बार याद दिलाते रहना चाहिए।