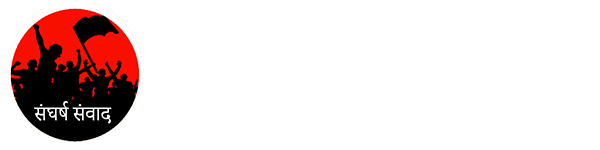बेघरी की बेबसी बनाम सरकारी बेदिली
गोया कि यह सालाना रिवाज़ बन गया है कि ठंड कहर बरपा करती है, शोर मचता है और तब कहीं जा कर बेघरों के लिए अस्थाई रैन बसेरों और अलाव का बंदोबस्त किये जाने का सरकारी आदेश जारी होता है। और जिस तरह उस पर अमल होता है, वह महज़ रस्म अदायगी होता है, लूट का एक और मौक़ा हो जाता है। ठंड की विदाई के साथ ही बेघरी का मसला भी ठंडा पड़ जाता है। हालांकि बेघरी कोई मौसमी मसला नहीं हुआ करती कि गरमी में पिघल जाये। उसकी आह भाप बन कर अगली सर्दी तक के लिए कहीं उड़ नहीं जाया करती। उसकी मार तो हर मौसम में सताती है। बेघरी अगर सर्दी में ठिठुरती है तो गर्मी में लू के थपेड़ों से गुज़रती है और बारिश में लगातार भीगती है। बेघरी माने हर दिन दुश्वारियों से मुठभेड़- जितना बड़ा शहर, उतनी ही संगीन।
तो फ़िलहाल, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ चलें और सरकारी बेदिली का दीदार करें। दिसंबर आते-आते सर्दी का मौसम उत्तर भारत के ग़रीबों और ख़ास कर बेघरों को डराने-धमकाने लगा था। लेकिन लखनऊ में अस्थाई रैन बसेरों और अलाव का इंतज़ाम किये जाने का सरकारी आदेश साल के आख़ीर में जारी हो सका। तब तक ठंड से होनेवाली मौतों का आंकड़ा सैकड़ा पार कर चुका था और रात का तापमान लुढ़क कर 2 डिग्री सेल्सियस के आसपास डोलने लगा था। यह बेघरों के लिए नये साल की ज़ालिमाना शुरूआत थी।
 |
| यह विधानसभा मार्ग है। |
लेकिन हुक़्मरान तो ख़ैर चैन की नींद सोते हैं। उत्तर प्रदेश विधानसभा की 125 जयंती के मौक़े पर राजधानी लखनऊ में गुज़री 6 जनवरी से तीन दिवसीय आयोजन की शानदार शुरूआत होगी। इसे यादगार बनाने की तैयारी न जाने कब से पूरी गर्माहट और मुस्तैदी के साथ चली, बिना किसी कमी-कोताही के। इसे कहते हैं ऊंचे महलों में जम्हूरी निजाम का जश्न और फ़ुटपाथ पर मातम। लखनऊ का हालचाल गवाही है कि सूबे के दूसरे बड़े शहरों में फ़ुटपाथ की ज़िदगी जी रहे लोगों को सर्दी का निवाला बनने से बचाने के लिए पहले अगर ‘बहुजन हिताय’ का नगाड़ा पीटनेवाली तो अब पिछले नौ महीने से उत्तर प्रदेश को ‘उत्तम प्रदेश’ बनाने का नारा उछालनेवाली राज्य सरकार कितना और किस तरह मुस्तैद रही। इस मायने में हाथी और साइकिल सवार इकजैसे निकले।