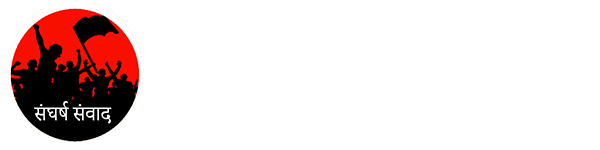मुसहर-दलित-वंचित सम्मेलन: नयी मुहिम की शुरूआत
बरही नवादा से लौट कर आदियोग की रिपोर्ट;
यह सम्मेलन वंचितों के सम्मान, पहचान और गरिमा के साथ उनके जीने के अधिकार पर फ़ोकस होगा। मुसहर अति दलित, अति वंचित समुदाय है। बेहद ग़रीब समुदायों में भी वे अति ग़रीब हैं। पुलिसिया और सामंती जुलुम की सबसे ज़्यादा और सबसे तीखी मार भी वही झेलते हैं। इसलिए सम्मेलन का पहला ज़ोर मुसहरों पर होगा।
इसी कड़ी में यह ज़िक़्र ग़ौर तलब है कि कोई 10 दिन पहले वाराणसी के चोलापुर ब्लाक के सैनाखुर्द गांव के एक मुसहर को पीट-पीट कर मार डाला गया। इलाक़े के दबंगों ने उसे बेरहमी से सरेआम पीटा और अधमरा कर दिया। उसी बुरी हालत में जानवर की तरह लाद कर उसे थाने ले जाया गया। कहा गया कि उसने चोरी की थी लेकिन पुलिस ने मौत के मुहाने पर खड़ी उसकी नाज़ुक हालत देखते हुए उसके ख़िलाफ़ कोई मामला दर्ज़ करने से इंकार कर दिया।
यह दबंगों के हित में पुलिस की भलमानसाहत थी। पुलिस को पिटाई किये जाने और इस तरह क़ानून को हाथ में लिये जाने का जुर्म नज़र नहीं आया, ग़ैर इरादतन ही सही लेकिन हत्या की कोशिश करने का मामला दर्ज़ किये जाने का फ़र्ज़ याद नहीं आया। तो पुलिस ने अपने हाथ खड़े कर दिये- कुछ यों कि यह साला मर रहा है, इसे थाने के सामने से फ़ौरन हटाओ, कहीं भी ले जाओ लेकिन हमको किसी पचड़े में मत फंसाओ। बहरहाल, पिछले 26 नवंबर तक (जिस दिन मैं आयोजन समिति की बैठक के सिलसिले में बरही नवादा में था) उस अभागे मुसहर का कहीं कोई पता नहीं था। तय है कि अब वह ज़िंदा नहीं है और उसका नामोनिशान मिटाया जा चुका है।
मामला दर्ज़ होता तो तफ़्तीश होती। असलियत सामने आती कि क्या वाक़ई उस मुसहर ने चोरी की थी और ऐसा क्या चुराया था कि जिसकी उसको इतनी तगड़ी सज़ा मिली? हो सकता है कि पता चलता कि उसकी चोरी उसके ज़िंदा रहने के लिए बहुत बड़ी मजबूरी रही हो। यह भी हो सकता है कि पता चलता कि मामला तो कुछ और था जिसे ढंकने के लिए चोरी की कहानी बना दी गयी। वैसे, किसी मुसहर पर चोरी का इल्ज़ाम लगना या लगा दिया जाना हमेशा से बहुत आसान काम रहा है। कई मुसहर ऐसे ही फ़र्ज़ी मामलों में जेलों में बंद हैं। उनकी पैरवी कौन करे? पुलिस ड्यूटी की पाबंद होती तो कथित चोर को पहले इलाज की सहूलियत मिलती और उसके ख़िलाफ़ मामला दर्ज़ कराने पहुंचे लोगों को सबसे पहले हवालात। लेकिन ऐसा कैसे होता, क्यों होता? यह तो होता ही रहता है। आख़िर पुलिस इंसानों के लिए होती है- मुसहरों के लिए नहीं।
कहा जा सकता है कि मुसहर टोले में सुअर के साथ भूख भी पलती है। सुअर तो खाया जा सकता है लेकिन भूख को इमान चट कर जाने में देर नहीं लगती। दूसरे अति वंचित समुदायों के लिए भी यही सच है।
इन्हीं चिताओं और चुनौतियों की रोशनी में आयोजित होने जा रहा यह सम्मेलन बहुत प्रासंगिक और ज़रूरी है। इस समझ के साथ है कि तमाम वंचित समुदाय अपने-अपने कोने बना कर बेहतरी की कोई मज़बूत लड़ाई नहीं लड़ सकते। आज के हालात में मुसहर जैसे समुदायों का तो अपने बूते उठ खड़ा हो पाना ही लगभग नामुकिन सा है। लेकिन हां, विभिन्न वंचित समूह मिल कर इतनी बड़ी ताक़त ज़रूर हो सकते हैं कि जिसे अनसुना करना या दबाना आसान न हो।
इसका आयोजन स्थानीय स्तर पर सक्रिय तीन जन संगठनों की साझा पहल पर किया जा रहा है- मेहनतकश मोर्चा, आदिवासी वनवासी कल्याण समिति और मानवाधिकार जन चिंतन समिति। आयोजन के सहयोगी की भूमिका में हैं- बिहान मंच और कासा।
जो कमज़ोरों में कमज़ोर हैं, साझा संघर्ष की अगुवाई में उन्हें बराबर की जगह दी जानी चाहिए। इस मायने में आयोजक गंभीर हैं। सम्मेलन की आयोजन समिति में लगभग एक तिहाई मुसहर हैं। हालांकि नट-कंजड़ जैसे समुदायों का इसमें कोई प्रतिनिधित्व नहीं है। बड़ी बात है कि आयोजन समिति के अध्यक्ष हरीराम आदिवासी ने इस ओर इशारा किया। उन्होंने कहा कि हिंदू नट-कंजड़ राज्य में अनुसूचित जनजाति में आते हैं जबकि मुसलमान नट-कंजड़ नहीं। यह सरासर भेदभाव है। उन्हीं के सुझाव पर यह मांग जोड़ी गयी है कि हिंदू नट-कंजड़ की तरह मुसलमान नट-कंजड़ को भी अनुसूचित जनजाति घोषित किया जाये। इसी तरह उन्होंने फ़क़ीर, हेला, चमरमंगता, कंकाली जैसे दूसरे अति वंचित समुदायों को भी इस ताज़ा मुहिम के नेतृत्व में वांछित जगह दिये जाने की वकालत की।
इसी कड़ी में बताते चलें कि सुल्तानपुर जिले के कादीपुर ब्लाक के कमरावां गांव के हरीराम आदिवासी मुसहर समुदाय के गिने-चुने उच्च शिक्षितों में से हैं। उन्होंने एमए की डिग्री हासिल की लेकिन कहीं नौकरी करने के बजाय अपने समुदाय के भले के लिए काम करने का फ़ैसला किया। कहते हैं: पिता अनपढ़ थे लेकिन चाहते थे कि उनका बेटा पढ़े-लिखे। उन्होंने नाम तो लिखवा दिया लेकिन मेरी शामत आ गयी। हेड मास्टर साहब कायस्थ थे। उन्हें बर्दाश्त नहीं था कि कोई मुसहर बच्चा स्कूल जाये। वह बात-बेबात मुझे गालियां देते, मोटे डंडे से बेरहमी से पिटाई करते। ताना देते कि मुसहर की औलाद चला कलेक्टर बनने। मैं उनकी पिटाई से डर कर स्कूल जाने से कतराता तो स्कूल न जाने पर पिता जी पीटते। एक समय तो ऐसा आया कि मैंने उकता कर मर जाने का मन बना लिया। नहर में कूद जाने के लिए चल पड़ा। लेकिन रास्ते में एक दूसरे अध्यापक ने मुंशीजी यानी हेड मास्टर के तबादले की ख़ुशख़बरी सुना दी। इस तरह मैं ख़ुदकशी करने से बचा वरना आज यहां नहीं होता।
यह बानगी है कि स्कूलों तक में मुसहर बच्चों के साथ अच्छा सलूक़ नहीं किया जाता। आज भी इसमें कोई फ़र्क़ नहीं आया है। इसलिए कि पूरे समाज में गहरे तक अपनी जड़ें जमाये जाति आधारित भेदभाव और नफ़रत की स्थिति नहीं बदली है। क़ानून का बन जाना ही इस समस्या का हल नहीं हो सकता।
आयोजन समिति के दूसरे मुसहर सदस्य कुंडली आदिवासी बरही नवादा से तीन किलोमीटर दूर पर बसे धनेथू गांव के वाशिंदे हैं। कहते हैं कि उनके गांव के मुसहरों के पास ना लाल कार्ड है और न जाब कार्ड। उनके पास ज़मीन का कोई पट्टा भी नहीं। स्वास्थ्य केंद्र पांच किलोमीटर दूर नेवगढ़िया बाज़ार में है। यही कहानी दूसरे गांवों के भी मुसहरों की है।
समय की क़िल्लत के चलते बरही नवादा की दल्लीपुर नाम की मुसहर बस्ती का मैं बस चक्कर भर लगा सका। इतने में ही जो दिखा, उसके लिए किसी सर्वेक्षण की ज़रूरत नहीं है। यह भयानक ग़रीबी और अभाव का चीख़ता हुआ नज़ारा है। गांव के कम बच्चे स्कूल जाते हैं। जो स्कूल पहुंचते हैं, उनमें इक्का-दुक्का ही पांचवीं कर पाते हैं। इसके आगे की पढ़ाई कोई नहीं कर सका। वैसे, जहां खाने के लाले पड़े हों और बच्चों को भी कमाई के दो हाथ बना देने की मजबूरी हो, वहां उन्हें स्कूल भेजने की चिंता कौन करे? पढ़ाई पहले कि पेट?
फ़सल कटी नहीं कि मुसहर बच्चे चूहे के शिकार पर निकल पड़ते हैं। भुरभुरी हो गयी मिट्टी उसके नीचे चूहे के मौजूद होने का पता दे देती है। वहीं बिल होते हैं। चूहे को बाहर निकालने के आसान जतन हैं- बिल में धुंआ भरो या पानी, चूहा बाहर निकलने को मजबूर हो जायेगा। सबकी आंखें चौकस हैं। चूहे के बाहर आते ही फ़ुर्ती से उस पर झपट्टा मारना होता है और उसी फ़ुर्ती से उसे ज़मीन पर दे मारना होता है। इसमें कोई चूक नहीं होती। यह विरासत में मिला कौशल है।
मुझे भी पहली बार यह शिकार देखने का मौक़ा मिला लेकिन दुर्भाग्य से हाथ में कैमरा नहीं था। वे स्कूली बच्चे थे। उनकी मदद को एक नौजवान मय लाठी के मौजूद था। किसी को बात करने की फ़ुर्सत नहीं। कोई बिल में पानी उलीच रहा है तो कोई बिलों पर नज़रें गड़ाये धावा बोलने को तैयार है। जिसके हाथ चूहा लगता, उसके चेहरे पर कामयाबी की इतराती मुस्कान उतरती। लेकिन हां, इतनी तमीज़ है कि सबके बीच चूहे का बंटवारा किया जाना है। इसमें कोई छीना-झपटी नहीं। यह कम बड़ी बात है? यह तो सामूहिकता की गवाही है।
पेट की आग इंसान को खोजी बनाती है। बस्ती के कई चूल्हों के पास मिट्टी के छोटे-छोटे गोले जैसे दिखे। मुसहर इसे सेरखी कहते हैं और बाक़ी लोग दुल्हन। यह तालाब में मिलता है। कमल की तरह उसके फूल-पत्ते पानी की सतह पर होता है जबकि उसका यह कंद तालाब के नीचे- ज़मीन के भीतर। इसे निकालना मुश्क़िल तलब होता है। इसे भूंज कर खाया जाता है और जिसका स्वाद कुछ आलू सरीखा होता है। मुसहरों को छोड़ कर इसे कोई नहीं खाता।
कोई 45 साल के करिया आदिवासी ने जो कहा, उसका कुल सार यह कि बस घिसट-घिसट कर जी रहे हैं। खेतों में तिहाई पर काम करते हैं। मतलब कि लागत खेत मालिक की (बीज, खाद, सिंचाई वगैरह) और फ़सल का एक तिहाई हिस्सा मज़दूरी। फ़सल चौपट हुई तो मेहनत गयी पानी में। फ़सल अच्छी हुई तो कोई सात-आठ महीना तक खाने का इंतज़ाम हो जाता है। पेट भरने के लिए साल में कम से कम छह महीना घर से बाहर रहते हैं और ईंट भट्टे पर खटते हैं। एक हज़ार ईंटों की पथाई के 300 रूपये मिलते हैं। मियां-बीबी दोनों के हाथ लगते हैं, तब कहीं जाकर मुश्किल से दो दिन में इतनी पथाई हो पाती है- हरेक की रोज़ाना मज़दूरी ज़्यादा से ज़्यादा 75 रूपये। इसमें मिट्टी तैयार करना भी शामिल है यानी रूंदना।
वैसे, ख़बर यह भी है कि ईंट भट्टे अब कुछ साल के मेहमान हैं। इसलिए कि प्रदूषण पर लगाम लगाने के लिए सरकार ईंट भट्टों को बंद कर औद्योगिक कचरे से ईंट बनाये जाने का फ़ैसला करने जा रही है।
दल्लीपुर के कई घरों के बाहर धान फैला हुआ है- कोई गमछे भर जितनी जगह में। कहीं उससे कंकड़-पत्थर की बिनाई हो रही है तो कहीं उसकी कुटाई। यह फ़सल कटने के बाद खेत में छूट गये धान को झाड़ू से बुहार कर जमा किया गया है। इससे अधिक से अधिक डेढ़ किलो चावल मिलना है। यह कम से कम दो औरतों की दिन भर की कमाई है।
लेकिन आसपास के खेतों से पूरी बस्ती के लिए इतना धान नहीं बटोरा जा सकता। इसलिए हमेशा की तरह इस बार भी बड़ी संख्या में मुसहर परिवार पंजाब चले गये हैं। वहां धान बटोरने लायक़ खेतों की कमी नहीं। उनकी वापसी अगली जनवरी के बीच तक होगी। इस बीच उन्हें धान के साथ चूहे भी इफ़रात में मिलेंगे।
पलायन के अलावा कोई दूसरा चारा भी तो नहीं। पत्तल बनाना-बेचना मुसहरों का पुराना काम रहा है। इस धंधे में मशीनों और पूंजीपतियों ने हाथ डाले तो पत्तल की सूरत बदल गयी। पत्तल प्लेट जैसे सपाट हो गये। मुसहरों के हाथों से बने ऊबड़-खाबड़ पत्तलों का ज़माना लदने लगा। इलाक़े से महुआ और पलाश (वनफूल) के पेड़ भी ग़ायब होने लगे जिसके चौड़े पत्ते पत्तल बनाने के काम आते रहे हैं। उसी की तलाश में भटकते हुए बरही नवादा के आसपास के कई परिवार बाराबंकी के देवां ब्लाक तक पहुंच गये और वहीं बस गये। उनकी भी वही हालत है। पांच-छह साल पहले तो बड़े लोगों ने अपने खेतों में उनकी हगनी-मुतनी बंद किये जाने का फ़रमान सुना दिया था।
ख़ैर, दल्लीपुर से लगा हुआ कोई पांच बीघे का तालाब है। यह गांव समाज की संपत्ति है लेकिन इस पर कुछ दबंग पटेल अपनी दावेदारी करने की फ़िराक़ में हैं। इसको लेकर तनातनी है। वैसे, पूरे इलाक़े के ज़्यादातर पटेल ग़रीब हैं और सदियों से सवर्ण जातियों के हाथों उत्पीड़ित रहे हैं। इस नाते दूसरी उत्पीड़ित जातियों के साथ उनका अपेक्षाकृत हमदर्दी का रिश्ता रहा है- अवध क्षेत्र से ठीक उलट जहां कुर्मी (पटेल का स्थानीय संबोधन) दबंग और ताक़तवरों में गिने जाते हैं।
12 साल की पूजा का बुरा हाल है। वह सूखी टहनी जैसी है। माता-पिता उसके बचपन में ही चल बसे। उसने होश संभाला तो चाचा अपनी बीबी और दो बच्चों को छोड़ कर किसी दूसरी के साथ भाग गया। चाची भी बच्चों को छोड़ कर किसी और के साथ हो ली। रह गये दो मासूम बच्चे, 50 साल पार चुकी दादी और वह ख़ुद। पिछले चार सालों से वह दोनों बच्चों की मां की भूमिका में है। दादी इधर-उधर मज़दूरी के लिए भटकती है। फ़सल कटाई के बाद दूसरी तमाम औरतों की तरह वह भी खेतों में यहां-वहां पड़े धान को जमा करने का काम करती है। पूजा के पास केवल दो जोड़ी सूती कपड़ा है। पता नहीं सर्दी की रातें कैसे कटती होंगी? इसे जीना नहीं, घिसट-घिसट कर जीना, तिल-तिल कर मरना कहते हैं।
इधर राजनैतिक दलों के बीच लोकसभा चुनाव की गहमागहमी बढ़ती जा रही है। वोट पक्के करने की जुगत बिठाने का काम तेज़ी पर है लेकिन अति वंचितों का भला किये जाने की घोषणाएं और वायदे (भले ही रिझाने के झूठ और फ़रेब के बतौर ही सही) कहीं नहीं हैं। मान लिया गया है कि मुसहर और उन जैसे अति वंचित समुदायों को दारू, मुर्गा, साड़ी, रूपया या धमक से बस हांका जाना है तो इतनी इसकी क्या ज़रूरत? यह स्थिति इसलिए है कि वंचितों की कोई राजनैतिक ताक़त नहीं।
2 दिसंबर का सम्मेलन इसी ग़रज़ से है ताकि यथास्थिति के टूटने की शुरूआत हो। अहम बात यह भी कि इसके आयोजन में दलितों और पिछड़े मुसलमानों का भी हाथ लगनेवाला है। उदाहरण के तौर पर आयोजन समिति में अगर बरही नवादा के एमए-बीएड दलित ग्राम प्रधान आशीष कुमार शामिल हैं तो कालीन उद्योग में डिज़ाइनर के तौर पर काम कर रहे कफ़ील अंसारी भी हैं। इसी तरह बड़ागांव के ब्रजमोहन वनवासी हैं तो स्थानीय व्यापारी नेता अब्दुल रशीद और हमीरापुर के दलित कार्यकर्ता बनारसी भी। तय हुआ है कि सम्मेलन का संचालन श्यामबली पटेल करेंगे जो कोई पांच किलोमीटर दूर बड़ागांव स्थित बल्देव डिग्री कालेज छात्र संघ के पूर्व महामंत्री हैं।