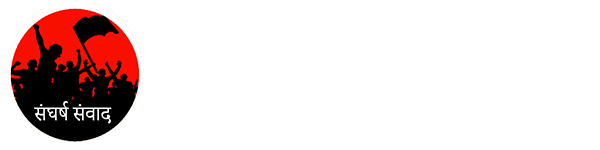संविधान के हक़ में
आज़ादी के समय लोकतंत्र व्यवस्था के साथ-साथ एक स्वप्न भी था-संवेदना, संवाद और संघर्ष से उमग रहा ओजस्वी सपना! यह ऐसा समय था जब संविधान सभा की बहसें नए गणतंत्र की नैतिक आकांक्षा का पारदर्शी प्रतिनिधित्व कर रही थीं। नैतिक आकांक्षा इसलिए कि सारी आकांक्षाएँ नैतिक नहीं थीं। कुछ सांप्रदायिक और निहित स्वार्थ तब भी सिर उठा रहे थे और अपने संकीर्ण हितों को राष्ट्र से बड़ा मान रहे थे। यह बात हम जानते हैं। किसी भी विमर्श की पहली आवश्यकता होती है कि कुछ मूलभूत मुद्दों पर हम न्यूनतम सहमति बनाकर आगे बढ़ें। इस बात से सहमत हैं तो हम आगे बढ़ें।
ये नैतिक आकाक्षाएँ क्या थीं? सामान्य शब्दों में, ये थीं- समानता, स्वतंत्रता, बंधुत्व, भेदभाव (धार्मिक, जातीय, लैंगिक) का निषेध, समान न्याय प्रणाली इत्यादि।
आज जब इन नैतिक आकांक्षाओं का अवमूल्यन होते हुए हम देख रहे हैं, और “लोकतंत्र ख़तरे में है”, “संविधान ख़तरे में है” जैसे वाक्य सुनते हैं, तब यह आवश्यक हो जाता है कि हम अपने समय के यथार्थ को उन मूल विचारों की रोशनी में समझें जो भारत के गणराज्य का बीज बने थे। अन्यथा ये निर्णयात्मक कथन अपनी वैधता नहीं साबित कर पायेंगे।
यह विश्लेषण मैं संवैधानिक, ऐतिहासिक, राजनीतिक, समाजशास्त्रीय और राजनीतिक-मनोवैज्ञानिक संदर्भों से करना चाहता हूँ और एक-एक प्रतिनिधि विचारक के माध्यम से अपनी बात रखना युक्ति-युक्त समझता हूँ।
संविधान-विद् डॉ.भीमराव आम्बेडकर ने जब यह कहा कि “We are going to enter into a life of contradictions…” तो इसका मतलब क्या था?
आज़ादी के समय भारत विपन्न था, सामाजिक असमानता थी और क्षेत्रीय तथा संकीर्ण ताक़तें अपना सिर उठा रही थीं। ऐसे में डॉ. भीमराव आम्बेडकर के ऐसा कहना, कि हम विरोधाभासों के युग में प्रवेश करने जा रहे हैं, यथातथ्यता की बात नहीं थी बल्कि एक चेतावनी थी…और चेतावनी को संकल्प में बदलना था। संकल्प यह कि ग़रीबी दूर करनी है, कि असमानता मिटानी है, कि भेदभाव समाप्त करने हैं।
और यह सब कैसे होगा? यह तब होगा जब हम मानेंगे कि लोकतंत्र केवल संवैधानिक ढाँचा नहीं है, वह एक सामाजिक-राजनीतिक-आर्थिक क्रांति है—एक ऐसी नैतिक शपथ, जो तब तक अपूर्ण रहेगी जब तक भारत जाति, पूँजी और धर्म के वर्चस्व के भाव से मुक्त न हो जाए, संकीर्णता समाप्त न हो जाए।
उन्होंने चेताया था कि यदि ‘राजनीति में हम समानता स्वीकार करेंगे, परंतु सामाजिक और आर्थिक जीवन में असमानता बनाए रखेंगे,’ तो बात बनेगी नहीं…न लोकतंत्र टिकेगा, न संवैधानिक व्यवस्था का सार बचेगा।
आज जब दलितों, आदिवासियों, स्त्रियों और अल्पसंख्यकों पर अत्याचार, पीट-पीटकर हत्या और संस्थागत भेदभाव की ख़बरें आती हैं तो क्या आम्बेडकर की चेतावनी हमारे चारों ओर नहीं गूँज रही होती है?
उनके अनुसार “बंधुता” केवल संविधान की प्रस्तावना में दर्ज शब्द नहीं, बल्कि लोकतंत्र की प्राणवायु है। राजनीतिक प्रतिनिधित्व बढ़ा है, परंतु सामाजिक समावेश कितना बढ़ा है? आम्बेडकर जिस बंधुता की बात करते हैं, वह सार्वजनिक जीवन से आज भी लुप्तप्राय है या नहीं?
इतिहासकार बिपन चंद्र ने सांप्रदायिकता पर काफ़ी समग्रता से विचार किया है। वे इसे औपनिवेशिक शक्तियों के छल से उपजी मानते हैं और इसके विभिन्न चरणों की चर्चा करते हैं। उनके मत में, ब्रिटिश शासन ने मुसलमानों, हिंदुओं, सिखों, आदि को अलग-अलग समुदायों के रूप में देखा और उन्हें एक-दूसरे के विरोधी हित-समूहों की तरह रखा।
ऐतिहासिक तथ्य इस विश्लेषण की पुष्टि करते हुए देखे जा सकते हैं।
हम ग़ौर करें तो पायेंगे कि 1909, 1919 के ब्रिटिश अधिनियम और 1932 में पृथक निर्वाचक मंडल के प्रावधान इत्यादि ने धार्मिक तथा अन्य पहचानों के आधार पर राजनीतिक प्रतिनिधित्व को संस्थागत स्वरूप दिया था। इससे ‘राजनीतिक इकाई के रूप में समुदाय’ (community as political unit) का विचार मज़बूत हुआ।
पुन: मुस्लिम लीग, हिंदू महासभा जैसे संगठन सांप्रदायिक विचारधारा को बढ़ावा देने लगे, और 1937 के चुनावों के बाद इस प्रतिस्पर्धा ने तीव्र रूप धारण किया। ये सांप्रदायिक शक्तियाँ भारत के समावेशी राष्ट्रवाद की अवधारणा को चुनौती देती थीं, जिससे स्वतंत्रता आंदोलन की धार कमज़ोर होती थी। यह अंग्रेजों के स्पष्ट हित में था।
स्वतंत्रता के बाद हालाँकि भारत में राजनीतिक रूप से सांप्रदायिकता को हाशिये पर डाला गया, उसे हतोत्साह किया गया और नेहरू ने धर्मनिरपेक्षता को संस्थागत करने की कोशिश की, परंतु यह सामाजिक संरचना और मनोवृत्तियों में जीवित रही (“Communalism after 1947 was no longer a dominant ideology, but remained a potent social force.”)। आज़ाद भारत में हुए सांप्रदायिक दंगों ने दिखाया कि सांप्रदायिकता केवल विचारधारा नहीं, हिंसा और राजनीतिक लामबंदी का यंत्र बन चुकी है।
बिपन चंद्र ने अपने लेखन में बार-बार इस बात पर ज़ोर दिया कि सांप्रदायिकता मध्यमवर्गीय नेतृत्व और अवसरवादी अभिजन शक्तियों की वह रणनीति है जिससे वह अपने सामाजिक-आर्थिक हितों को छिपाकर धार्मिक पहचान के माध्यम से लोगों को लामबंद करते हैं। बिपन चंद्र उस ख़तरनाक मोड़ की ओर संकेत करते हैं जब सांप्रदायिकता को सत्ता के गलियारों से वैधता मिलने लगी- “The communal ideology began to acquire mass base only when supported by sections of the ruling classes and state institutions.”
उन्होंने चेतावनी दी थी कि यदि सांप्रदायिक शक्तियों को सत्ता मिलती है, तो वे राष्ट्र को एक धर्माधारित राज्य की ओर मोड़ सकती हैं।
आज सांप्रदायिक-मानस के असंख्य शेड्स बन गए हैं और पहचान-मात्र शत्रुता की वजह बनती जा रही है। बौद्धिक-वर्ग भी सांप्रदायिक भाव-विचार से अपने को बचा नहीं पा रहा है। यह शक्ति की वैधता द्वारा सत्य की वैधता को दी गई चुनौती तो नहीं है?
आधुनिक भारत के विद्वान राजनीतिशास्त्री रजनी कोठारी ने लोकतंत्र को केवल संस्थाओं का तंत्र नहीं, बल्कि राजनीतिक कल्पनाशक्ति का अभ्यास कहा था और चेताया था कि “Decline of imagination precedes decline of institutions”। उनके अनुसार, जब विकासात्मक राज्य अपने सामाजिक वादों में विफल होता है, तो वह भावनात्मक और सांस्कृतिक मुद्दों की शरण में चला जाता है।
ग़ौर कीजिए, आज कौन-से मुद्दे रोज़गार, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे सवालों को विस्थापित कर रहे हैं?
लोकतंत्र संवाद पर आधारित था, अब वह स्वीकृति और समर्पण पर आधारित होता जा रहा है।
उनकी चेतावनी आज के समय में गूँज रही है क्या, सोचिए- “When the state fails to be a distributor of welfare, it becomes a producer of symbols.”
विकासशील समाज अध्ययन पीठ (CSDS) केवरिष्ठ समाजशास्त्री धीरुभाई शेठ भारत में लोकतंत्र के एक मौलिक व्याख्याकार माने जाते हैं जिन्होंने हमारे लोकतंत्र को उसकी जातीय, सामाजिक और सांस्कृतिक विविधताओं व बहुलताओं के भीतर से देखने-समझने की दिशा दी है। उन्होंने भारतीय लोकतंत्र को पश्चिमी मॉडल में नहीं, बल्कि “बहुलतावादी यथार्थ” (pluralistic reality) के साथ देखने की अपील की। शेठ के अनुसार, जाति और लोकतंत्र विरोधी नहीं हैं, बल्कि जातियाँ भारत में लोकतंत्र के प्रवेश द्वार बन सकती हैं। वे मानते थे कि: “In India, caste has become a medium for democratization, not merely a relic of feudalism.” जातीय पहचानें, जब राजनीतिक मंच पर आती हैं, तो वे हाशिये के तबकों को प्रतिनिधित्व, अधिकार और स्वायत्तता की लड़ाई में ताक़त देती हैं। उनका विमर्श पहचान को ‘अधिकार और भागीदारी’ के नियामक के रूप में देखता है।
धीरुभाई शेठ भारतीय लोकतंत्र को ‘नाज़ुक पर स्पंदित लोकतंत्र’ कहते हैं। उनके अनुसार, भारत में लोकतंत्र संस्थागत स्थायित्व की तुलना में राजनीतिक समाजीकरण और सांस्कृतिक संवाद की वजह से जीवित है। ग्राम्शी के विचारों से प्रभावित शेठ ने कहा कि भारत में ऊपर से किया गया बदलाव काफ़ी नहीं है। “Indian democracy needs a second democratic upsurge, rooted in social movements, not just electoral shifts.” यहाँ उनका इशारा दलित, महिला, पर्यावरण, और किसानों के आंदोलनों की ओर था जो संस्थागत लोकतंत्र को सामाजिक लोकतंत्र से जोड़ते हैं।
शेठ राज्य पर अत्यधिक निर्भरता को एक लोकतांत्रिक ख़तरा मानते थे। उनका मानना था कि जब तक नागरिक समाज मज़बूत नहीं होगा और सत्ता पर जन-निगरानी नहीं होगी, तब तक लोकतंत्र प्रतीक-मात्र रहेगा। “Democracy in India is sustained by protest and participation, not by obedience.”
उनके अनुसार, भारतीय लोकतंत्र संस्कृति-विरोधी नहीं, संस्कृति-संवादी होना चाहिए। उन्होंने धर्मनिरपेक्षता को केवल राज्य की तटस्थता नहीं, बल्कि सांस्कृतिक बहुलता के साथ संवाद की प्रक्रिया के रूप में परिभाषित किया। आज जब लोकतंत्र लोक के विमर्शों से दूर और राज्य के नारों में सीमित होता जा रहा है, धीरुभाई शेठ की यह चेतावनी और भी अर्थवान लगती है: “A democracy without democratization is a mirage.” लोकतंत्र को केवल चुनावों का नहीं, ‘गरिमा और न्याय के लिए रोज़मर्रा के मोलतोल’ (everyday negotiation of dignity and justice) का मंच होना चाहिए।
राजनीतिक मनोविज्ञानी आशीष नंदी ने भारत में सांप्रदायिकता के सामाजिक, राजनीतिक और मानसिक प्रभावों का गहरा विश्लेषण किया है। वे सांप्रदायिकता को एक समाजशास्त्रीय और मानसिकता आधारित परिघटना मानते हैं, जो केवल राजनीतिक रणनीतियों तक सीमित नहीं है, बल्कि एक सांस्कृतिक और मानसिक प्रक्रिया भी है। नंदी ने सांप्रदायिकता की जड़ें ब्रिटिश साम्राज्य में पायीं, जो भारत में बाँटो और राज करो की नीति के तहत विभिन्न धार्मिक और सामाजिक समुदायों के बीच अंतर और घृणा बढ़ाता था। इस दृष्टिकोण के तहत, साम्राज्य ने भारतीय समाज को धार्मिक रूप से विभाजित किया, और एक राजनीतिक “पार्टीशन” की मानसिकता तैयार की, जो स्वतंत्रता के बाद भी बनी रही। वे यह भी मानते थे कि अंग्रेजों ने हिंदू-मुस्लिम विरोध को इस हद तक बढ़ा दिया कि यह एक स्थायी सामाजिक बँटवारा बन गया। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम ने एक सामूहिक भारतीय पहचान बनाने का प्रयास किया, लेकिन सांप्रदायिक ताक़तों ने इसे अपने राजनीतिक लाभ के लिए बाधित किया। यह मानसिक विभाजन तब और भी गहरा हो जाता है जब राजनीतिक दल इस विभाजन का सामाजिक और राजनीतिक फ़ायदा उठाते हैं।
आशीष नंदी ने यह भी स्पष्ट किया कि आधुनिक समय में सांप्रदायिकता की प्रवृत्तियाँ नयी रणनीतियों के तहत विकसित हो रही हैं। यह केवल धार्मिक मसलों तक सीमित नहीं रह गई है, बल्कि राजनीतिक पहचान, जातीय अस्मिता, और समाज के अन्य विभाजनों के माध्यम से नया रूप ले चुकी है।
आशीष नंदी ने सांप्रदायिकता से निपटने के लिए लोकतांत्रिक और समावेशी दृष्टिकोण की आवश्यकता पर बल दिया। वे मानते हैं कि भारतीय समाज में धर्मनिरपेक्षता केवल एक राजनीतिक आदर्श नहीं होनी चाहिए, बल्कि इसे सांस्कृतिक और सामाजिक मूल्यों के रूप में समाज में गहरे तरीक़े से स्थापित किया जाना चाहिए।
आज जब लोकतंत्र का क्षरण हमारे समकालीन यथार्थ का हिस्सा बनता जा रहा है, तब यह पूछना अप्रासंगिक हो गया है कि लोकतंत्र ख़तरे में है या नहीं; अब सवाल यह है कि उस ख़तरे ने कैसा स्वरूप ग्रहण कर लिया है। भारत में यह ख़तरा बहुस्तरीय है—सांस्कृतिक वर्चस्ववाद, सामाजिक बहिष्करण, आर्थिक असुरक्षा, और वैचारिक संकुचन ने मिलकर उस गणराज्य की आत्मा को आहत कर दिया है जिसकी कल्पना संविधान सभा ने एक न्यायप्रिय, बहुल और समावेशी राष्ट्र के रूप में की थी।
इस ऐतिहासिक मोड़ पर हमें न केवल संविधान सभा की नैतिक दूरदर्शिता की ओर लौटना होगा, बल्कि बिपिन चंद्र, रजनी कोठारी, धीरुभाई शेठ, आशीष नंदी और विशेषकर डॉ.भीमराव आम्बेडकर जैसे बौद्धिक स्तंभों की ओर भी मुड़ना होगा, जिनकी चेतावनियाँ आज सच होती प्रतीत हो रही हैं।
बहुराष्ट्रीय और एकाधिकार पूँजीवाद ने जिन नये आर्थिक संकटों को जन्म दिया है और ग़ैर-बराबरी जितनी मारक हो गई है, वह सारी दुनिया में जनतांत्रिक विचार-भावना को गंभीर क्षति पहुँचा रही है। राज्य अपनी कल्याणकारी भूमिका छोड़ देता है, वंचित समुदाय और अधिक हाशियाकृत होता है, आजीविका के संकट गहराते हैं। ये संकट राजनीतिक रूप से नस्लीय और धार्मिक अल्पसंख्यकों को को बहुसंख्यकों के क्रोध और उनकी नफ़रत का शिकार बनाता है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स अपने अलगॉरिद्मिक बॉयस के ज़रिये इस नफ़रत और ध्रुवीकरण को बढ़ावा देते हैं।
हमें पुनः उस लोकतांत्रिक भाव के लिए गंभीरता से कोशिश करनी होगी जहाँ नागरिकता अधिकार से परिभाषित हो, पहचान से नहीं; जहाँ वाद-विवाद का स्थान हो, हिंसा और चुप्पी का नहीं। यह कार्य केवल नीतियों से नहीं होगा-यह एक नैतिक संस्कृति के पुनर्निर्माण से संभव होगा, जहाँ करुणा, समता और विवेक की पुनः प्रतिष्ठा हो और यह हमारे जनतंत्र में तभी फलीभूत होगा जब हम संवैधानिक नैतिकता की बातें नहीं करेंगे बल्कि उसे जीने लगेंगे।
_____________________________________________________________________
महेश मिश्र का यह आलेख नयापथ से साभार लिया गया है।