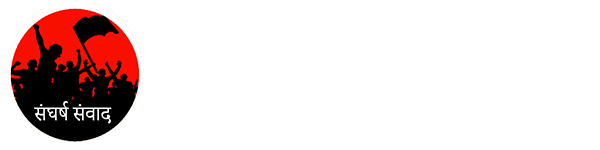भारत के ट्रेड यूनियन आंदोलन की समस्याएं
28 सितंबर शंकर गुहा नियोगी की शहादत का
दिन है। बीस साल पहले इसी दिन उन्हें गोलियों का शिकार बनाया गया था। यह
उद्योगपतियों का घिनौना कारनामा था जिनकी मज़दूर विरोधी नीतियों की राह में नियोगी
जी बहुत बड़ा रोड़ा बन गये थे। वे मज़दूर हितों के निडर और अडिग योद्धा थे। विचार, संघर्ष और रचनाशीलता उनकी सक्रियताओं का
प्रस्थान बिंदु था। वे ट्रेड यूनियन आंदोलन को अर्थवाद के संकीर्ण जाल से बचाते
हुए उसे व्यापक बदलाव के मोर्चे की अगली क़तार में खड़ा करने की मुहिम पर थे। वे
मज़दूरों के ही बीच जितना लोकप्रिय थे,
उससे
कहीं ज़्यादा उनके परिवारों के बीच लोकप्रिय थे। समाज के विभिन्न ग़रीब और मेहनतकश
तबक़े उन्हें अपना भरोसेमंद हमसफ़र मानते थे। नियोगी जी इतने सहज-सरल और उदार थे।
त्याग, सहिष्णुता, ईमानदारी, सादगी, समर्पण, आशावादिता, जुझारूपन जैसे विराट मूल्यों और
प्रवृत्तियों ने शहीद नियोगी की अमर तसवीर गढ़ने का काम किया है।
दिन है। बीस साल पहले इसी दिन उन्हें गोलियों का शिकार बनाया गया था। यह
उद्योगपतियों का घिनौना कारनामा था जिनकी मज़दूर विरोधी नीतियों की राह में नियोगी
जी बहुत बड़ा रोड़ा बन गये थे। वे मज़दूर हितों के निडर और अडिग योद्धा थे। विचार, संघर्ष और रचनाशीलता उनकी सक्रियताओं का
प्रस्थान बिंदु था। वे ट्रेड यूनियन आंदोलन को अर्थवाद के संकीर्ण जाल से बचाते
हुए उसे व्यापक बदलाव के मोर्चे की अगली क़तार में खड़ा करने की मुहिम पर थे। वे
मज़दूरों के ही बीच जितना लोकप्रिय थे,
उससे
कहीं ज़्यादा उनके परिवारों के बीच लोकप्रिय थे। समाज के विभिन्न ग़रीब और मेहनतकश
तबक़े उन्हें अपना भरोसेमंद हमसफ़र मानते थे। नियोगी जी इतने सहज-सरल और उदार थे।
त्याग, सहिष्णुता, ईमानदारी, सादगी, समर्पण, आशावादिता, जुझारूपन जैसे विराट मूल्यों और
प्रवृत्तियों ने शहीद नियोगी की अमर तसवीर गढ़ने का काम किया है।
नियोगी शहादत दिवस पर हम यहां उनके भाषण
पर आधारित यह आलेख पेश कर रहे हैं जो पहली बार अगस्त 1990 में छमुमो की ‘लोक साहित्य परिषद’ द्वारा एक पुस्तिका के रूप में प्रकाशित
किया गया था। नियोगी जी की हत्या के बाद उनके कागजातों में ‘इस्पात ट्रेड यूनियन:
नयी दिशा की तलाश’ शीर्षक एक पांडुलिपि
मिली। खोजबीन के बाद पता चला कि यह पांडुलिपि उस भाषण पर आधारित है जो नियोगी जी
ने अक्टूबर 1982 में दल्ली राजहरा में ‘अखिल भारतीय इस्पात
समन्वय समिति’ के तत्वावधान में आयोजित सम्मेलन में दिया था। यह
भाषण भले ही इस्पात उद्योग की ट्रेड यूनियनों के संदर्भ में दिया गया था लेकिन
उसका मूल तत्व सभी ट्रेड यूनियनों पर लागू होता है। पुस्तिका को 1984 में
राजनांदगांव के कपड़ा मजदूर आंदोलन के दौरान मजदूरों की शिक्षण सामग्री के बतौर
प्रकाशित किया गया था।
पर आधारित यह आलेख पेश कर रहे हैं जो पहली बार अगस्त 1990 में छमुमो की ‘लोक साहित्य परिषद’ द्वारा एक पुस्तिका के रूप में प्रकाशित
किया गया था। नियोगी जी की हत्या के बाद उनके कागजातों में ‘इस्पात ट्रेड यूनियन:
नयी दिशा की तलाश’ शीर्षक एक पांडुलिपि
मिली। खोजबीन के बाद पता चला कि यह पांडुलिपि उस भाषण पर आधारित है जो नियोगी जी
ने अक्टूबर 1982 में दल्ली राजहरा में ‘अखिल भारतीय इस्पात
समन्वय समिति’ के तत्वावधान में आयोजित सम्मेलन में दिया था। यह
भाषण भले ही इस्पात उद्योग की ट्रेड यूनियनों के संदर्भ में दिया गया था लेकिन
उसका मूल तत्व सभी ट्रेड यूनियनों पर लागू होता है। पुस्तिका को 1984 में
राजनांदगांव के कपड़ा मजदूर आंदोलन के दौरान मजदूरों की शिक्षण सामग्री के बतौर
प्रकाशित किया गया था।
किसी
भी देश के विकास के लिए उद्योग की स्थापना एवं उसका निरंतर विकास होना जरूरी है।
पिछली शताब्दी के अंत तक भारत में औद्योगिक विकास उल्लेखनीय नहीं रहा। अंग्रेज
लौह-इस्पात, भारी
मशीन, कपड़ा, दवाई आदि इंग्लैंड से मंगाकर अपना धंधा
चलाते थे। मुनाफा बटोरना अंग्रेजों का एकमात्र उद्देश्य था।
भी देश के विकास के लिए उद्योग की स्थापना एवं उसका निरंतर विकास होना जरूरी है।
पिछली शताब्दी के अंत तक भारत में औद्योगिक विकास उल्लेखनीय नहीं रहा। अंग्रेज
लौह-इस्पात, भारी
मशीन, कपड़ा, दवाई आदि इंग्लैंड से मंगाकर अपना धंधा
चलाते थे। मुनाफा बटोरना अंग्रेजों का एकमात्र उद्देश्य था।
सन् 1947 के बाद अंग्रेज तो चले गये लेकिन उनके धंधे
ज्यों-के-त्यों रह गये। उसके बाद विभिन्न बहुराष्ट्रीय कंपनियों, विशेष रूप से अमेरिकी, जापानी, फ्रांसीसी एवं जर्मन
कंपनियों ने भारत के उद्योग-धंधों में हाथ डाला। हत्यारी यूनियन कार्बाइड उनमें से
एक है।
ज्यों-के-त्यों रह गये। उसके बाद विभिन्न बहुराष्ट्रीय कंपनियों, विशेष रूप से अमेरिकी, जापानी, फ्रांसीसी एवं जर्मन
कंपनियों ने भारत के उद्योग-धंधों में हाथ डाला। हत्यारी यूनियन कार्बाइड उनमें से
एक है।
उद्योग और भारत
वर्तमान समय में भारत के उद्योग-धंधें मूलतः तीन
प्रकार के मालिक वर्ग के कब्जे में हैं-
प्रकार के मालिक वर्ग के कब्जे में हैं-
- सार्वजनिक क्षेत्र के मालिक- देश में वर्तमान में सार्वजनिक क्षेत्र
के तहत चालीस हजार करोड़ से भी अधिक लागत के कल-कारखाने, उद्योग-धंधे चल रहे हैं।
इस्पात, बिजली, कपड़ा, रेल, कोयला, तेल आदि उद्योगों में ज्यादातर सार्वजनिक क्षेत्र का कब्जा है। - बहुराष्ट्रीय कंपनियां- विदेशी कंपनियों, विशेष रूप से साम्राज्यवादी
देशों के पूंजीपतियों ने सारी दुनिया के उद्योग-धंधों पर अपने कब्जे जमा रखे
हैं। सिर्फ समाजवादी देशों में ही उनके शिकंजे कमजोर हैं। साम्राज्यवादी
दुनिया का मालिक वर्ग हमारे देश में भी इंजीनियरिंग, दवाई, आटोमोबाइल, चाय, रबर, केमिकल्स
आदि क्षेत्रों में उद्योग-धंधा चला रहा है। - इजारेदार पूंजीपति- तीसरे, महत्वपूर्ण पूंजीपति हमारे ही देश के इजारेदार
पूंजीपति हैं, जैसे बिड़ला, टाटा, डालमिया, किर्लोस्कर, महेन्द्रा आदि। देश में
टेक्सटाइल, केमिकल्स, इस्पात आदि अनेकानेक
उद्योग-धंधों पर इनका कब्जा है।
इसके अलावा कुछ पूंजीपति अपने उद्योग-धंधें के लिए
जी-तोड़ कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन इन्हें अधिक कामयाबी नहीं मिल पा
रही है। ये असंगठित रहने के कारण सरकार व बहुराष्ट्रीय कंपनियों की शोषण की नीति
का कुफल भोग रहे हैं और अपना गुस्सा अपने ही उद्योग में कार्यरत मजदूरों के ऊपर
निकालते रहते हैं।
जी-तोड़ कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन इन्हें अधिक कामयाबी नहीं मिल पा
रही है। ये असंगठित रहने के कारण सरकार व बहुराष्ट्रीय कंपनियों की शोषण की नीति
का कुफल भोग रहे हैं और अपना गुस्सा अपने ही उद्योग में कार्यरत मजदूरों के ऊपर
निकालते रहते हैं।
छत्तीसगढ़ में दिन-ब-दिन उद्योगों का विकास होता जा
रहा है। औद्योगिक विकास की गुंजाइश भी प्रचुर है। जितना विकास अब तक हो चुका है, वह भी कम नहीं है।
रहा है। औद्योगिक विकास की गुंजाइश भी प्रचुर है। जितना विकास अब तक हो चुका है, वह भी कम नहीं है।
यह सवाल बार-बार उठता रहता है कि छत्तीसगढ़ में
औद्योगिक विकास के साथ तालमेल रखकर छत्तीसगढ़ की जनता का विकास क्यों नहीं हो रहा
है? इस सवाल का जवाब
संगठित मजदूर वर्ग ही दे सकता है। संगठित मजदूर वर्ग अगर अपनी ट्रेड यूनियन को एक
स्कूल और हथियार के रूप में इस्तेमाल करे,
संघर्ष
एवं रचना के सिद्धांत पर आधारित अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाये, तभी छत्तीसगढ़ का मजदूर राज्य के विकास
के साथ अपना संबंध बना सकेगा, स्वार्थी पूंजीपति
वर्ग के किराये का टट्टू बन कर नहीं नाचेगा, हर क्षेत्र में
मजदूरों का दबदबा बन सकेगा।
औद्योगिक विकास के साथ तालमेल रखकर छत्तीसगढ़ की जनता का विकास क्यों नहीं हो रहा
है? इस सवाल का जवाब
संगठित मजदूर वर्ग ही दे सकता है। संगठित मजदूर वर्ग अगर अपनी ट्रेड यूनियन को एक
स्कूल और हथियार के रूप में इस्तेमाल करे,
संघर्ष
एवं रचना के सिद्धांत पर आधारित अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाये, तभी छत्तीसगढ़ का मजदूर राज्य के विकास
के साथ अपना संबंध बना सकेगा, स्वार्थी पूंजीपति
वर्ग के किराये का टट्टू बन कर नहीं नाचेगा, हर क्षेत्र में
मजदूरों का दबदबा बन सकेगा।
छत्तीसगढ़ के औद्योगिक मजदूर गुणात्मक सामाजिक
परिवर्तन में एक निर्णायक इस्पाती नेतृत्व देने में कामयाब हो सकते हैं।
परिवर्तन में एक निर्णायक इस्पाती नेतृत्व देने में कामयाब हो सकते हैं।
विभिन्न उद्योगों में फौलादी ट्रेड यूनियन नेतृत्व का
अभाव क्यों?
अभाव क्यों?
- देश की जनता विभिन्न वर्गों और राष्ट्रीयताओं में बैठी हुई है। हर
वर्ग के अपने अलग वर्ग-हित होते हें और विभिन्न राष्ट्रीयताओं के हित भी भी
अलग होते हैं। अब तक भारत में वैज्ञानिक पद्धति और विचारधारा के अनुसार
विभिन्न शोषित वर्गों और विभिन्न राष्ट्रीयताओं की जनता के बीच एकता का आधार
नहीं बनाया गया है। इस कार्य में ट्रेड यूनियनों की विशेष भूमिका को भी
नजरअंदाज किया गया है। - शोषक वर्ग अपनी बनायी व्यवस्था के जरिये ही जिंदा है। शोषण पर आधारित
शोषक वर्ग की व्यवस्था को सिर्फ उस क्षेत्र विशेष की जनता की जरूरतों के मुताबिक
क्षेत्र में उपलब्ध कच्चे माल का भरपूर उपयोग करते हुए एक नयी उत्पादन पद्धति
के विकास के जरिये, उस क्षेत्र की जनशक्ति के बलबूते पर, वैकल्पिक
व्यवस्था कायम करने के लिए किये गये संघर्ष के द्वारा ही ध्वस्त किया जा सकता
है। ट्रेड यूनियनों ने इस विषय पर कभी भी सृजनात्मक दिशा देने के लिए सोचा ही
नहीं। - कुछ वर्ग मौजूदा व्यवस्था को बनाये रखना चाहते हैं, बाकी वर्ग इस व्यवस्था को
खत्म करना और नयी व्यवस्था को कायम करना चाहते हैं। इन परस्पर विरोधी वर्ग
समूहों में जीत किसकी होगी, किसकी बात चलेगी? इसका
साफ जवाब है कि जो वर्ग बुद्धि और भौतिक शक्ति में ज्यादा ताकतवर होगा, विजय उसी की होगी।
वर्तमान समय में निश्चित रूप से पूंजीपति वर्ग तथा
सामंतवादी तत्व ही अधिक बुद्धिमान और शक्ति-सम्पन्न है। उनकी बुद्धि का मुकाबला
करने के लिए हमें अपनी बुद्धि का विकास करना होगा। इसके लिए चार कार्य साथ-साथ
जरूरी हैं- वर्ग संघर्ष, उत्पादन
संघर्ष, वैज्ञानिक प्रयोग और
इतिहास का अध्ययन। हमारी शक्ति के विकास के लिए हमें व्यापक जनता को जगाने का काम
लगातार करना होगा।
सामंतवादी तत्व ही अधिक बुद्धिमान और शक्ति-सम्पन्न है। उनकी बुद्धि का मुकाबला
करने के लिए हमें अपनी बुद्धि का विकास करना होगा। इसके लिए चार कार्य साथ-साथ
जरूरी हैं- वर्ग संघर्ष, उत्पादन
संघर्ष, वैज्ञानिक प्रयोग और
इतिहास का अध्ययन। हमारी शक्ति के विकास के लिए हमें व्यापक जनता को जगाने का काम
लगातार करना होगा।
आज का ट्रेड यूनियन आंदोलन केवल इस पद्धति का उपयोग
ही नहीं करता, बल्कि
उसे ये बातें नापसंद भी हैं
ही नहीं करता, बल्कि
उसे ये बातें नापसंद भी हैं
4. हमारे जैसे पिछड़े हुए देश में पूंजीपति वर्ग मजदूरों को
ट्रेड यूनियन का अधिकार इन कारणों से देता है-
ट्रेड यूनियन का अधिकार इन कारणों से देता है-
क. दमन और शोषण से त्रसत मजदूरों द्वारा अचानक बगावत
करने की आशंका को निर्मूल करने के लिए;
करने की आशंका को निर्मूल करने के लिए;
ख. उद्योगों में मालिक वर्ग द्वारा तय अनुशासन के
दमन-मूलक नियमों व हर प्रकार के कानूनी बंधनों को ट्रेड यूनियन नेताओं के माध्यम
से मजदूरों से स्वेच्छापूर्वक मनवाने के लिए;
दमन-मूलक नियमों व हर प्रकार के कानूनी बंधनों को ट्रेड यूनियन नेताओं के माध्यम
से मजदूरों से स्वेच्छापूर्वक मनवाने के लिए;
ग. सिर्फ आर्थिक संघर्ष के लिए मजदूरों को
प्रोत्साहित करके मजदूरों की सोच को उसके उद्योग तक ही सीमित रखने के लिए; एवं
प्रोत्साहित करके मजदूरों की सोच को उसके उद्योग तक ही सीमित रखने के लिए; एवं
घ. सह-अस्तित्व की नीति को सभी स्तरों पर प्रचारित और
प्रतिष्ठित करने के लिए। आज भारत की केंद्रीय ट्रेड यूनियनें मालिक वर्ग के इन्हीं
उद्देश्यों को पूरा करने में लगी हुई हैं।
प्रतिष्ठित करने के लिए। आज भारत की केंद्रीय ट्रेड यूनियनें मालिक वर्ग के इन्हीं
उद्देश्यों को पूरा करने में लगी हुई हैं।
5. विभिन्न राष्ट्रीयताओंवाले हमारे देश में नौकरी की
भर्ती नीति भी ट्रेड यूनियनों के मजबूत नहीं होने का एक प्रमुख कारण है।
भर्ती नीति भी ट्रेड यूनियनों के मजबूत नहीं होने का एक प्रमुख कारण है।
अंग्रेज साम्राज्यवादियों ने सन् 1971 की अक्तूबर
क्रांति से उपयोगी शिक्षा हासिल की थी। उद्योग में उनकी भर्ती की नीति भी भारत में
इस प्रकार की क्रांति की संभावनाओं पर रोक लगाने के लिए तय की गयी थी। कहीं
सर्वहारा के नेतृत्व में भारत में जनवादी लोकतांत्रिक क्रांति सम्पन्न न हो जायें, इसके लिए उन्होंने काफी दूरदर्शिता
दिखायी। किसी खास क्षेत्र में स्थित उद्योगों में उस क्षेत्र के लोगों को भर्ती न
करके अन्य क्षेत्रों के लोगों को भर्ती किया गया। मध्य प्रदेश व झारखंड की कोयला
खानों में ‘सेंट्रल रिक्रूटमेंट आफिस’ के माध्यम से गोरखपुरी
मजदूरों को भर्ती किया गया। असम और बंगाल के चाय बागानों में छत्तीसगढ़ी और
झारखंडी मजदूरों को भर्ती किया गया। झारखंड और बंगाल की कोयला खदानों में
छत्तीसगढ़ी और गोरखपुरी मजदूरों को भर्ती किया गया।
क्रांति से उपयोगी शिक्षा हासिल की थी। उद्योग में उनकी भर्ती की नीति भी भारत में
इस प्रकार की क्रांति की संभावनाओं पर रोक लगाने के लिए तय की गयी थी। कहीं
सर्वहारा के नेतृत्व में भारत में जनवादी लोकतांत्रिक क्रांति सम्पन्न न हो जायें, इसके लिए उन्होंने काफी दूरदर्शिता
दिखायी। किसी खास क्षेत्र में स्थित उद्योगों में उस क्षेत्र के लोगों को भर्ती न
करके अन्य क्षेत्रों के लोगों को भर्ती किया गया। मध्य प्रदेश व झारखंड की कोयला
खानों में ‘सेंट्रल रिक्रूटमेंट आफिस’ के माध्यम से गोरखपुरी
मजदूरों को भर्ती किया गया। असम और बंगाल के चाय बागानों में छत्तीसगढ़ी और
झारखंडी मजदूरों को भर्ती किया गया। झारखंड और बंगाल की कोयला खदानों में
छत्तीसगढ़ी और गोरखपुरी मजदूरों को भर्ती किया गया।
क्षेत्रीय विकास में क्षेत्रीय जनता की भागीदारी ही
राष्ट्रीय विकास की गारंटी है। क्षेत्रीय विकास में बाहर से आये हुए मजदूर
दिलचस्पी नहीं लेते क्येांकि
उनकी राष्ट्रीयता, संस्कृति
तथा आर्थिक पृष्ठभूमि अलग होती है। इस तरह चूंकि उद्योगों में अधिकांश मजदूर बाहरी
क्षेत्रों से आये हुए हैं, इसलिए
मजदूर वर्ग क्षेत्रीय विकास की मुख्य धारा से कट जाते हैं, नेतृत्व देना तो दूर की बात। चूंकि इन
मजदूरों की आर्थिक-सामाजिक जड़ें कहीं और हैं, इसलिए वे स्थानीय
विकास के मुद्दों से जुड़ नहीं पाते। नतीजा होता है एक बहुत ही असंतुलित और विकृत विकास।
राष्ट्रीय विकास की गारंटी है। क्षेत्रीय विकास में बाहर से आये हुए मजदूर
दिलचस्पी नहीं लेते क्येांकि
उनकी राष्ट्रीयता, संस्कृति
तथा आर्थिक पृष्ठभूमि अलग होती है। इस तरह चूंकि उद्योगों में अधिकांश मजदूर बाहरी
क्षेत्रों से आये हुए हैं, इसलिए
मजदूर वर्ग क्षेत्रीय विकास की मुख्य धारा से कट जाते हैं, नेतृत्व देना तो दूर की बात। चूंकि इन
मजदूरों की आर्थिक-सामाजिक जड़ें कहीं और हैं, इसलिए वे स्थानीय
विकास के मुद्दों से जुड़ नहीं पाते। नतीजा होता है एक बहुत ही असंतुलित और विकृत विकास।
भारत के विभिन्न उद्योग-कारखानों में गोरे अंग्रेजों
के इस तरीके को काले अंग्रेजों ने पूरी वफादारी के साथ अपनाया है। भिलाई के 90
प्रतिशत मजदूर दूसरे क्षेत्रों से आये हुए हैं। बोकारो में दक्षिण बिहार से आये
मजदूरों की संख्या 20 प्रतिशत से अधिक है। दुर्गापुर इस्पात कारखाने में स्थानीय
लोगों की कमी ने ही वहां के ग्रामांचल में झारखंड की आवाज को जोरदार किया है। टाटा
के कारखानों में भी आपको बहुत ही कम झारखंडी मिलेंगे।
के इस तरीके को काले अंग्रेजों ने पूरी वफादारी के साथ अपनाया है। भिलाई के 90
प्रतिशत मजदूर दूसरे क्षेत्रों से आये हुए हैं। बोकारो में दक्षिण बिहार से आये
मजदूरों की संख्या 20 प्रतिशत से अधिक है। दुर्गापुर इस्पात कारखाने में स्थानीय
लोगों की कमी ने ही वहां के ग्रामांचल में झारखंड की आवाज को जोरदार किया है। टाटा
के कारखानों में भी आपको बहुत ही कम झारखंडी मिलेंगे।
एक तरफ तमाम सुविधाओं से भरपूर इस्पात नगरी, मानो एक गमले में
सुंदर सा गुलाब का पौधा है, वहीं
दूसरी तरफ घोर दरिद्रता के अंधकार में डूबे हुए गांव। एक ओर अधिक वेतन पानेवाले
संगठित मजदूर और दूसरी ओर गांव में भुखमरी के शिकार खेतिहर मजदूर, गरीब किसान और बेरोजगारों की फौज। इसी
प्रक्रिया से शासक वर्ग मजदूरों को दो टुकड़ों में बांटता है। अफसर और मैनेजमेंट
के लोग करीब-करीब सभी बाहर के होते हैं। वे क्षेत्रीय विकास में कोई दिलचस्पी तो
लेते ही नहीं, बल्कि
वे जान-बूझकर क्षेत्र की प्रगति के लिए जरूरी संसाधनों का बरबाद कर देते हैं।
सुंदर सा गुलाब का पौधा है, वहीं
दूसरी तरफ घोर दरिद्रता के अंधकार में डूबे हुए गांव। एक ओर अधिक वेतन पानेवाले
संगठित मजदूर और दूसरी ओर गांव में भुखमरी के शिकार खेतिहर मजदूर, गरीब किसान और बेरोजगारों की फौज। इसी
प्रक्रिया से शासक वर्ग मजदूरों को दो टुकड़ों में बांटता है। अफसर और मैनेजमेंट
के लोग करीब-करीब सभी बाहर के होते हैं। वे क्षेत्रीय विकास में कोई दिलचस्पी तो
लेते ही नहीं, बल्कि
वे जान-बूझकर क्षेत्र की प्रगति के लिए जरूरी संसाधनों का बरबाद कर देते हैं।
6. ट्रेड यूनियनों के कार्यक्रम भी अन्य राजनैतिक
सिद्धातों की तरह वैचारिक दिवालियपन के शिकार हैं। ट्रेड यूनियन मजदूरों का संगठन
होता है। मजदूर वर्ग का वैज्ञानिक सिद्धांत उनको उस नये प्रकार की राजसत्ता कायम
करने के लिए प्रेरित करता है, जो वर्तमान व्यवस्था
की कब्र पर खड़ी की गयी हो। यह सिद्धांत पुराने को तोड़ने और नये का निर्माण करने
का राजनैतिक सिद्धांत है। ट्रेड यूनियनों से उम्मीद की जाती है कि वे इसी सिद्धांत
की रोशनी में काम करेंगी। परंतु वर्तमान व्यवस्था ऐसी ट्रेड यूनियन को स्वीकार
नहीं कर सकती, जो उसी की कब्र खोदे।
जब वर्तमान व्यवस्था पायेगी कि ट्रेड यूनियन का व्यवहार उसके खिलाफ है तो वह ट्रेड
यूनियन कानून को ही समाप्त कर देगी। ट्रेड यूनियन रहेगी या नहीं रहेगी, वह इस बात पर निर्भर करेगा कि ट्रेड
यूनियन ने समाज की सबसे प्रतिक्रियावादी, घृणित शक्ति को अपना
दुश्मन करार देकर बाकी वर्गों के साथ तालमेल का नया सैद्धांतिक आधार बनाया या नहीं; प्रतिक्रियावादियों के आपसी द्वंद्व को
तेज करने में मदद कर और एक लचीली कार्य पद्धति पर अमल करते हुए हर मामलों में अगुआ
भूमिका स्वीकार की या नहीं; बुनियादी सामाजिक
परिवर्तन के लिए मजदूर वर्ग को जागरूक किया या नहीं।
सिद्धातों की तरह वैचारिक दिवालियपन के शिकार हैं। ट्रेड यूनियन मजदूरों का संगठन
होता है। मजदूर वर्ग का वैज्ञानिक सिद्धांत उनको उस नये प्रकार की राजसत्ता कायम
करने के लिए प्रेरित करता है, जो वर्तमान व्यवस्था
की कब्र पर खड़ी की गयी हो। यह सिद्धांत पुराने को तोड़ने और नये का निर्माण करने
का राजनैतिक सिद्धांत है। ट्रेड यूनियनों से उम्मीद की जाती है कि वे इसी सिद्धांत
की रोशनी में काम करेंगी। परंतु वर्तमान व्यवस्था ऐसी ट्रेड यूनियन को स्वीकार
नहीं कर सकती, जो उसी की कब्र खोदे।
जब वर्तमान व्यवस्था पायेगी कि ट्रेड यूनियन का व्यवहार उसके खिलाफ है तो वह ट्रेड
यूनियन कानून को ही समाप्त कर देगी। ट्रेड यूनियन रहेगी या नहीं रहेगी, वह इस बात पर निर्भर करेगा कि ट्रेड
यूनियन ने समाज की सबसे प्रतिक्रियावादी, घृणित शक्ति को अपना
दुश्मन करार देकर बाकी वर्गों के साथ तालमेल का नया सैद्धांतिक आधार बनाया या नहीं; प्रतिक्रियावादियों के आपसी द्वंद्व को
तेज करने में मदद कर और एक लचीली कार्य पद्धति पर अमल करते हुए हर मामलों में अगुआ
भूमिका स्वीकार की या नहीं; बुनियादी सामाजिक
परिवर्तन के लिए मजदूर वर्ग को जागरूक किया या नहीं।
आज की केंद्रीय ट्रेड यूनियनें इस दिशा में किसी भी
प्रकार की नीति अपनाने के बदले, सरकार और मैनेजमेंट की मदद से ट्रेड
यूनियन नाम की दुकानदारी चला रही हैं। चाहे बाहरी रूप कुछ हो, सभी केंद्रीय ट्रेड यूनियनें दलालों की
चैम्पियनशिप हासिल करने की होड़ में लगी हुई हैं।
प्रकार की नीति अपनाने के बदले, सरकार और मैनेजमेंट की मदद से ट्रेड
यूनियन नाम की दुकानदारी चला रही हैं। चाहे बाहरी रूप कुछ हो, सभी केंद्रीय ट्रेड यूनियनें दलालों की
चैम्पियनशिप हासिल करने की होड़ में लगी हुई हैं।
7. राजनैतिक ‘पंडितों’ की स्वेच्छाचारिता के
कारण भी ट्रेड यूनियन आंदोलन सही ढंग से विकसित नहीं हो पाया है। अंग्रेजों के
जमाने में ‘एटक’ यूनियन के कम्युनिस्ट
हिस्से ने समाजवादी क्रांति की आवाज बुलंद करके, उग्रवादी लाइन चलाकर
मजदूर आंदोलन का सर्वनाश किया (शोलापुर का इतिहास उल्लेखनीय है)। 1946-47 में भी
वी.टी. रणदिवे ने समाजवादी क्रांति कहकर तेलंगाना आंदोलन को गुमराह किया। एटक
यूनियन का कांग्रेसी हिस्सा उधर उद्योगों में संघर्ष पनपने न देकर मालिक वर्ग की
तरफदारी करता रहा। यही हिस्सा स्वतंत्रता के बाद इंटक यूनियन बनकर सरकारी ट्रेड यूनियन
के रूप में सामने आया। आज कम्युनिस्ट पार्टियों की यूनियनें इंटक ही ‘दिलदार’ भावना से ओत-प्रोत हो
चुकी है। चारू मजूमदार के नेतृत्व में नक्सलवादी संघर्ष ने मजदूर वर्ग में नयी आशा
का संचार किया था, लेकिन
उन्होंने भी बाद में ट्रेड यूनियन में संशोधनवादी नेतृत्व के खिलाफ संघर्ष न कर ‘ट्रेड यूनियन छोड़ दो’ के पलायनवादी सिद्धांत की प्रतिष्ठा की।
कारण भी ट्रेड यूनियन आंदोलन सही ढंग से विकसित नहीं हो पाया है। अंग्रेजों के
जमाने में ‘एटक’ यूनियन के कम्युनिस्ट
हिस्से ने समाजवादी क्रांति की आवाज बुलंद करके, उग्रवादी लाइन चलाकर
मजदूर आंदोलन का सर्वनाश किया (शोलापुर का इतिहास उल्लेखनीय है)। 1946-47 में भी
वी.टी. रणदिवे ने समाजवादी क्रांति कहकर तेलंगाना आंदोलन को गुमराह किया। एटक
यूनियन का कांग्रेसी हिस्सा उधर उद्योगों में संघर्ष पनपने न देकर मालिक वर्ग की
तरफदारी करता रहा। यही हिस्सा स्वतंत्रता के बाद इंटक यूनियन बनकर सरकारी ट्रेड यूनियन
के रूप में सामने आया। आज कम्युनिस्ट पार्टियों की यूनियनें इंटक ही ‘दिलदार’ भावना से ओत-प्रोत हो
चुकी है। चारू मजूमदार के नेतृत्व में नक्सलवादी संघर्ष ने मजदूर वर्ग में नयी आशा
का संचार किया था, लेकिन
उन्होंने भी बाद में ट्रेड यूनियन में संशोधनवादी नेतृत्व के खिलाफ संघर्ष न कर ‘ट्रेड यूनियन छोड़ दो’ के पलायनवादी सिद्धांत की प्रतिष्ठा की।
इन स्वेच्छाचारी राजनैतिक पंडिजों की कृपा से ट्रेड
यूनियनें भारत की मेहनतकश जनता की इच्छा के मुताबिक अपने को कभी नहीं ढाल पायीं।
जो आया वह पछताया और जो नहीं आया वह भी पछताया। आज भी हरेक ट्रेड यूनियन के
सदस्य-मजदूर अपने व्यक्तिगत हित और अपने उद्योग के मजदूरों के हित को देश की तमाम
जनता के हितों के साथ मिलाकर यानी साधारण को विशेष के साथ जोड़ कर नहीं देख पाते।
पश्चिम बंगाल के कारखानों में यह कहावत प्रचलित है ‘वोट के लिए तरंगा झंडा, पेट के लिए लाल झंडा।’ इसी सिलसिले में उनकी
नयी उपलब्धि है ‘चोट के लिए सगा भाई’।
यूनियनें भारत की मेहनतकश जनता की इच्छा के मुताबिक अपने को कभी नहीं ढाल पायीं।
जो आया वह पछताया और जो नहीं आया वह भी पछताया। आज भी हरेक ट्रेड यूनियन के
सदस्य-मजदूर अपने व्यक्तिगत हित और अपने उद्योग के मजदूरों के हित को देश की तमाम
जनता के हितों के साथ मिलाकर यानी साधारण को विशेष के साथ जोड़ कर नहीं देख पाते।
पश्चिम बंगाल के कारखानों में यह कहावत प्रचलित है ‘वोट के लिए तरंगा झंडा, पेट के लिए लाल झंडा।’ इसी सिलसिले में उनकी
नयी उपलब्धि है ‘चोट के लिए सगा भाई’।
भारत की ट्रेड यूनियनें राजनैतिक पार्टियों पर अपना
प्रभाव तो डाल नहीं पायी हैं, बल्कि निराशाग्रस्त नेताओं ने ट्रेड
यूनियनों पर हावी होकर सारे मजदूर आंदेालन को भंवरजाल में फंसा दिया है।
प्रभाव तो डाल नहीं पायी हैं, बल्कि निराशाग्रस्त नेताओं ने ट्रेड
यूनियनों पर हावी होकर सारे मजदूर आंदेालन को भंवरजाल में फंसा दिया है।
8. ट्रेड यूनियन मजदूर वर्ग का हथियार है। ठोस ढंग से
इस हथियार का उपयेाग करने की विधि है- जनवादी केंद्रीयता। संघर्ष का निर्णय, रणनीति और संगठन से
संबंधित मामलों में फैसला जनवादी तरीके से करना चाहिए एवं इन फैसलों को केंद्रीयता
के मातहत लागू करना चाहिए। कभी-कभी भारी संख्या में मौजूद या दूर-दूर तक छितराये
हुए मजदूरों में सामान्य ढंग से इस विधि का उपयोग करने में दिक्कत आती है। इस
स्थिति में विभिन्न इकाइयों में व्यापक चर्चा चलाकर और ‘जनता से, जनता को’ के सिद्धांत को लागू करके, जनता की विस्तृत भागीदारी और मुद्दों के
प्रति उसकी समझ व चेतना को सही निर्णय-प्रक्रिया का आधार बनाया जा सकता है।
इस हथियार का उपयेाग करने की विधि है- जनवादी केंद्रीयता। संघर्ष का निर्णय, रणनीति और संगठन से
संबंधित मामलों में फैसला जनवादी तरीके से करना चाहिए एवं इन फैसलों को केंद्रीयता
के मातहत लागू करना चाहिए। कभी-कभी भारी संख्या में मौजूद या दूर-दूर तक छितराये
हुए मजदूरों में सामान्य ढंग से इस विधि का उपयोग करने में दिक्कत आती है। इस
स्थिति में विभिन्न इकाइयों में व्यापक चर्चा चलाकर और ‘जनता से, जनता को’ के सिद्धांत को लागू करके, जनता की विस्तृत भागीदारी और मुद्दों के
प्रति उसकी समझ व चेतना को सही निर्णय-प्रक्रिया का आधार बनाया जा सकता है।
आज की तमाम केंद्रीय ट्रेड यूनियनें इस पद्धति का
उपयोग नहीं करती हैं। वहां निर्णय ऊपर से थोप दिया जाता है। वास्तविक समस्या, मजदूर वर्ग की विचारधारा, अत्याचारी ताकतों
द्वारा निर्दयतापूर्वक दमन आदि के विषय में नेतृत्व लापरवाह रहता है। ये
यूनियनवाले श्रम कानून पर, श्रम
कानून लागू करनेवाली शोषक वर्गों की मशीनरी एवं कानूनी व्यवस्था के मसलों की
जरूरतों पर अधिक ध्यान देते हैं। ये लोग इन मामलों में मजदूर वर्ग की अज्ञानता और
निस्पृहता का लाभ उठाकर नौकरशाही यानी सिर्फ केंद्रीयता की पद्धति से तमाम मामलों
का निराकरण या निपटारा करते हैं। इसी प्रकार आज की ट्रेड यूनियनें एक भयावह स्थिति
पैदा कर चुकी हैं। इससे ट्रेड यूनियनों को बनाये रखने की पूंजीपतियों की जरूरतें
तक पूरी नहीं हो रही हैं, मेहनतकशों के हथियार
के रूप में ट्रेड यूनियन का इस्तेमाल करना तो दूर की बात है।
उपयोग नहीं करती हैं। वहां निर्णय ऊपर से थोप दिया जाता है। वास्तविक समस्या, मजदूर वर्ग की विचारधारा, अत्याचारी ताकतों
द्वारा निर्दयतापूर्वक दमन आदि के विषय में नेतृत्व लापरवाह रहता है। ये
यूनियनवाले श्रम कानून पर, श्रम
कानून लागू करनेवाली शोषक वर्गों की मशीनरी एवं कानूनी व्यवस्था के मसलों की
जरूरतों पर अधिक ध्यान देते हैं। ये लोग इन मामलों में मजदूर वर्ग की अज्ञानता और
निस्पृहता का लाभ उठाकर नौकरशाही यानी सिर्फ केंद्रीयता की पद्धति से तमाम मामलों
का निराकरण या निपटारा करते हैं। इसी प्रकार आज की ट्रेड यूनियनें एक भयावह स्थिति
पैदा कर चुकी हैं। इससे ट्रेड यूनियनों को बनाये रखने की पूंजीपतियों की जरूरतें
तक पूरी नहीं हो रही हैं, मेहनतकशों के हथियार
के रूप में ट्रेड यूनियन का इस्तेमाल करना तो दूर की बात है।
फलस्वरूप, मजदूरों पर ट्रेड
यूनियन का कोई प्रभाव नहीं रहता हैं। मजदूर ट्रेड यूनियन के सदस्य नहीं बनते और न
ही सदस्यता शुल्क देते हैं। काल्पनिक नामों से सदस्यता रजिस्टर भरे रहते हैं।
मजदूर हंसता है कि उसने विभिन्न यूनियनों को बेवकूफ बना दिया और यूनियनवाले हंसते
हैं कि मजदूर बेवकूफ बन गया। पूंजीपति इन दोनों की बेवकूफी पर हंसता है और खुद को
अधिक सुरक्षित महसूस करता है। मजदूरों की मामूली से मामूली समस्या का निपटारा भी
ठेके में होता है। इस नौकरशाही या अति-केंद्रीय तरीकों के चलते मालिक का उद्देश्य
पूरा न होने पर भी वह खुश रहता है। मालिक या मैनेजमेंट मजदूरों में से 10-20
प्रतिशत ‘लायक’ मजदूरों को छांट लेता
है और उनको प्रमोशन, ओवर-टाइम, ‘कामचोरी की छूट’ या अन्य सुविधाएं देकर
अपना समर्थक गुट बना लेता है। इस गुट के लोग हर यूनियन में घुसपैठ करते रहते हैं।
ऐसे उद्योग में मजदूरों का जीवन गुलाम से भी बदतर होता है, तानाशाही दमन का तरीका
जारी रहता है। उधर मालिक के पैर चाटनेवाले कुत्ते अपने गले में लगे बेल्ट को
फूलमाला मानकर अपने को गौरवान्वित महसूस करते रहते हैं।
यूनियन का कोई प्रभाव नहीं रहता हैं। मजदूर ट्रेड यूनियन के सदस्य नहीं बनते और न
ही सदस्यता शुल्क देते हैं। काल्पनिक नामों से सदस्यता रजिस्टर भरे रहते हैं।
मजदूर हंसता है कि उसने विभिन्न यूनियनों को बेवकूफ बना दिया और यूनियनवाले हंसते
हैं कि मजदूर बेवकूफ बन गया। पूंजीपति इन दोनों की बेवकूफी पर हंसता है और खुद को
अधिक सुरक्षित महसूस करता है। मजदूरों की मामूली से मामूली समस्या का निपटारा भी
ठेके में होता है। इस नौकरशाही या अति-केंद्रीय तरीकों के चलते मालिक का उद्देश्य
पूरा न होने पर भी वह खुश रहता है। मालिक या मैनेजमेंट मजदूरों में से 10-20
प्रतिशत ‘लायक’ मजदूरों को छांट लेता
है और उनको प्रमोशन, ओवर-टाइम, ‘कामचोरी की छूट’ या अन्य सुविधाएं देकर
अपना समर्थक गुट बना लेता है। इस गुट के लोग हर यूनियन में घुसपैठ करते रहते हैं।
ऐसे उद्योग में मजदूरों का जीवन गुलाम से भी बदतर होता है, तानाशाही दमन का तरीका
जारी रहता है। उधर मालिक के पैर चाटनेवाले कुत्ते अपने गले में लगे बेल्ट को
फूलमाला मानकर अपने को गौरवान्वित महसूस करते रहते हैं।
नौकरशाही या सिर्फ केंद्रीयता की पद्धति के साथ-साथ
एक और भी कार्यशैली है जिसका खतरा नजर आता है। यह कार्यशैली है –
ट्राट्स्कीवादियों का पथ। यह सिर्फ जनवादी प्रक्रिया को जरूरत से अधिक महत्व देने
का पथ है। हालांकि यह पद्धति भी जनवादी प्रक्रिया को सिर्फ छोटे-मोटे मसलों में ही
लागू करती है। रणनीति तो मानो किसी अदृश्य स्थान से आ धमकती है। प्रश्न उठने पर
संगठन के बड़े आकार का बहाना लेकर इसकी बात टाल दी जाती है। अंततः कार्य पद्धति
में जो भी जनवादी प्रक्रिया का इस्तेमाल होता है उससे ‘जन’ गायब हो जाता है, और केवल ‘वाद’ बचा रहता है। फिर ‘वाद’ को लेकर विवाद पैदा
होता है। जितने सिर, उतने
ही मत और उतने की पथ। इस प्रकार बहु-केंद्रीयता से संगठन का शरीर कैंसर की बीमारी
का घर बन जाता है। आज की कई सोशलिस्ट ट्रेड यूनियनों की ऐसी ही दयनीय स्थिति हो
गयी है। हालांकि इस प्रकार की ट्रेड यूनियनों को पूंजीपति अधिक महत्व देते हैं, लेकिन मजदूर वर्ग की
एकता की भावना का फायदा उठाते हुए नौकरशाहीवाले ट्रेड यूनियन अधिक कामयाब रहते
हैं।
एक और भी कार्यशैली है जिसका खतरा नजर आता है। यह कार्यशैली है –
ट्राट्स्कीवादियों का पथ। यह सिर्फ जनवादी प्रक्रिया को जरूरत से अधिक महत्व देने
का पथ है। हालांकि यह पद्धति भी जनवादी प्रक्रिया को सिर्फ छोटे-मोटे मसलों में ही
लागू करती है। रणनीति तो मानो किसी अदृश्य स्थान से आ धमकती है। प्रश्न उठने पर
संगठन के बड़े आकार का बहाना लेकर इसकी बात टाल दी जाती है। अंततः कार्य पद्धति
में जो भी जनवादी प्रक्रिया का इस्तेमाल होता है उससे ‘जन’ गायब हो जाता है, और केवल ‘वाद’ बचा रहता है। फिर ‘वाद’ को लेकर विवाद पैदा
होता है। जितने सिर, उतने
ही मत और उतने की पथ। इस प्रकार बहु-केंद्रीयता से संगठन का शरीर कैंसर की बीमारी
का घर बन जाता है। आज की कई सोशलिस्ट ट्रेड यूनियनों की ऐसी ही दयनीय स्थिति हो
गयी है। हालांकि इस प्रकार की ट्रेड यूनियनों को पूंजीपति अधिक महत्व देते हैं, लेकिन मजदूर वर्ग की
एकता की भावना का फायदा उठाते हुए नौकरशाहीवाले ट्रेड यूनियन अधिक कामयाब रहते
हैं।
मात्र जनवाद केंद्रीयता ही सही पद्धति हो सकती है।
9. मजदूर वर्ग की सही राजनैतिक पार्टी के अभाव में
तथा सही ट्रेड यूनियन के नहीं रहने से आज ‘नेता’ शब्द अपनी इज्जत-आबरू
खो बैठा है। स्वार्थी, अनैतिक
और उच्छृंखल जीवन जीनेवाले असामाजिक तत्वों के झुंड माइक पर लम्बी-चौड़ी हांकने
में माहिर होते हैं, दरोगा साहब से दोस्ती
गांठते हैं, पद रूपी सिंहासन पर
कब्जा चाहते हैं, देश व प्रांत की
राजधानियों में नियमित सम्पर्क साधते हैं और आम जनता को आश्वासनों के भंवरजाल में
घुमाते रहते हैं- ऐसे व्यक्ति ‘नेता’ कहलाते हैं। ऐसे नेताओं से जनता
दिलोदिमाग से नफरत करती है।
तथा सही ट्रेड यूनियन के नहीं रहने से आज ‘नेता’ शब्द अपनी इज्जत-आबरू
खो बैठा है। स्वार्थी, अनैतिक
और उच्छृंखल जीवन जीनेवाले असामाजिक तत्वों के झुंड माइक पर लम्बी-चौड़ी हांकने
में माहिर होते हैं, दरोगा साहब से दोस्ती
गांठते हैं, पद रूपी सिंहासन पर
कब्जा चाहते हैं, देश व प्रांत की
राजधानियों में नियमित सम्पर्क साधते हैं और आम जनता को आश्वासनों के भंवरजाल में
घुमाते रहते हैं- ऐसे व्यक्ति ‘नेता’ कहलाते हैं। ऐसे नेताओं से जनता
दिलोदिमाग से नफरत करती है।
एक और प्रकार के नेता होते हैं। ये मार्क्स और लेनिन
की किताबों के नाम जानते हैं, और समय-समय पर उन नामों को उद्धृत करते
हुए अपनी विद्वता को जाहिर करते रहते हैं। ये लोग अर्जी-अपील लिखने में माहिर होते
हैं। ये उत्पादन से विमुख रहते हैं। ये लोग घरेलू झगड़ों की व्याख्या भी
अंतर्राष्ट्रीय और ऐतिहासिक महत्व की घटनाओं की रोशनी में करने की कोशिश करते हैं।
वे ज्यादा माला-माल नहीं होते, फिर भी रंगीन जिंदगी
जीने के शौकीन होते हैं। मजदूर इन नेताओं का विश्वास नहीं करते, ये नेता मजदूरों का विश्वास नहीं करते।
ऐसे ही नेताओं से सुशोभित ट्रेड यूनियनों ने मजदूरों के जीवन को दूभर बना दिया है।
की किताबों के नाम जानते हैं, और समय-समय पर उन नामों को उद्धृत करते
हुए अपनी विद्वता को जाहिर करते रहते हैं। ये लोग अर्जी-अपील लिखने में माहिर होते
हैं। ये उत्पादन से विमुख रहते हैं। ये लोग घरेलू झगड़ों की व्याख्या भी
अंतर्राष्ट्रीय और ऐतिहासिक महत्व की घटनाओं की रोशनी में करने की कोशिश करते हैं।
वे ज्यादा माला-माल नहीं होते, फिर भी रंगीन जिंदगी
जीने के शौकीन होते हैं। मजदूर इन नेताओं का विश्वास नहीं करते, ये नेता मजदूरों का विश्वास नहीं करते।
ऐसे ही नेताओं से सुशोभित ट्रेड यूनियनों ने मजदूरों के जीवन को दूभर बना दिया है।
संगठन हो या आंदोलन,
नेतृत्व
का सवाल एक महत्वपूर्ण सवाल है। एक साधारण व्यक्ति के गलत विचारों या कार्यों से
अधिक लोगो को नुकसान नहीं होता, परंतु नेतृत्व के गलत
विचारों और कार्यों से लाखों-करोड़ों की जिंदगियां बुरी तरह प्रभावित होती हैं।
इसीलिए नेतृत्व के बारे में सही जानकारी होना जरूरी है।
नेतृत्व
का सवाल एक महत्वपूर्ण सवाल है। एक साधारण व्यक्ति के गलत विचारों या कार्यों से
अधिक लोगो को नुकसान नहीं होता, परंतु नेतृत्व के गलत
विचारों और कार्यों से लाखों-करोड़ों की जिंदगियां बुरी तरह प्रभावित होती हैं।
इसीलिए नेतृत्व के बारे में सही जानकारी होना जरूरी है।
नेतृत्व को अपने वर्ग का सबसे अधिक वर्ग-चेतना से
भरपूर अंश होना चाहिए। यह बात पूंजीपति वर्ग पर भी उतनी ही लागू होती है जितनी
मजदूर वर्ग पर।
भरपूर अंश होना चाहिए। यह बात पूंजीपति वर्ग पर भी उतनी ही लागू होती है जितनी
मजदूर वर्ग पर।
सबसे अधिक वर्ग-चेतना से भरपूर होने के तरीके का
जिक्र पहले ही किया गया है। यह चार-सूत्री तरीका है- वर्ग संघर्ष, उत्पादन संघर्ष, वैज्ञानिक प्रयोग और
इतिहास का अध्ययन। वर्तमान व्यवस्था के अंतर्गत ट्रेड यूनियनों में बिना वर्ग
संघर्ष के भी नेतागिरी चलती है। लेकिन अगर इस व्यवस्था के खिलाफ संघर्ष करना हे तो
अवश्य ही सामंतवादी-पूंजीवादी और प्रतिक्रियावादी शक्तियों के खिलाफ संघर्ष में
नेतृत्व को खुद भी बहादुरी के साथ भाग लेना होगा। अक्सर देखा जाता है कि जब जनता
आंदोलन करती है तब नेतृत्व चुपचाप मुंह छिपाकर भाग जाता है। जो आदमी कर्फ्यू और
144 धारा लगने पर सिर के बाल नोचता है, वही स्थिति शांत होने
पर नेता बन जाता है। इससे मजदूर आंदोलन पूंजीपतियों की राह पर चलने लगता है।
जिक्र पहले ही किया गया है। यह चार-सूत्री तरीका है- वर्ग संघर्ष, उत्पादन संघर्ष, वैज्ञानिक प्रयोग और
इतिहास का अध्ययन। वर्तमान व्यवस्था के अंतर्गत ट्रेड यूनियनों में बिना वर्ग
संघर्ष के भी नेतागिरी चलती है। लेकिन अगर इस व्यवस्था के खिलाफ संघर्ष करना हे तो
अवश्य ही सामंतवादी-पूंजीवादी और प्रतिक्रियावादी शक्तियों के खिलाफ संघर्ष में
नेतृत्व को खुद भी बहादुरी के साथ भाग लेना होगा। अक्सर देखा जाता है कि जब जनता
आंदोलन करती है तब नेतृत्व चुपचाप मुंह छिपाकर भाग जाता है। जो आदमी कर्फ्यू और
144 धारा लगने पर सिर के बाल नोचता है, वही स्थिति शांत होने
पर नेता बन जाता है। इससे मजदूर आंदोलन पूंजीपतियों की राह पर चलने लगता है।
वर्ग संघर्ष में निडरता से भाग लेना सही नेतृत्व की
पहली कौसटी है। दूसरी कसौटी है उत्पादन संघर्ष। ऐसे कामचोर जिनको उत्पादन के काम
में कोई दिलचस्पी नहीं, वह
नेतृत्व के लायक नहीं है। दीवाली के पहले घर में मकड़ी के जालों की सफाई करने की
तरह मजदूर वर्ग को अपने ट्रेड यूनियन रूपी घर से ऐसे उत्पादन-विमुख नेताओं का
सफाया कर देना चाहिए।
पहली कौसटी है। दूसरी कसौटी है उत्पादन संघर्ष। ऐसे कामचोर जिनको उत्पादन के काम
में कोई दिलचस्पी नहीं, वह
नेतृत्व के लायक नहीं है। दीवाली के पहले घर में मकड़ी के जालों की सफाई करने की
तरह मजदूर वर्ग को अपने ट्रेड यूनियन रूपी घर से ऐसे उत्पादन-विमुख नेताओं का
सफाया कर देना चाहिए।
नेतृत्व तभी सही नीति का निर्धारण और कार्य पद्धति का
उपयोग कर सकेगा, जब
वह साधारण परिस्थिति को विशेष परिस्थिति के साथ जोड़ सके। अगर हड़ताल करना हे तो
नेतृत्व को यह समझ होनी चाहिए कि मुख्य मुद्दा क्या होगा हड़ताल का यह उचित समय है
या नहीं। अगर नेतृत्व इस पर सही निर्णय नहीं ले सकता तो आंदोलन में मार खाने की
पूरी गुंजाइश रह जायेगी। साधारण परिस्थिति की जानकारी, वैज्ञानिक प्रयोग और
इतिहास की जानकारी के जरिये ही हो सकती है। सफल नेतृत्व की कसौटी है, साधारण परिस्थिति की पूर्ण जानकारी और
विशेष परिस्थिति में उस जानकारी को लागू करने की क्षमता। नेतृत्व की व्यक्तिगत तौर
पर महत्वाकांक्षी नहीं होना चाहिए। ईमानदारी और कुर्बानी, नेतृत्व के साथ
श्वास-निःश्वास की तरह जुड़े हुए गुण होने चाहिए। तभी वह नेतृत्व लोकप्रिय हो सकता
है और उस नेतृत्व पर भरोसा करके लाखों लोग जान हथेली पर रखकर संघर्ष में कूद
जायेंगे।
उपयोग कर सकेगा, जब
वह साधारण परिस्थिति को विशेष परिस्थिति के साथ जोड़ सके। अगर हड़ताल करना हे तो
नेतृत्व को यह समझ होनी चाहिए कि मुख्य मुद्दा क्या होगा हड़ताल का यह उचित समय है
या नहीं। अगर नेतृत्व इस पर सही निर्णय नहीं ले सकता तो आंदोलन में मार खाने की
पूरी गुंजाइश रह जायेगी। साधारण परिस्थिति की जानकारी, वैज्ञानिक प्रयोग और
इतिहास की जानकारी के जरिये ही हो सकती है। सफल नेतृत्व की कसौटी है, साधारण परिस्थिति की पूर्ण जानकारी और
विशेष परिस्थिति में उस जानकारी को लागू करने की क्षमता। नेतृत्व की व्यक्तिगत तौर
पर महत्वाकांक्षी नहीं होना चाहिए। ईमानदारी और कुर्बानी, नेतृत्व के साथ
श्वास-निःश्वास की तरह जुड़े हुए गुण होने चाहिए। तभी वह नेतृत्व लोकप्रिय हो सकता
है और उस नेतृत्व पर भरोसा करके लाखों लोग जान हथेली पर रखकर संघर्ष में कूद
जायेंगे।
10. आज की ट्रेड यूनियनें अर्थवाद से बुरी तरह ग्रस्त
हैं। आर्थिक मांग के लिए संघर्ष करना अर्थवाद नहीं है। परंतु जब संघर्ष केवल
आर्थिक मांग के लिए होता है और आर्थिक मांग के अलावा बाकी तमाम राजनैतिक, सांस्कृतिक और सामाजिक
सवालों को ताक पर रख दिया जाता है, तब इस प्रकार की नीति
को अर्थवाद कहा जाता है। यह एक खतरनाक नीति है। आज की ट्रेड यूनियनें ऐसे ही
खतरनाक रास्ते पर चल रही हैं। इससे ट्रेड यूनियनों के जीवन की सजीवता समाप्त हो
चुकी है और सूखी लकड़ी पर बढ़ई द्वारा रंदा चलाये जाने की तरह मजदूरों की जिंदगी
के सांस्कृतिक, सामाजिक
और राजनैतिक पहलुओं में निराशाजनक कृत्रिमता लाकर उन पर पूंजीपतियों के राजनैतिक, सांस्कृतिक और सामाजिक
विचारों को थोपा जा रहा है।
हैं। आर्थिक मांग के लिए संघर्ष करना अर्थवाद नहीं है। परंतु जब संघर्ष केवल
आर्थिक मांग के लिए होता है और आर्थिक मांग के अलावा बाकी तमाम राजनैतिक, सांस्कृतिक और सामाजिक
सवालों को ताक पर रख दिया जाता है, तब इस प्रकार की नीति
को अर्थवाद कहा जाता है। यह एक खतरनाक नीति है। आज की ट्रेड यूनियनें ऐसे ही
खतरनाक रास्ते पर चल रही हैं। इससे ट्रेड यूनियनों के जीवन की सजीवता समाप्त हो
चुकी है और सूखी लकड़ी पर बढ़ई द्वारा रंदा चलाये जाने की तरह मजदूरों की जिंदगी
के सांस्कृतिक, सामाजिक
और राजनैतिक पहलुओं में निराशाजनक कृत्रिमता लाकर उन पर पूंजीपतियों के राजनैतिक, सांस्कृतिक और सामाजिक
विचारों को थोपा जा रहा है।
हमें ऐसी रंदा लगायी गयी लकड़ी की जरूरत नहीं है। हम
एक सजीव सुंदर वृक्ष की तरह का जीवन अपने अंदर समा लेना चाहते हैं। पूंजीपति
मजदूरों को आधे-अधूरे, विकृत
एवं कमजोर बनाकर रखना चाहते हैं- सस्ती कीमत की निर्जीव वस्तु की तरह। इससे उनके
मालामाल होने की प्रक्रिया सुरक्षित रहने की गारंटी हो जाती है।
एक सजीव सुंदर वृक्ष की तरह का जीवन अपने अंदर समा लेना चाहते हैं। पूंजीपति
मजदूरों को आधे-अधूरे, विकृत
एवं कमजोर बनाकर रखना चाहते हैं- सस्ती कीमत की निर्जीव वस्तु की तरह। इससे उनके
मालामाल होने की प्रक्रिया सुरक्षित रहने की गारंटी हो जाती है।
पूंजीवादी विचारों क़ॆ अवसरवादियों ने मजदूर आंदोलन
को गुमराह करने के लिए अर्थवाद को जारी किया है। इन अवसरवादियों को संशोधनवादी कहा
जाता है। ये मजदूरों की वैज्ञानिक विचारधारा का विरोध करते हैं और पूंजीपतियों के
बताये रास्ते पर मजदूरों को ले जाने की कोशिश करते हैं।
को गुमराह करने के लिए अर्थवाद को जारी किया है। इन अवसरवादियों को संशोधनवादी कहा
जाता है। ये मजदूरों की वैज्ञानिक विचारधारा का विरोध करते हैं और पूंजीपतियों के
बताये रास्ते पर मजदूरों को ले जाने की कोशिश करते हैं।
नतीजा यह हो रहा है कि आज देश में तमाम ट्रेड
यूनियनों के सामने साल में एक बार बोनस की लड़ाई लड़ने और तीन या पांच साल में एक
बार वेतनमान बदलने की लड़ाई लड़ने के अलावा दूसरा कोई कार्यक्रम नहीं रह गया है।
तमाम केंद्रीय ट्रेड यूनियनों का काम सिर्फ प्रमोशन के लिए सिफारिश करना या
चार्जशीट का जवाब देने की दुकानदारी तक सीमित रह गया है।
यूनियनों के सामने साल में एक बार बोनस की लड़ाई लड़ने और तीन या पांच साल में एक
बार वेतनमान बदलने की लड़ाई लड़ने के अलावा दूसरा कोई कार्यक्रम नहीं रह गया है।
तमाम केंद्रीय ट्रेड यूनियनों का काम सिर्फ प्रमोशन के लिए सिफारिश करना या
चार्जशीट का जवाब देने की दुकानदारी तक सीमित रह गया है।
उत्पादन की नीति का निर्धारण पूंजीपति करता है। इससे
धड़ल्ले से मशीनीकरण का राक्षस मजदूरों की नौकरियों को खाये जा रहा है। राजनीति
करने की जिम्मेदारी ठेकेदारों, शराब ठेकेदारों, मालगुजारों आदि शोषक वर्ग को सौंप दी गयी
है।
धड़ल्ले से मशीनीकरण का राक्षस मजदूरों की नौकरियों को खाये जा रहा है। राजनीति
करने की जिम्मेदारी ठेकेदारों, शराब ठेकेदारों, मालगुजारों आदि शोषक वर्ग को सौंप दी गयी
है।
संस्कृति का ठेका बम्बई (अब मुंबई) के स्मगलर और अन्य
काले पैसे के पूंजीपतियों को दे दिया गया है, जो ढुसुम-ढुसुम और
नंगे नाचवाली कुसंस्कृति को जन संस्कृति बनाने में ओवर-टाइम कर रहे हैं।
काले पैसे के पूंजीपतियों को दे दिया गया है, जो ढुसुम-ढुसुम और
नंगे नाचवाली कुसंस्कृति को जन संस्कृति बनाने में ओवर-टाइम कर रहे हैं।
शराब के नशे में पूरा देश बेहोश है, महिलाओं पर अत्याचार जारी है और इधर
ट्रेड यूनियनों के पास सिर्फ एक ही कार्यक्रम है, ‘बोनस दो, बोनस दो।’ पैसा बढ़ता है, महंगाई और भी बढ़ती है, मजदूर की जेब खाली हो जाती है और वह
सूदखोर के चंगुल में जा फंसता है। ठेकेदार पैसा बढ़ाता है और शराब ठेकेदार उसे लूट
ले जाता है। घर की औरत मार खाती है, बच्चों को भूखे रहना
पड़ता है और मजदूर झोपड़ियों में सदा सोया रह जाता है।
ट्रेड यूनियनों के पास सिर्फ एक ही कार्यक्रम है, ‘बोनस दो, बोनस दो।’ पैसा बढ़ता है, महंगाई और भी बढ़ती है, मजदूर की जेब खाली हो जाती है और वह
सूदखोर के चंगुल में जा फंसता है। ठेकेदार पैसा बढ़ाता है और शराब ठेकेदार उसे लूट
ले जाता है। घर की औरत मार खाती है, बच्चों को भूखे रहना
पड़ता है और मजदूर झोपड़ियों में सदा सोया रह जाता है।
आज बैंक, जीवन बीमा, गोदी (डॉक) वगैरह
उद्योगों में अर्थवाद इतनी मजबूत जड़ें जमा चुका है कि वहां मजदूरों के सामने अपने
उद्योगों को छोड़कर दूसरे उद्योंगों के मजदूरों के मामलों और संघर्षों के बारे में
कोई विचार ही नहीं रहता है। इन उद्योगों में ट्रेड यूनियन का नेतृत्व मजदूरों को
आत्म-केंद्रित और संवेदनहीन बना चुका है।
उद्योगों में अर्थवाद इतनी मजबूत जड़ें जमा चुका है कि वहां मजदूरों के सामने अपने
उद्योगों को छोड़कर दूसरे उद्योंगों के मजदूरों के मामलों और संघर्षों के बारे में
कोई विचार ही नहीं रहता है। इन उद्योगों में ट्रेड यूनियन का नेतृत्व मजदूरों को
आत्म-केंद्रित और संवेदनहीन बना चुका है।
अर्थवाद के एक और प्रकार का नमूना रेल उद्योग में
देखने को मिलता है। यहां हर मजदूर अपने विभाग के महत्व और विभाग की समस्या से घिरा
रहता है। वहां जब गार्ड साहब हरी झंडी दिखाते हैं तब गैंगमैन अपनी लाल झंडी दिखाकर
बैठ जाते हैं। यहां पर लाल-हरे को मिलाकर सारे रेल मजदूरों को संगठित करने का
प्रयास आज नहीं किया जा रहा है। अल्प समय के लिए 1974 की ऐतिहासिक रेल हड़ताल ने
इस दिशा में एक उम्मीद को जन्म दिया था, जिसकी गाड़ी केंद्रीय
यूनियनों के चक्कर में फिर पटरी से उतर गयी। इसके फलस्वरूप 146 स्वतंत्र यूनियनों
को इस तरह तानाशाही हमलों का शिकार होना पड़ा कि अभी तक वे फिर से खड़ी नहीं हो
पायी हैं। इस्पात उद्योग में भी इस तरह का संशोधनवादी प्रयास जारी है। इसी कारण
चार्जमैन, क्रेन
आपरेटर, वर्कमैन
आदि मजदूरों को अलग-अलग संगठनों में संगठित करने की कोशिश चल रही है। फिर भी स्टील
प्लांट की इंटीग्रेटेड (समन्वित) उत्पादन व्यवस्था के कारण इन प्रयासों को
मैनेजमेंट का पूर्ण समर्थन नहीं मिल पा रहा है।
देखने को मिलता है। यहां हर मजदूर अपने विभाग के महत्व और विभाग की समस्या से घिरा
रहता है। वहां जब गार्ड साहब हरी झंडी दिखाते हैं तब गैंगमैन अपनी लाल झंडी दिखाकर
बैठ जाते हैं। यहां पर लाल-हरे को मिलाकर सारे रेल मजदूरों को संगठित करने का
प्रयास आज नहीं किया जा रहा है। अल्प समय के लिए 1974 की ऐतिहासिक रेल हड़ताल ने
इस दिशा में एक उम्मीद को जन्म दिया था, जिसकी गाड़ी केंद्रीय
यूनियनों के चक्कर में फिर पटरी से उतर गयी। इसके फलस्वरूप 146 स्वतंत्र यूनियनों
को इस तरह तानाशाही हमलों का शिकार होना पड़ा कि अभी तक वे फिर से खड़ी नहीं हो
पायी हैं। इस्पात उद्योग में भी इस तरह का संशोधनवादी प्रयास जारी है। इसी कारण
चार्जमैन, क्रेन
आपरेटर, वर्कमैन
आदि मजदूरों को अलग-अलग संगठनों में संगठित करने की कोशिश चल रही है। फिर भी स्टील
प्लांट की इंटीग्रेटेड (समन्वित) उत्पादन व्यवस्था के कारण इन प्रयासों को
मैनेजमेंट का पूर्ण समर्थन नहीं मिल पा रहा है।
अर्थवादी लोग चाहे जितना भी आर्थिक मांगों के बारे
में आवाज बुलंद करें, फिर
भी आज ट्रेड यूनियनों के कार्यकर्ता इस बारे में वाकिफ हैं कि,
में आवाज बुलंद करें, फिर
भी आज ट्रेड यूनियनों के कार्यकर्ता इस बारे में वाकिफ हैं कि,
क). 1947 या 1960 के मूल्य सूचकांक के साथ आज के
मूल्य सूचकांक की तुलना की जाये तो हम देखेंगे कि इन 43 सालों या 30 सालों के बीच
मजदूरों का वेतन रुपयों में बढ़ा है, लेकिन असली वेतन घटा
है। मतलब यह हुआ कि आर्थिक संघर्षों और समझौतों की लम्बी प्रक्रिया के बाद भी कुछ
हासिल नहीं हुआ, बल्कि शोषण और भी बढ़ा
है।
मूल्य सूचकांक की तुलना की जाये तो हम देखेंगे कि इन 43 सालों या 30 सालों के बीच
मजदूरों का वेतन रुपयों में बढ़ा है, लेकिन असली वेतन घटा
है। मतलब यह हुआ कि आर्थिक संघर्षों और समझौतों की लम्बी प्रक्रिया के बाद भी कुछ
हासिल नहीं हुआ, बल्कि शोषण और भी बढ़ा
है।
ख). आर्थिक मांगों के बारे में ट्रेड यूनियनों का
दिमाग सरकार (राज्य) और मैनेजमेंट द्वारा निर्देशित होता है। जैसे कि हर बार वेतन
संशोधन (वेज रिवीज़न) में देखा जाता है कि वहां पुनर्विचार के लिए विशेष समयावधि
का प्रावधान दिया रहता है। या, राज्य द्वारा विज्ञप्ति (नोटिफिकेशन)
जारी करने के अधिकार और विभिन्न कोशिशों की सिफारिशों को मजदूरों के सामने रखकर
सरकार ट्रेड यूनियनों को लालायित करती रहती है।
दिमाग सरकार (राज्य) और मैनेजमेंट द्वारा निर्देशित होता है। जैसे कि हर बार वेतन
संशोधन (वेज रिवीज़न) में देखा जाता है कि वहां पुनर्विचार के लिए विशेष समयावधि
का प्रावधान दिया रहता है। या, राज्य द्वारा विज्ञप्ति (नोटिफिकेशन)
जारी करने के अधिकार और विभिन्न कोशिशों की सिफारिशों को मजदूरों के सामने रखकर
सरकार ट्रेड यूनियनों को लालायित करती रहती है।
घ). उद्योगों ओर अंचलों के आधार पर अलग-अलग वेतनमान
बनाकर सरकार एक ‘परिवर्तनशील लक्ष्मण रेखा’ खींच देती है। जिस तरह
अंग्रेजों ने रियासतों के लिए अलग-अलग कानून बनाकर उसकी जनता के मुंह से ‘अंग्रेजों का कानून लागू करो’ वाली मांग उठवाने का
साम्राज्यवादी तरीका अपनाया, आज भी उसी तरीके से
सरकार अर्थवाद को बढ़ावा दे रही है। एक उद्योग के मजदूर दूसरे उद्योग के मजदूरों
के समान वेतन हासिल करने की कोशिश में सारी जिंदगी बिता देते हैं।
बनाकर सरकार एक ‘परिवर्तनशील लक्ष्मण रेखा’ खींच देती है। जिस तरह
अंग्रेजों ने रियासतों के लिए अलग-अलग कानून बनाकर उसकी जनता के मुंह से ‘अंग्रेजों का कानून लागू करो’ वाली मांग उठवाने का
साम्राज्यवादी तरीका अपनाया, आज भी उसी तरीके से
सरकार अर्थवाद को बढ़ावा दे रही है। एक उद्योग के मजदूर दूसरे उद्योग के मजदूरों
के समान वेतन हासिल करने की कोशिश में सारी जिंदगी बिता देते हैं।
च). ‘कुछ छोड़ो-कुछ लो’ (गिव एंड टेक) की नीति इस स्थिति में
जड़ पकड़ लेती है। विजय का नहीं, बल्कि समझौते का पाठ पढ़ाया जाता है, जबकि हर समझौते को
लागू करने की समस्या हमेशा बनी ही रहती है। ‘इंकलाब जिंदाबाद’ के नारे के साथ ‘वेतन-समझौता जिंदाबाद’ के नारे से आसमान गूंजता रहता है इंकलाब
कभी नहीं आता।
जड़ पकड़ लेती है। विजय का नहीं, बल्कि समझौते का पाठ पढ़ाया जाता है, जबकि हर समझौते को
लागू करने की समस्या हमेशा बनी ही रहती है। ‘इंकलाब जिंदाबाद’ के नारे के साथ ‘वेतन-समझौता जिंदाबाद’ के नारे से आसमान गूंजता रहता है इंकलाब
कभी नहीं आता।
आज केंद्रीय ट्रेड यूनियनें अर्थवाद के गड्ढ़े में
फंस चुकी हैं। आर्थिक मंदी के युग में कर्ण का रथ जमीन में धंसता जा रहा है, कर्ज जितना ही रथ हांकता है, रथ उतना ही धंसता जाता है। कर्ण अपने ही
रथ में बंदी बना हुआ है।
फंस चुकी हैं। आर्थिक मंदी के युग में कर्ण का रथ जमीन में धंसता जा रहा है, कर्ज जितना ही रथ हांकता है, रथ उतना ही धंसता जाता है। कर्ण अपने ही
रथ में बंदी बना हुआ है।
इस हालत में नेता मजदूरों को सांत्वना देता है- ‘हो रही है, बातचीत हो रही है’, ‘कुछ मिला है’, ‘कुछ दिला देंगे।’ मजदूर अब आश्वासनों से खुश नहीं है। अब
मजदूर बढ़ चला है, सेनापति पीछे छूट रहा
है। पीछे फंसा हुआ सेनापति मजदूरों को उग्रवादी कहकर, वामपंथी भटकाव और
पृथकतावाद की दहाइ देकर अपने को व्यवस्थारूपी एवं राज्यरूपी भगवान के सामने
निर्दोष बता रहा है। मजदूर वर्ग केंद्रीय ट्रेड यूनियनों को हटाकर स्वतंत्र ट्रेड
यूनियनों का निर्माण कर रहा है। लेकिन अधिकांश स्वतंत्र ट्रेड यूनियनें भी उसी राह
की राही हैं।
मजदूर बढ़ चला है, सेनापति पीछे छूट रहा
है। पीछे फंसा हुआ सेनापति मजदूरों को उग्रवादी कहकर, वामपंथी भटकाव और
पृथकतावाद की दहाइ देकर अपने को व्यवस्थारूपी एवं राज्यरूपी भगवान के सामने
निर्दोष बता रहा है। मजदूर वर्ग केंद्रीय ट्रेड यूनियनों को हटाकर स्वतंत्र ट्रेड
यूनियनों का निर्माण कर रहा है। लेकिन अधिकांश स्वतंत्र ट्रेड यूनियनें भी उसी राह
की राही हैं।
हमें अर्थवाद का अंधकार नहीं, आर्थिक संघर्ष के
साथ-साथ मुक्ति का आलोक भी चाहिए, एक इज्जतदार मजदूर वर्ग की प्रतिष्ठा
चाहिए, नयी
संस्कृति की शुद्ध हवा चाहिए, एक क्रांतिकारी ट्रेड यूनियन चाहिए।
साथ-साथ मुक्ति का आलोक भी चाहिए, एक इज्जतदार मजदूर वर्ग की प्रतिष्ठा
चाहिए, नयी
संस्कृति की शुद्ध हवा चाहिए, एक क्रांतिकारी ट्रेड यूनियन चाहिए।